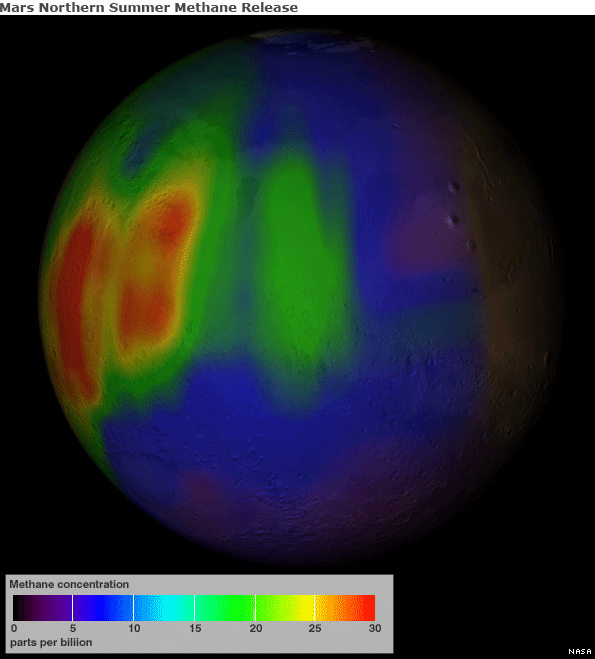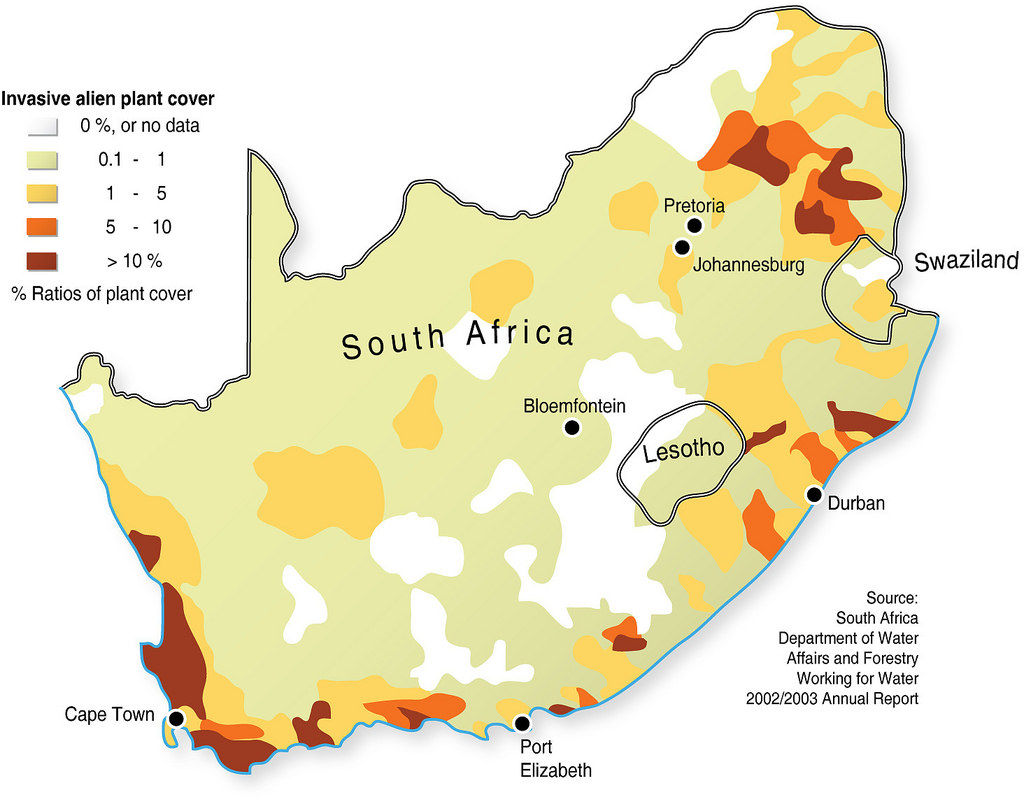पिछले दिनों लंबे अनशन के बाद डॉ. गुरुदास अग्रवाल का निधन हो गया। डॉ. अग्रवाल ने पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण तथा गंगा की सुरक्षा के अलावा पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यहां प्रस्तुत रिपोर्ट डॉ. अग्रवाल के मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से किशोर भारती एवं एकलव्य नामक दो संस्थाओं द्वारा 1987 में चलाए गए एक अनोखे पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम की बानगी प्रस्तुत करती है। एक ओर यह कार्यक्रम समाज के महत्वपूर्ण मुद्दों को शिक्षा में स्थान देने का एक प्रयास था, वहीं यह पर्यावरण के वैज्ञानिक अध्ययन की भी एक मिसाल है।
परासिया के लोग पेंच स्टाफ क्लब में एक विशेष जलसे में शामिल होने आए हैं। तीन बजे दोपहर का समय है। यह जलसा अजीब सा ही होने वाला है। परासिया और आसपास के क्षेत्र के पानी की गुणवत्ता पर रिपोर्ट पढ़ी जानी है। यानी पानी पीने के लिए व अन्य उपयोगों के लिए कितना उपयुक्त है। साथ ही साथ पेंच नदी की स्थिति पर भी एक रिपोर्ट पेश होगी। यह रिपोर्ट कोई सरकारी विभाग की ओर से नहीं बल्कि इस इलाके की उच्चतर माध्यमिक शालाओं और महाविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत होनी है। वे बताने वाले हैं कि परासिया, चांदामेटा, न्यूटन आदि के कुओं, झिरियों, हैंड-पम्पों आदि का पानी कैसा है?पीने योग्य है या नहीं?इस जलसे के शुरू होने से पहले सुबह से ही एक पोस्टर प्रदर्शनी पेंच स्टाफ क्लब के बरामदे में लगा दी गई थी जिसमें इस इलाके के पानी के बारे में मोटी-मोटी बातें चित्रित थीं। आखिर इन विद्यार्थियों को ये बातें पता कैसे चलीं? इसी बात का उत्तर हम यहां देने की कोशिश करेंगे।
इनमें से अधिकांश विद्यार्थी विज्ञान विषय लेकर 11 वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। इनके सामने एक प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव यह था कि ये अपने इलाके के पर्यावरण का वैज्ञानिक अध्ययन करें।
इसके लिए इन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। परन्तु पर्यावरण कोई छोटी-मोटी चीज़ तो है नहीं। वह तो बहुत बड़ी बात है और हमारे आसपास जो कुछ भी है या घटता है या उन चीज़ों के, घटनाओं के आपसी सम्बंध, सभी कुछ तो इसमें समाया हुआ है। इसलिए सोचा कि पर्यावरण के एक छोटे से हिस्से – पानी – से शुरुआत की जाए। दूसरी बात यह थी कि पानी का महत्व बहुत है। तीसरी बात यह थी कि पानी का अध्ययन करना आसान है बजाय किसी और चीज़ के, जैसे हवा या मिट्टी। शुरुआत तो हमेशा आसान से ही करते हैं।
यह प्रस्ताव देने वाली दो संस्थाएं थीं – बनखेड़ी की किशोर भारती और पिपरिया की एकलव्य। संभवत: पाठक इन दोनों ही संस्थाओं से वाकिफ हैं। मुख्य बात यह है कि दोनों ही शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के लिए काम करती हैं। इन्होंने प्रस्ताव क्यों दिया?
पर्यावरण का आजकल बहुत हल्ला है और पर्यावरण शिक्षा का शोर भी शुरू हो चला है। देखा यह जा रहा है कि पर्यावरण के विषय में कोई कुछ भी कह दे, चल जाता है क्योंकि इसके व्यवस्थित अध्ययन की बात तो होती ही नहीं। कोई कह दे पेड़ कटने से बारिश नहीं हो रही तो भी ठीक और कोई कह दे शेर को बचाना पर्यावरण है तो भी ठीक। आखिर निर्णय के मापदंड क्या हों? होता यह है कि आम लोगों के सामने मात्र निष्कर्ष नारों के रूप में आते हैं, उनकी विधियां नहीं। निर्णय तो विधियों से होता है। इसलिए विधियां जाने बिना सिर्फ निष्कर्ष देखा जाए तो नारेबाज़ी ही होगी। इन विद्यार्थियों के सामने प्रस्ताव रखने का एक कारण तो यही था कि ये अध्ययन की इन विधियों को समझें।
दूसरा कारण। विज्ञान विषय पढ़ते हुए और प्रयोग करते हुए ऐसा होता है कि भई‘कोर्स’ में है तो करना है। अपने जीवन से कुछ जुड़ता नहीं। वही टाइट्रेशन, वही सूचक घोल, वही फिनॉफ्थलीन, वही ब्यूरेट, पिपेट कैसे उपयोगी काम में लग सकते हैं, यह भी इस प्रस्ताव की भावना थी।
तीसरा कारण था कि पर्यावरण शिक्षा की बातें खूब हो रही हैं। इसमें मुख्य उद्देश्य यह रहता है कि अन्य विषयों के समान पर्यावरण पर कुछ भाषण बच्चे सुनें। प्रस्ताव में यह निहित ही था कि पर्यावरण शिक्षा का एक वैकल्पिक मॉडल विकसित हो। इसके पीछे मान्यता यह थी कि पर्यावरण समझने के लिए पर्यावरण से मेल-जोल करना ज़रूरी है।
खैर, ये सब तो सैद्धांतिक बातें थीं और इन्हें कोई भी झाड़ सकता है। अब कुछ ठोस बात। सबसे पहले तो प्रशिक्षण। दिसंबर में इन विद्यार्थियों को एक सप्ताह का प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान इन्हें पानी के लगभग 10 परीक्षण सिखाए जाते थे। परीक्षणों की सूची बॉक्स में है। कुछ नमूने कृत्रिम रूप से तैयार किए गए ताकि परिणामों की जांच हो सके और कुछ प्राकृतिक नमूने लाए गए। कौन से परीक्षण सिखाए जाएं इसका निर्णय विभिन्न आधारों पर हुआ। उच्चतर माध्यमिक शालाओं के विद्यार्थी इन्हें कर पाएं, महत्वपूर्ण हों, रसायन एवं उपकरण वगैरह आसानी से उपलब्ध कराए जा सकें, प्रमुख रहे।
हरेक विद्यालय से 5 विद्यार्थी चुने गए और एक या दो अध्यापक प्रभारी बने। प्रत्येक विद्यार्थी को अपने क्षेत्र के पानी के दो स्रोतों से नमूने लाने थे। इनमें से एक स्रोत भूमिगत हो और दूसरा कोई अन्य। यह हर महीने हुआ। परन्तु सभी विद्यार्थी दसों परीक्षण नहीं करते थे। सभी विद्यार्थी अपने नमूने लाकर बेंच पर जमा देते थे। अब हरेक को दो-दो परीक्षण की ज़िम्मेदारी दी गई थी। हर विद्यार्थी सभी नमूनों पर उसे दिए गए दो परीक्षण करता था हालांकि उसको ट्रेनिंग सभी परीक्षणों के लिए दी गई थी। ऐसा इसलिए किया गया था कि हर विद्यार्थी का हाथ दो परीक्षणों पर जम जाए और आंकड़े ज़्यादा विश्वसनीय हों। इस तरह से 6 महीनों तक लगातार परीक्षण का काम चला। ये मुख्यत: रासायनिक परीक्षण थे।
इसके साथ-साथ कॉलेज के दो छात्रों द्वारा दो तरह के परीक्षण और किए गए। पहला, पेंच नदी का जैविक अध्ययन और पानी के कुछ नमूनों का बैक्टीरिया परीक्षण। वैसे अच्छा होता यदि बैक्टीरिया परीक्षण सभी नमूनों का हो पाता। परन्तु यह थोड़ा मुश्किल परीक्षण है।
इस तरह से क्षेत्र के जल रुाोतों के बारे में रासायनिक व जैविक जानकारी एकत्रित हुई। पर एक और आयाम इसमें जुड़ना अभी बाकी था। इस जानकारी की लोगों के दैनिक अनुभवों से तुलना। यह देखना ज़रूरी था कि इस वैज्ञानिक जानकारी का लोगों के अनुभवों से क्या तालमेल है। इसके लिए एक सर्वेक्षण किया गया। ऐसे दस-दस परिवारों से जानकारी प्राप्त की गई जो इन जल रुाोतों का उपयोग करते हैं।
अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा उस इलाके की परिस्थिति को समझ लें जहां यह काम हुआ। परासिया, चांदामेटा और न्यूटन ये तीन पड़ोसी शहर छिंदवाड़ा ज़िले में हैं और पेंच नदी की घाटी में बसे हुए हैं। आसपास पश्चिम कोयला क्षेत्र की कोयला खदानें हैं। काफी पुरानी खदानें हैं। इस क्षेत्र में खेती न के बराबर होती है। खदानों के कारण यहां का पानी समस्या मूलक है और खदान व यातायात के कारण हवा की हालत भी अच्छी नहीं है। जाड़े के दिनों में सुबह-सुबह यदि परासिया की पहाड़ी से न्यूटन शहर ऊपर से देखा जाए तो धुएं से बना एक मैदान नजर आता है जिस पर एक मित्र का कहना है कि इस ‘मैदान’ पर उनकी जीप चलाने की इच्छा कई बार हुई।
ये जानकारी इकट्ठी होने के साथ-साथ एक और बात हो रही थी। ये विद्यार्थी पानी को ध्यान से देख रहे थे, उसके ‘सम्पर्क’ में आ रहे थे, प्रश्न कर रहे थे और धीरे-धीरे पर्यावरण के अन्य अंगों पर भी सोच रहे थे। यही तो थी पर्यावरण जागरूकता! खैर, जब 6 महीने यह काम चल चुका तो ज़रूरत थी इसे व्यवस्थित करने की, समेकित करने की और लोगों के बीच प्रस्तुत करने की। इसके लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई किशोर भारती में। कार्यक्रम में जुड़े सारे विद्यार्थी, प्रभारी शिक्षक और पर्यावरण से जुड़े कुछ कार्यकर्ता इस सात दिवसीय कार्यशाला में शामिल हुए।
| किए गए परीक्षण
1. पी.एच.
2. अम्लीयता
3. क्षारीयता
4. कठोरता – ज्यादा कठोरता होने से साबुन के साथ झाग नहीं बनते और दाल पकने में परेशानी होती है।
5. क्लोराइड – पानी के स्वाद पर असर पड़ता है।
6. फ्लोराइड – पानी में फ्लोराइड कम होने से हड्डियों का विकास ठीक से नहीं हो पाता, ज्यादा फ्लोराइड होने पर फ्लोरोसिस बीमारी हो सकती है।
7. लौह – ज्यादा होने पर पाचन क्रिया पर प्रतिकूल असर पड़ता है।
8. घुलित आक्सीजन – इसससे पानी के कई अन्य गुणों का पता चलता है।
9. परमेंग्नेट मांग – इससे पानी में कार्बनिक अशुद्धियों का पता चलता है।
10. कोलीफार्म परीक्षण- कोलीफार्म एक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, जो मनुष्य की आंत में पाए जाते है। पानी के प्राकृतिक रुाोत में इनका पाया जाना यह सूचित करता है कि यह स्रोत मल द्वारा प्रदूषित है।
|
इस कार्यशाला में पहला काम तो यह हुआ कि सारी जानकारी व आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई। रिपोर्ट, पांच भागों में तैयार हुई। दूसरा काम हुआ कि रिपोर्ट के आधार पर पोस्टर प्रदर्शनी बनाई गई। इसके अलावा विभिन्न विषयों पर चर्चाएं हुर्इं। इनमें पर्यावरण की समझ, जंगल, जल चक्र, पानी व हवा प्रदूषण, उद्योगों से स्वास्थ्य का रिश्ता, भोपाल गैस कांड आदि प्रमुख थे। ऐसे भाषण तो यहां-वहां सुनने को मिल ही जाते हैं। इन विषयों पर कोई भी कुछ भी कह सकता है। फिर यहां क्या खास हुआ?खास यह हुआ कि सुनने वाले स्वयं का कुछ अनुभव लेकर बैठे थे। कोई बात सुनकर वे चुप नहीं रहते थे। वे पूछते थे कि कैसे पता किया, किस आधार पर कह रहे हैं, यदि अमुक बात सही है तो उससे जोड़कर देखते थे कि और क्या-क्या बातें सही होंगी। यही तो महत्वपूर्ण है। कोई कुछ भी कहे, आपके पास वह हुनर हो जिससे आप दूध को दूध, पानी को पानी पहचान सकें।
अब हम चलें वापिस 12 जुलाई पर। प्रदर्शनी सुबह से ही लगा दी गई थी। विद्यार्थी भाग-भागकर अपना काम आंगतुकों को समझा रहे थे। कितना अच्छा लग रहा था। विद्यार्थी अपनी प्रयोगशाला के निष्कर्षों को आम लोगों को बता रहे थे। आम लोग शायद पहली बार उत्सुक थे कि उनके बच्चों ने स्कूल की प्रयोगशाला में क्या किया। एक और बात वहां हो रही थी। पहले से ही शहर में यह घोषणा कर दी गई थी कि लोग यदि चाहें तो अपने साथ पानी का नमूना लेते आएं, उसकी जांच करके परिणाम तुरंत दे दिए जाएंगे। कई लोग शीशियों में पानी भरकर लाए थे। प्रदर्शनी के बीच में सब तामझाम जमा था। सामने ही विद्यार्थी प्रयोग करके बता रहे थे – पानी कितना कठोर है, उसमें कितना क्लोराइड है आदि। साथ ही यह भी कि क्या करना होगा। विज्ञान की विधियां सार्वजनिक हो रहीं थीं।
तीन बजे आम सभा हुई। बाकी तो भाषण वगैरह होते ही हैं। सभा में कई प्रमुख व्यक्तियों ने भाग लिया। सबसे प्रभावशाली हिस्सा था विद्यार्थियों द्वारा रिपोर्ट पढ़ी जाना। आशा बन रही थी कि अपने इलाके के पर्यावरण की नियमित जांच उस इलाके की शैक्षणिक संस्थाएं कर सकती हैं। यह काम उन्हीं प्रयोगशालाओं में हो सकता है जहां सामान्यतया ऊपर से निरर्थक, अप्रासंगिक से दिखने वाले प्रयोग किए जाते हैं। क्या यही पर्यावरण शिक्षा का एक मॉडल नहीं हो सकता?
खैर, जहां तक किशोर भारती और एकलव्य के प्रस्ताव का सवाल था वह तो यहीं खत्म हुआ। परन्तु एक बार शुरू होने पर ऐसी प्रक्रियाएं रुकती हैं क्या? इन शिक्षकों और विद्यार्थियों में कुछ बदल गया था। कुछ और करने की इच्छा बन चुकी थी। क्या करें? इन लोगों ने मिलकर एक समूह की स्थापना की है –‘नीर’! इस नाम का सम्बंध इस समूह की उत्पत्ति से है, न कि आगे की योजनाओं से। आगे की योजनाएं तो अभी बन रही हैं। पूरे कार्यक्रम की बात तो हो गई पर यह तो बताया ही नहीं कि विद्यार्थियों की रिपोर्टों से क्या निष्कर्ष निकला। वास्तव में वह उतना महत्वपूर्ण भी नहीं है। वह ज़रूर महत्वपूर्ण है परासिया क्षेत्र के लोगों के लिए। परन्तु कार्यक्रम की मूल भावना वे रिपोर्ट बनाना नहीं बल्कि विद्यार्थियों और अन्य लोगों मे पर्यावरण के प्रति सजगता पैदा करना है। साथ ही साथ यह बात बताना भी कि ये सारे निष्कर्ष कुछ विधियों पर आधारित होते हैं और इनकों जांचा जा सकता है।(स्रोत फीचर्स)
किए गए परीक्षण
1. पी.एच.
2. अम्लीयता
3. क्षारीयता
4. कठोरता – ज्यादा कठोरता होने से साबुन के साथ झाग नहीं बनते और दाल पकने में परेशानी होती है।
5. क्लोराइड – पानी के स्वाद पर असर पड़ता है।
6. फ्लोराइड – पानी में फ्लोराइड कम होने से हड्डियों का विकास ठीक से नहीं हो पाता, ज्यादा फ्लोराइड होने पर फ्लोरोसिस बीमारी हो सकती है।
7. लौह – ज्यादा होने पर पाचन क्रिया पर प्रतिकूल असर पड़ता है।
8. घुलित आक्सीजन – इसससे पानी के कई अन्य गुणों का पता चलता है।
9. परमेंग्नेट मांग – इससे पानी में कार्बनिक अशुद्धियों का पता चलता है।
10. कोलीफार्म परीक्षण– कोलीफार्म एक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, जो मनुष्य की आंत में पाए जाते है। पानी के प्राकृतिक रुाोत में इनका पाया जाना यह सूचित करता है कि यह स्रोत मल द्वारा प्रदूषित है।
नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
Photo Credit :https://www.eklavya.in/gallery/photos-communitymenu/category/5-hoshangabad-science-teaching-programme