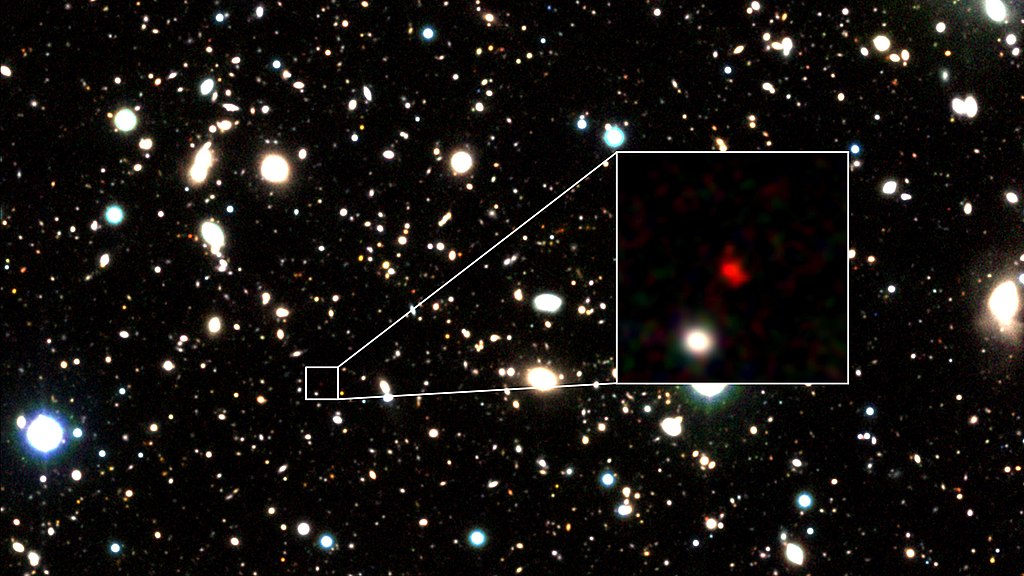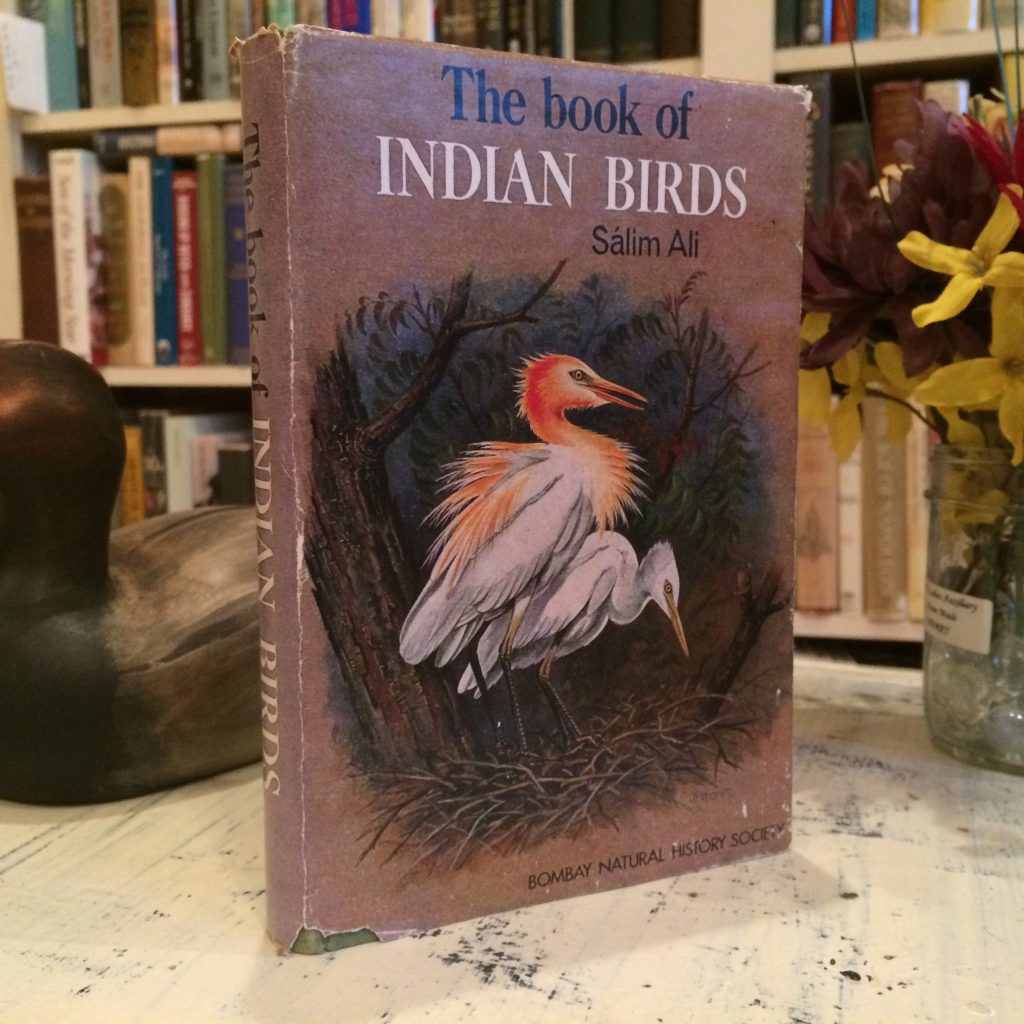विकलांगता की बात आते ही दो तस्वीरें सामने आती हैं। पहली है यूएसए, अन्य विकसित पश्चिमी देशों और जापान जैसे गैर-पश्चिमी विकसित देशों की तस्वीर, जहां विकलांगजन को अवसर, सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त है, जिनका उपयोग करते हुए वे गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने में समर्थ हैं। दूसरी तस्वीर है भारत सहित विकासशील और पिछड़े देशों की, जहां संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न पहलों के बावजूद विकलांगजन घोर दुर्दशापूर्ण जीवन जीने को अभिशप्त हैं।
विकलांगजन के हितों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1981 को विश्व विकलांगजन वर्ष घोषित किया गया था और 1983 से 1992 के दशक को संयुक्त राष्ट्र विकलांगजन दशक। संयुक्त राष्ट्र की ही पहल पर 1992 से 3 दिसंबर प्रति वर्ष विश्व विकलांगजन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उसकी इन पहलों से पहले भी दुनिया के विकसित देशों में, विशेष रूप से यूएसए में, विकलांगजन के लिए उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा था क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वहां डिसेबिलिटी राइट्स मूवमेंट काफी ज़ोर पकड़ चुका था। डिसेबिलिटी राइट्स मूवमेंट का खासा असर रहा और इससे इतना दबाव बना कि संयुक्त राष्ट्र संघ और दुनिया भर के देशों की सरकारों को सबसे उपेक्षित वर्ग यानी विकलांग वर्ग के लिए पहल करने पर मजबूर होना पड़ा।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद डिसेबिलिटी राइट्स मूवमेंट इसलिए अधिक प्रभावशाली हुआ क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में वे सैनिक शामिल थे जो विश्व युद्ध में विकलांग हो गए थे। चूंकि वे युद्ध के नायक थे और जनता उनके साथ थी इसलिए उनकी बातों या मांगों को नज़रअंदाज़ करना सरकार और संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए आसान नहीं था। इसके बावजूद परिणाम सामने आने में दो-तीन दशकों का वक्त लगा और ‘समान अवसर एवं पूर्ण भागीदारी’ पर आधारित कानून और नीतियां सामने आने लगी। ‘समान अवसर एवं पूर्ण भागीदारी’ विकलांगजन का ऐसा अधिकार है जो पूरी तरह इस बात पर निर्भर है कि किसी देश का संपूर्ण तंत्र, सरकार, संस्थाएं और गैर-विकलांग समुदाय विकलांगजन के प्रति अपना दायित्व किस प्रकार निभाते हैं।
भारत की ही मिसाल ले लीजिए जहां संविधान के निर्माताओं को यह एहसास तक नहीं हुआ कि उनसे विकलांग वर्ग की पूर्ण उपेक्षा हो रही है। भारत में विकलांगजन के लिए कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय सूची या समवर्ती सूची में न रखते हुए उन्होंने यह काम पूरी तरह राज्यों पर छोड़ दिया। संवेदनशीलता की कमी का नतीजा यह हुआ कि राज्यों द्वारा आधी सदी बीत जाने तक कोई प्रभावी कानून बनाए जाने की जानकारी नहीं है। विकलांगता सम्बंधी अंतर्राष्ट्रीय संधियों या घोषणा पत्रों पर हस्ताक्षर करने के बाद ही संविधान के विशेष प्रावधान का उपयोग करते हुए विकलांगजन के लिए 1995 और 2016 के केंद्रीय कानून लाए गए। लेकिन फिर भी विकलांगजन के लिए कानून बनाने का मुद्दा केंद्रीय या समवर्ती सूची में नहीं जोड़ा गया।
डिसेबिलिटी राइट्स मूवमेंट एक अत्यंत महत्वपूर्ण आंदोलन रहा है और इस पर निगाह डालना उचित होगा। यूएसए और अन्य विकसित देशों में यह विशेष रूप से प्रभावी रहा है और इसी का नतीजा है कि भारत सहित विकासशील और पिछड़े देशों में भी विकलांगजन के अधिकारों और कल्याण की बात हो रही है। डिसेबिलिटी राइट्स मूवमेंट एक विश्वव्यापी सामाजिक आंदोलन है लेकिन मुख्य रूप से यह यूएसए में जन्मा और पनपा और फिर दुनिया भर में फैल गया। इसका मुख्य लक्ष्य विकलांगजन को जबरन दरकिनार करने के विरुद्ध लड़ाई लड़ना है।
विकलांगजन के अधिकारों के लिए लड़ाई यूएसए में 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में शुरू हो चुकी थी और इसने धीरे-धीरे आकार लिया। लुई ब्रेल और उनके बाद हेलेन केलर ने इस दिशा में व्यक्तिगत तौर पर उल्लेखनीय कार्य किया। धीरे-धीरे स्थानीय और राज्य स्तरीय संगठन अस्तित्व में आए और पहला राष्ट्रीय संगठन – दी नेशनल एसोसिएशन ऑफ दी डेफ (बधिरों के राष्ट्रीय संगठन) – 1880 में स्थापित किया गया। 1930 के दशक में दी सोशल सिक्योरिटी एक्ट (सामाजिक सुरक्षा कानून) में दृष्टिबाधितों और विकलांग बच्चों की सहायता के लिए राज्यों को धनराशि उपलब्ध कराई गई। 1940 के दशक में नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट (राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कानून) के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ स्थापित करने की बात कही गई थी और विकलांगजन के अधिकारों के लिए दी अमेरिकन फेडरेशन ऑफ दी फिज़िकली हैंडीकैप्ड (शारीरिक रूप से विकलांगजन संगठन) प्रथम बहु-विकलांगता संगठन के रूप में उभरा।
1950 के दशक में ब्राउन बनाम बोर्ड ऑफ एजुकेशन के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के फलस्वरूप डिसेबिलिटी राइट्स मूवमेंट ने गति पकड़ी और 1964 के दी सिविल राइट्स एक्ट (नागरिक अधिकार कानून) से इस आंदोलन को नई दिशा मिली। 1970 के दशक में यह मांग भी उठी कि 1972 के रिहैबिलिटेशन एक्ट (पुनर्वास कानून) में विकलांगजन के नागरिक अधिकार शामिल किए जाएं। 1973 में पारित रिहैबिलिटेशन एक्ट में यह मांग पूरी की गई। इस तरह इतिहास में पहली बार विकलांगजन के नागरिक अधिकार कानूनन संरक्षित किए गए। तत्पश्चात सभी विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा तक पहुंच समान रूप से सुनिश्चित करने के लिए 1975 में दी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन एक्ट पारित हुआ (बाद में इसे इंडिविजुअल्स विथ डिसेबिलिटिज़ एजुकेशन एक्ट कहा गया)। एक कदम और आगे बढ़ते हुए 1980 के दशक में यह मांग रखी गई कि अलग-अलग कानूनों/हिस्सों में बंटे हुए प्रावधानों को एकल कानून का रूप दिया जाए। 1990 में अमेरिकंस विद डिसेबिलिटिज़ एक्ट पारित किया गया जिसका उद्देश्य विकलांगता के आधार पर भेदभाव को रोकना है।
भारत के संदर्भ में देखें तो विकलांगजन के अधिकारों को लेकर आंदोलन इतना मज़बूत नहीं रहा है और उनके लिए कानून भी आंदोलन के परिणामस्वरूप और कानून-निर्माताओं की स्वयं की सोच और संवेदनशीलता के कारण नहीं बने। दुर्भाग्यवश बहुत से अन्य देशों की तरह भारत में भी विकलांगजन को अनुपयोगी, अनुत्पादक और बोझ समझा जाता है। भारत में विकलांगजन के अधिकारों के लिए पहला कानून एशिया-प्रशांत क्षेत्र में विकलांगजनों की समानता और पूर्ण भागीदारी की घोषणा के आधार पर बना – नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995। इसका स्थान लेने वाला अगला कानून विकलांगजन के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की संधि (सं.रा. विकलांगजन अधिकार संधि – UNCRPD) के आधार पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के रूप में सामने आया। ये दोनों कानून अंतर्राष्ट्रीय संधि या घोषणा पत्र के पालन के लिए संविधान के अनुच्छेद 253 का उपयोग करते हुए बनाए गए थे। इन दोनों के बीच ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन और मल्टीपल डिसेबिलिटी से प्रभावित व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 पारित किया गया।
भारत में डिसेबिलिटी राइट्स मूवमेंट की शुरुआत 1970 के दशक से मानी जा सकती है लेकिन आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति और संगठन बिखरे हुए थे। उनकी आवाज़ मज़बूत नहीं थी और कमोबेश यही स्थिति आज भी कायम है। 1986 में रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में की गई और एक कानून के ज़रिए 1993 में इसे वैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया। लेकिन विकलांगजन के कल्याण और पुनर्वास के लिए तब तक भी कानून का अभाव था। इस बीच मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 पारित किया गया, जिसका स्थान मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 ने लिया। विकलांगजन के प्रति संवेदनशीलता की कमी इस सच्चाई से भी समझी जा सकती है कि स्वतंत्र भारत में उन्हें शुरू से एक श्रेणी के रूप में राष्ट्रीय जनगणना से बाहर रखा गया। अत्यधिक दबाव पड़ने पर 2001 की जनगणना में उन्हें अलग स्थान दिया गया। तब तक सैंपल सर्वे के माध्यम से उनकी संख्या का अनुमान लगाया जाता रहा।
भारत में 2006 में विकलांगता सम्बंधी राष्ट्रीय नीति लागू की गई। अगली कड़ी के रूप में 2011 में तैयार किए गए विकलांगजन अधिकार विधेयक का उद्देश्य राष्ट्र संघ संधि के तहत भारत के दायित्वों को कानून का रूप देना था। इसे अमली जामा पहनाते हुए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 पारित किया गया। इसमें पूर्ववर्ती कानून में शामिल 7 विकलांगताओं के स्थान पर 21 विकलांगताएं शामिल की गईं।
एक मत यह भी है कि भारत में डिसेबिलिटी राइट्स मूवमेंट जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। कुछ व्यक्तियों और संगठनों द्वारा विकलांगजन के लिए अच्छे प्रयास ज़रूर किए जा रहे हैं, लेकिन वे विकलांगजन की वास्तविक आबादी के मान से बहुत ही कम हैं। ग्रामीण इलाके और छोटे कस्बे सेवाओं से पूरी तरह वंचित हैं।
पुनः अमेरिका की बात करें तो पुराने समय में लुई ब्रेल और हेलेन केलर ने जिस जुझारूपन का परिचय दिया, उसी राह पर वहां के आधुनिक समय के कुछ विकलांग भी चल रहे हैं। वे न सिर्फ डिसेबिलिटी राइट्स मूवमेंट को नए संदर्भों में आगे बढ़ा रहे हैं बल्कि विकलांगजन का जीवन आसान और बेहतर बनाने के उल्लेखनीय प्रयास भी कर रहे हैं। इनमें एसिड हमले में अपनी दृष्टि गंवा चुके युनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले के छात्र रह चुके जोशुआ मिली हैं जो मैकआर्थर ‘जीनियस ग्रांट’ विजेता हैं और अमेज़न जैसी कंपनी में एडाप्टिव टेक्नॉलॉजी विकसित करते हैं ताकि दृष्टिबाधिता और अन्य विकलांगताओं से प्रभावित व्यक्तियों के लिए उपभोक्ता उपकरण उपयोग में लाना सुगम हो जाए। इसका नतीजा यह हुआ कि विकलांग-अनुकूल उत्पाद उपलब्ध कराने की उम्मीद अब व्यापक स्तर पर सभी उद्योगों से की जाने लगी है। यहीं के एक और छात्र मार्क सटन की कहानी भी इसी तरह प्रेरणादायक है। अपनी दृष्टिबाधिता के कारण उन्हें कंप्यूटर साइंस और वनस्पति विज्ञान की पढ़ाई में घोर उपेक्षा का सामना करना पड़ा, लेकिन वे आज एप्पल कंपनी में कार्य करते हुए सॉफ्टवेयर में ऐसे बदलाव लाने और ऐसे समाधान खोजने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं जिनसे दृष्टिबाधितों के लिए कंप्यूटर और मोबाइल फोन जैसे उपकरण वापरना सुगम हो जाए। इन प्रेरक प्रसंगों का परिणाम यह हुआ कि युनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले के छात्रों का एक नेटवर्क बन गया। इस नेटवर्क के सदस्य अपने-अपने क्षेत्र में अग्रणि रहे हैं और डिसेबिलिटी राइट्स मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं।
बर्कले ही वह स्थान है जहां डिसेबिलिटी राइट्स मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। नेशनल फेडरेशन ऑफ दी ब्लाइंड का जन्म भी बर्कले में ही हुआ और नागरिक अधिकार कानून तथा ब्राउन बनाम बोर्ड ऑफ एजुकेशन के मुकदमे के लिए आधार भी बर्कले में कानून के एक प्रोफेसर के विश्लेषण से प्राप्त हुआ। संभव है संयुक्त राष्ट्र संघ की पहलों और संयुक्त राष्ट्र संधि के लिए आधार भी अमेरिका और उसके जैसे संवेदनशील और अग्रणि देशों द्वारा विकलांगजन के लिए किए गए कार्यों से मिला हो।
इससे यह बात समझ आती है कि भारत में विकलांगजन को अपने अधिकार तब ही मिलेंगे जब वे और उनके परिजन एकजुट होकर अपनी आवाज़ उठाकर दबाव बनाने में कामयाब होंगे। गौरतलब है कि भारतीय संविधान में संशोधन की भी ज़रूरत है ताकि अंतर्राष्ट्रीय संधियों/घोषणा पत्रों के बगैर भी केंद्रीय स्तर पर विकलांगजन के लिए स्वप्रेरित राष्ट्रीय कानून बनाने का मार्ग खुल जाए। संपूर्ण तंत्र, सरकार, संस्थाओं और गैर-विकलांग समुदाय को विकलांगजन की विशेष आवश्यकताओं के प्रति जागरूक और संवेदनशील बनाना होगा। ऐसी कल्याणकारी योजनाएं बनानी होंगी जो विकलांगजन के लिए वास्तव में लाभकारी हों और उनका पैमाना बढ़ती लागत के साथ बढ़ना चाहिए। राष्ट्र संघ संधि और कानून में काफी कुछ लिखा है, लेकिन संवेदनशीलता और ईमानदारी से क्रियान्वयन होने पर ही उसका लाभ मिलना संभव है। अशिक्षा और गरीबी का उन्मूलन होना चाहिए क्योंकि दोनों एक-दूसरे के कारण और परिणाम हैं। शिक्षित विकलांगजन अधिक जागरूक होकर अधिक प्रभावी ढंग से अपनी आवाज़ उठाने में सक्षम होंगे और शिक्षित समाज विकलांगजन के प्रति अपना दायित्व बेहतर ढंग से समझकर संवेदनशीलता के साथ निभा सकेगा। (स्रोत फीचर्स)
नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
Photo Credit : https://mcmscache.epapr.in/post_images/website_350/post_15732875/thumb.png