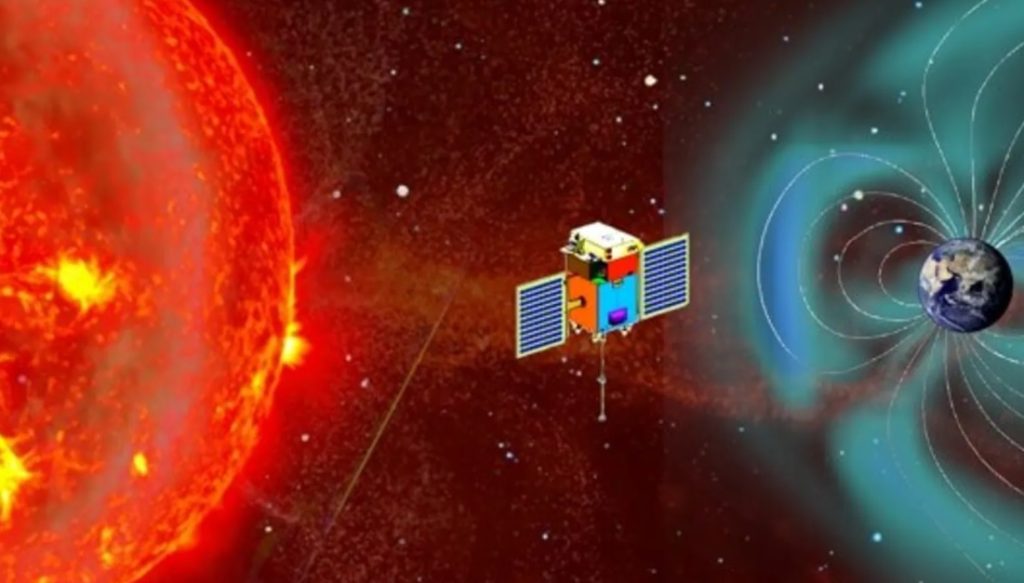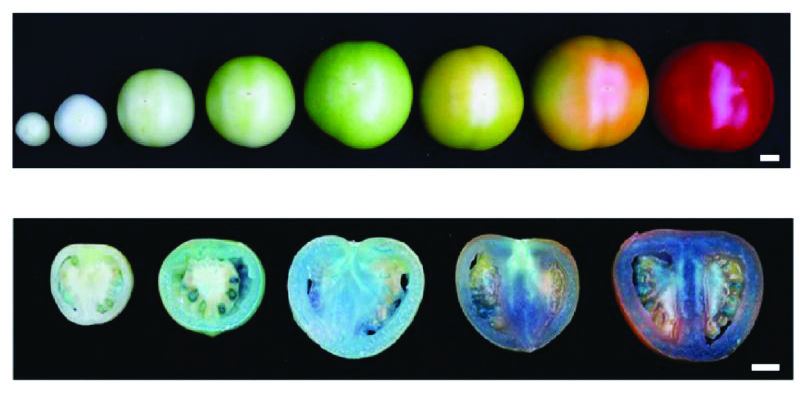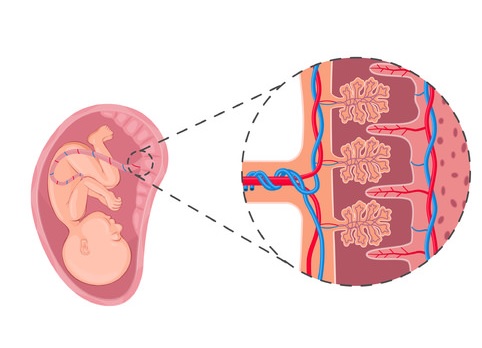भोपाल गैस त्रासदी (Bhopal Gas Tragedy) के चालीस साल हो गए हैं, और इन चालीस सालों में भारत दुनिया का छठवां सबसे बड़ा रसायन उत्पादक देश बन गया है। तेज़ी से बढ़ते रसायन उद्योग के साथ भारत में रासायनिक दुर्घटनाएं (chemical accidents) भी बढ़ रही हैं। सवाल है कि ऐसा क्यों है?
कोविड-19 महामारी (2020-2023) के दौरान भारत में 29 रासायनिक दुर्घटनाएं हुईं। इन दुर्घटनाओं में 118 मौतें हुईं और लगभग 257 लोग घायल हुए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने इन दुर्घटनाओं का कारण प्लांट की खराबी, रासायनिक रिसाव (chemical leakage), विस्फोट (explosion) और फैक्ट्री में आग लगना पाया है।
वैज्ञानिकों के एक समूह साइंटिस्ट फॉर पीपल (scientist for people) ने 2021 में एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद भी रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए सुरक्षा सम्बंधी नियम-कायदों में कोई सुधार नहीं हुआ है।
भारत का फलता-फूलता औद्योगिक क्षेत्र लगातार ट्रेड सीक्रेट संरक्षण कानून (Trade secret protection law) की मांग कर रहा है। ऐसे कानून कंपनियों को बौद्धिक संपदा की आड़ में महत्वपूर्ण जानकारी गोपनीय रखने की अनुमति देते हैं। एक ओर जहां ट्रेड सीक्रेट को गोपनीय रखना किसी कंपनी को प्रतिस्पर्धात्मक फायदा दे सकता है, वहीं दूसरी ओर, पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बंधी जोखिम पैदा करने वाली कंपनियां अक्सर इस गोपनीयता का दुरुपयोग करती हैं। ट्रेड सीक्रेट संरक्षण कानून की अनुपस्थिति में, कंपनियां फिलहाल व्यावसायिक प्रक्रियाओं की जानकारी उजागर होने से रोकने के लिए गैर-प्रकटीकरण (नॉन-डिसक्लोज़र) समझौतों पर निर्भर हैं।
पश्चिम बंगाल नेशनल युनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेज़ (west Bengal national university of juridical sciences) के प्रोफेसर अनिरबन मजूमदार कहते हैं, “कंपनियां खुद को बचाने के लिए गैर-प्रकटीकरण समझौतों का उपयोग करती हैं, और भारत में ट्रेड सीक्रेट को लेकर कोई विशिष्ट कानून नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम(RTI), 2005 की धारा 8(i) के तहत सार्वजनिक हित के उद्देश्य से बौद्धिक संपदा और ट्रेड सीक्रेट से सम्बंधित जानकारी मांगने की अनुमति देता है, लेकिन यह अधिनियम निजी कंपनियों पर लागू नहीं होता है।“
मजूमदार एक उदाहरण के तौर पर भोपाल गैस त्रासदी का हवाला देते हैं। “डॉऊ केमिकल्स(Dow Chemicals), जिसने 2001 में यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन (Union Carbide Corporation) का अधिग्रहण किया था, ने रिसी हुई गैस के रासायनिक संघटन (chemical composition) का खुलासा करने से इन्कार कर दिया था। यदि संघटन उजागर कर दिया जाता तो उसके आधार पर पीड़ितों का प्रभावी ढंग से इलाज किया जा सकता था। यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन 1950 के दशक से ही ट्रेड सीक्रेट संरक्षण का उपयोग कर रहा है।
मिक का उपयोग जारी है
यहां भोपाल गैस त्रासदी एक प्रासंगिक उदाहरण होगा क्योंकि भारत में मिथाइल आइसोसाइनेट (mic) का उपयोग अब तक जारी है। मिक को खतरनाक रसायनों के निर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989 (अनुसूची 1) के तहत एक खतरनाक रसायन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
डाउन टू अर्थ द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मिक के उपयोग की मात्रा और स्थानों के बारे में सवाल के जवाब में रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग ने जानकारी नहीं दी। मजूमदार बताते हैं कि कुछ रिपोर्टें इस बात की पुष्टि करती हैं कि डाऊ केमिकल्स सिंगापुर स्थित कंपनी मेगा वीसा के माध्यम से भारत में यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन के उत्पादों का व्यापार जारी रखे हुए है।
टॉक्सिक्स वॉच अलाएंस के गोपाल कृष्ण ने उजागर किया है कि कई खतरनाक रसायनों (hazardeous chemicals) को अभी भी ‘खतरनाक’ के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है या ‘दर्ज’ करने योग्य ही नहीं माना गया है। उनका आरोप है कि भोपाल में यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन के अनुसंधान और विकास केंद्र ने अमेरिका में युद्ध हथियार निर्माण के लिए प्रतिबंधित गैसों और रसायनों के साथ प्रयोग किए हैं। त्रासदी के लिए ज़िम्मेदार गैस की सटीक पहचान आज भी अज्ञात है।
यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन का भोपाल संयंत्र कीटनाशक कार्बेरिल (sevin) के निर्माण के लिए मिक का उपयोग एक मध्यवर्ती के रूप में करता था। इसे त्रासदी के लगभग तीन दशक बाद 8 अगस्त, 2018 को भारत में प्रतिबंधित किया गया। प्रतिबंध लगाने में इस देरी का कारण बताया नहीं गया है।
हमारा भोजन
इस बीच, कई खतरनाक कृषि रसायन नियमन/नियंत्रण से बाहर बने हुए हैं। जैसे संश्लेषित कीटनाशक डीडीटी (DDT) (डाइफिनाइलट्राइक्लोरोइथेन), जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए खतरनाक है। वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से इसे समाप्त किए जाने के निर्णय के बावजूद भारत में, एचआईएल लिमिटेड (HIL Limited) के माध्यम से अफ्रीकी देशों को निर्यात के लिए इसका उत्पादन जारी है। 17वीं लोकसभा की रसायन और उर्वरक स्थायी समिति (2023-24) के अनुसार, सरकार ने डीडीटी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की बात को दिसंबर 2024 तक के लिए टाल दिया है।
2022 में, पेस्टिसाइड्स एक्शन नेटवर्क इंडिया (PAN India) ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी: भारत में क्लोरपाइरीफॉस, फिप्रोनिल, एट्राज़ीन और पैराक्वाट डाइक्लोराइड की स्थिति। रिपोर्ट में मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण और अन्य जीवों पर गंभीर जोखिमों के कारण अत्यधिक विषैले कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने की तत्काल आवश्यकता बताई गई है।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने अपनी 1989 की अधिसूचना के माध्यम से, खतरनाक रसायन (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियमों की अनुसूची 1 के तहत 684 खतरनाक रसायनों को सूचीबद्ध किया है। अलबत्ता, इस सूची से कई खतरनाक रसायन नदारद हैं। गोपाल कृष्ण के अनुसार, यह एक अत्यंत सीमित सूची है। भारत में अब तक एस्बेस्टस जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित रसायनों का उपयोग हो रहा है।
भारत में अनियंत्रित या अल्प-नियंत्रित संश्लेषित रसायनों का एक और उदाहरण है: पर-एंड-पॉलीफ्लोरोएल्काइल पदार्थ (PFAS), जिन्हें ‘शाश्वत रसायन’ भी कहा जाता है। नॉन-स्टिक बर्तन, खाद्य पैकेजिंग और जल-रोधी उत्पादों में खूब उपयोग किए जाने वाले PFAS पर्यावरण में बने रहने और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। युरोपीय रसायन एजेंसी ने युरोप में इन्हें नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए हैं, लेकिन इस संदर्भ में भारत में कोई प्रगति नहीं हुई है।
अक्टूबर 2024 में डाउन टू अर्थ ने एक बार फिर सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मिक और अन्य खतरनाक रसायनों पर जानकारी तलब की थी। रसायन विभाग का जवाब था, “सूचना अधिकारी के पास ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।” यदि ट्रेड सीक्रेट संरक्षण विधेयक, 2024 पारित हो जाता है तो कंपनियों को, राष्ट्रीय आपात स्थिति या सार्वजनिक हित के मामलों को छोड़कर, महत्वपूर्ण जानकारी रोकने की और अधिक शक्ति मिल जाएगी।
भारत में रसायन उद्योग का विस्तार जारी है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय का अनुमान है कि 2040 तक यह 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। रासायनिक प्रबंधन और सुरक्षा नियमों का मसौदा अधूरा है: भारत में अमेरिका या युरोपीय संघ के जैसे व्यापक नियमों का अभाव है। इसके अलावा, भारत में न तो कोई रासायनिक सूची है या न ही रासायनिक पंजीकरण अनिवार्य है।
पब्लिक पॉलिसी और PAN India से जुड़े नरसिम्हा रेड्डी दोंती का कहना है, “हमारे पास शस्त्र कानून जैसे मज़बूत कानून का अभाव है। बंदूक रखने पर सात वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा हो सकती है, लेकिन खतरनाक रसायनों से भरा डिब्बा खरीदने पर अक्सर कोई परिणाम नहीं भुगतना पड़ता। हमें क्रियान्वयन के लिए सख्त कानून, नियम और संस्थागत तंत्र की आवश्यकता है।”
टॉक्सिक्स लिंक के पीयूष महापात्रा बताते हैं कि मौजूदा नीतियां औद्योगिक हितों को प्राथमिकता देती हैं और रासायनिक प्रबंधन और खतरे के वर्गीकरण को नज़रअंदाज़ करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समझौतों में शामिल होने के बावजूद नीतियों का कार्यान्वयन बदतर बना हुआ है।
लगभग पांच साल पहले 2019 में, डाउन टू अर्थ ने ई-मेल के माध्यम से बातचीत के एक लंबी शृंखला में देश में मिक के उत्पादन और उपयोग पर सरकार से जानकारी मांगी थी। उत्तर मिला: “रसायन विभाग के संयुक्त सचिव मिक जैसी विषाक्त गैस की अधिसूचना पर काम कर रहे हैं। उनके संपर्क में रहें।” अब तक मंत्रालय की ओर से ऐसी कोई अधिसूचना नहीं आई है। रसायन (प्रबंधन और सुरक्षा) नियमों का मसौदा तैयार है, लेकिन अभी तक इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है।
हालांकि भारत में रासायनिक उद्योग के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करने वाले 15 कानून और 19 नियम हैं, लेकिन उनमें से कोई भी विशेष रूप से रसायनों के उपयोग, उत्पादन और सुरक्षा को पूरे उद्योग के स्तर पर संबोधित नहीं करता। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पूर्व वैज्ञानिक डीडी बसु ने ज़ोर देकर कहा है, “हमें रासायनिक उपयोग, उत्पादन और सुरक्षा को विनियमित करने के लिए व्यापक कानून की आवश्यकता है।”
अन्य देश हानिकारक रसायनों पर नियंत्रण और प्रतिबंध लगाने के प्रयासों को गति दे रहे हैं, लेकिन भारत इसमें अभी भी पिछड़ा है। दोंती का निष्कर्ष है, “भारत को एक मज़बूत नियामक ढांचे की आवश्यकता है जो न केवल ट्रेड सीक्रेट को संबोधित करता हो बल्कि आपूर्ति शृंखलाओं में पारदर्शिता भी सुनिश्चित करता हो। उद्योगों ने ऐसी प्रणालियां बनाई हैं जो उन्हें जांच से बचाती हैं जबकि जनता को नुकसान पहुंचाती हैं।” (स्रोत फीचर्स)
यह लेख मूलत: डाउन टू अर्थ में अंग्रेज़ी में Bhopal Gas Tragedy at 40: Harmful chemicals, including methyl isocyanate, are still used in India due to lax laws; can this change? शीर्षक से प्रकाशित हुआ था।
नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
Photo Credit : https://media.assettype.com/newindianexpress%2F2024-04%2Fd5b81c46-3644-4ba8-9c51-da8342bf216b%2FBHOPAL.jpg?w=768&auto=format%2Ccompress&fit=max