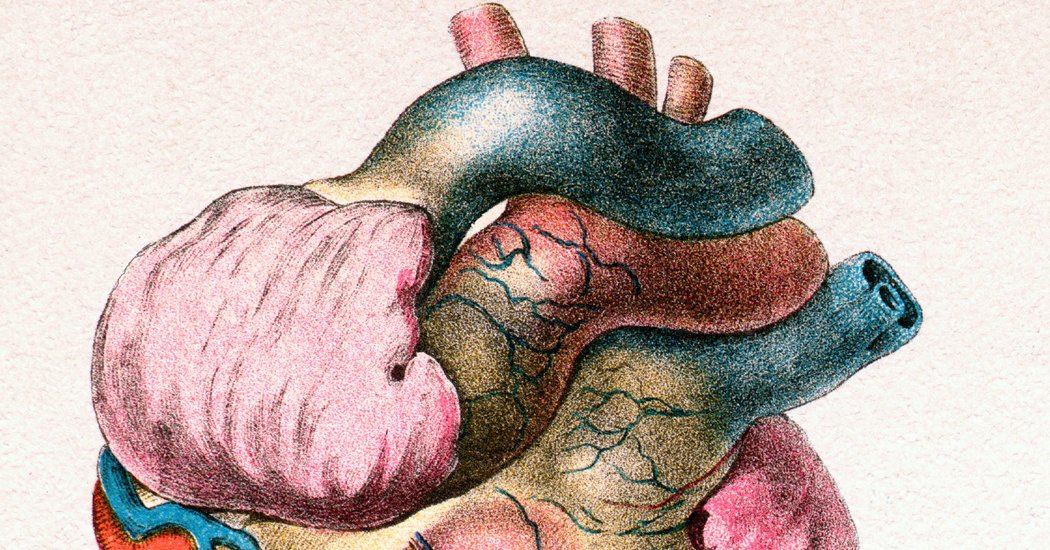एक भारी-भरकम गोलाकार तारे पर विचार कीजिए जो बाह्य अंतरिक्ष में विपुल मात्रा में विकिरण छोड़ रहा है। ऐसे किसी तारे के आसपास गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का व्यवहार कैसा होगा? अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा 1915 में प्रतिपादित क्रांतिकारी सामान्य सापेक्षता सिद्धांत को लागू करके कई सवालों को संबोधित किया जा सकता था। उपरोक्त सवाल उनमें से एक महत्वपूर्ण सवाल था। और इसका समाधान सबसे पहले गणितज्ञ और खगोलविद पी.सी. वैद्य (1918-2010) ने निकाला था। इसे वैद्य मेट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। मई में उनकी जन्म शती थी।
सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत को दस ‘क्षेत्र समीकरणों’ द्वारा व्यक्त किया जाता है जो समूचे ब्रह्मांड में वैध हैं। ये समीकरण कतिपय सरलीकृत मान्यताओं के अंतर्गत कुछ सटीक समाधान की गुंजाइश प्रदान करते हैं। पहला सटीक समाधान सिद्धांत के प्रतिपादन के फौरन बाद सामने आया था जब जर्मन वैज्ञानिक कार्ल श्वाजऱ्चाइल्ड ने अंतरिक्ष में विकिरण का उत्सर्जन न करने वाले किसी गोलाकार पिंड के आसपास के क्षेत्र का विवरण प्रस्तुत किया था।
इसके पूरे 26 साल बाद वैद्य ने 1943 में विकिरण करते गोलाकार पिंड के क्षेत्र की गणना की थी। 1960 के दशक में रेडियो दूरबीनों की मदद से दूरस्थ निहारिकाओं के मध्य में क्वासर (क्वासी-स्टेलर रेडियो स्रोतों) की खोज की गई जो विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। वैद्य ने बाद में याद करके बताया था, “न्यूटन का (गुरुत्वाकर्षण) सिद्धांत इन पिंडों के अत्यंत तीव्र गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के संदर्भ में अपर्याप्त साबित हुआ था और (इनके विवरण के लिए) आइंस्टाइन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत की आवश्यकता थी।”
वैद्य का समाधान इन परिस्थितियों के अध्ययन के लिए आदर्श था, और इसके चलते वे उच्च-ऊर्जा खगोल-भौतिकविदों की दुनिया में शामिल कर लिए गए।
महान, अनोखे
आने वाले दशकों में उन्होंने सामान्य सापेक्षता और खगोल-भौतिकी के संगम बिंदु पर कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। उन्होंने सटीक समाधानों के अलावा अति-विशाल पिंडों और ब्लैक होल्स जैसे विषयों पर काम किया। अकेले या अपने शोध छात्रों के साथ काम करते हुए उन्होंने नेचर, फिजि़कल रिव्यू लेटर्स, एस्ट्रोफिजि़कल जर्नल और करंट साइन्स जैसी शोध पत्रिकाओं में कई शोध पत्र प्रकाशित किए।
वैद्य एक संस्था-निर्माता भी थे। इंडियन एसोसिएशन फॉर जनरल रिलेटिविटी के संस्थापक सदस्य के रूप में उन्होंने भारत में इस क्षेत्र में काम कर रहे वैज्ञानिकों को साथ लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। इन वैज्ञानिकों में सी.वी. विश्वेश्वरा, नरेश दधीच और जयंत नार्लीकर जैसे वैज्ञानिक शामिल थे। जयंत नार्लीकर आगे चलकर इंटरयुनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजि़क्स (IUCAA, पुणे) के प्रथम निदेशक बने।
हालांकि भारत में सामान्य सापेक्षता अनुसंधान के शुरुआती केंद्र जयंत नार्लीकर के पिता वी.वी. नार्लीकर और एन. आर. सेन के नेतृत्व में स्थापित हुए थे, अगली पीढ़ी पर वैद्य का ज़बर्दस्त प्रभाव रहा। सामान्य सापेक्षता के क्षेत्र में कार्यरत वैज्ञानिक कलकत्ता (अब कोलकाता) के गणितज्ञ अमल कुमार रायचौधरी के साथ-साथ वैद्य को अपना मार्गदर्शक मानते थे और 1985 में इन दोनों वैज्ञानिकों के सम्मान में पुस्तिका का प्रकाशन किया गया था।
इस बात में कोई संदेह नहीं कि पी. सी. वैद्य अव्वल दर्जे के वैज्ञानिक थे और आइंस्टाइन से लेकर स्टीफन हॉकिंग और गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज करने वाली लिगो टीम तथा अन्य प्रायोगिक वैज्ञानिकों की परंपरा के हिस्से थे। और फिर भी – हालांकि मैं प्रशिक्षण और पेशे से विज्ञान का इतिहासकार हूं – मैंने चंह महीनों पहले तक पी.सी. वैद्य का नाम तक नहीं सुना था। मैंने उनका नाम पहली बार तब सुना जब एक मित्र ने हॉकिंग के जीवन और कार्य पर व्याख्यान देते हुए उनका जि़क्र किया।
यह मेरे अज्ञान का द्योतक हो सकता है किंतु एक गैर-वैज्ञानिक जनमतसंग्रह से लगता है कि बात इतनी ही नहीं है। गुजरात का यह महान व्यक्तित्व भारत के घर-घर में सी.वी. रामन, मेघनाथ साहा, एस.एस. भटनागर, सुब्रामण्यन चंद्रशेखर या होमी भाभा जैसा नाम नहीं बन पाया।
इसे कैसे समझें? इसका कुछ सम्बंध तो इस बात से है कि जिस परिवेश में उन्होंने अपना कैरियर बनाया और जिस असाधारण जीवन शैली को उन्होंने अपनाया। कई स्रोतों से हम उस कैरियर को पुनर्निर्मित कर सकते हैं। इनमें उनकी गुजराती स्मरण पुस्तिका चॉक एंड डस्टर तथा उनके सम्बंधियों और सहकर्मियों द्वारा लिखे गए जीवन वृत्त शामिल हैं।
शुरुआती वर्ष
प्रहलाद चुन्नीलाल वैद्य (कुछ लोगों के लिए वैद्य साहेब) का जन्म 1918 में जूनागढ़ रियासत के एक गांव शाहपुर में हुआ था। वे एक डाक अधिकारी के द्वितीय पुत्र थे। बचपन में ही उनके माता-पिता गुज़र गए और उनका लालन-पालन भावनगर के नज़दीक कुछ रिश्तेदारों ने किया, जहां 1933 तक वे अल्फ्रेड हाई स्कूल में पढ़े।
उनके भाई मधुसूदन को बंबई (अब मुंबई) में स्कूल शिक्षक की नौकरी मिल गई और पी. सी. वैद्य ने अपनी स्कूल शिक्षा वहीं पूरी की। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स से बी.एससी. (और आगे चलकर एम.एससी.) करने से पहले वे जोगेश्वरी स्थित इस्माइल यूसुफ कॉलेज में पढ़े। स्नातक शिक्षा के दौरान उन्हें डिस्टिंक्शन मिला और स्नातकोत्तर परीक्षा में बंबई विश्वविद्यालय के टॉपर रहे।
इस दौर में उनके व्यक्तित्व पर एक गहरी छाप बंबई विश्वविद्यालय में 1937 में वी.वी. नार्लीकर (कैंब्रिज विश्वविद्यालय में अध्ययन के बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर) द्वारा दिए गए व्याख्यानों ने डाली। यहीं पी.सी. वैद्य ने पहली बार सुना था कि विकिरण करते तारों के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का विवरण अब तक सामान्य सापेक्षता के परिप्रेक्ष्य में नहीं दिया गया है।
उनके अकादिमक कैरियर के बावजूद, जिस ढंग से पी.सी. वैद्य का शोध कैरियर शुरू हुआ, उसमें संयोग का कुछ पुट अवश्य है। भावनगर में पी. सी. वैद्य और उनके भाई पर गांधी के विचारों का काफी असर पड़ा था। अब राजकोट में एक कॉलेज शिक्षक के रूप में थोड़े दिन काम करने के बाद उन्होंने अपने कैरियर में एक गैर-परंपरागत कदम उठाया। 1941 में उन्होंने बंबई लौटकर एक गांधी-प्रेरित स्वैच्छिक संस्था स्थापित की। अहिंसक व्यायाम संघ नामक यह संस्था सत्याग्रहियों के प्रशिक्षण के लिए बनाई गई थी।
यह कई भारतीय युवाओं के लिए जुनून का दौर था क्योंकि इसी समय भारतीय नेताओं ने ब्रिटेन द्वारा भारत को एकतरफा ढंग से द्वितीय विश्व युद्ध में झोंकने के निर्णय के खिलाफ संघर्ष करते हुए भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कर दी थी। यह पी. सी. वैद्य के लिए निराशा का कारण बना कि व्यायाम संघ की प्रेरक शक्ति पृथ्वी सिंह की वैचारिक उलझनों के चलते संस्था को समेट दिया गया। सिंह का वैचारिक झुकाव कम्यूनिज़्म की ओर था और वे ब्रिटिशों का विरोध करने में खुद को असमर्थ पा रहे थे क्योंकि ब्रिटिश तब सोवियत संघ के सहयोगी थे।
खुद को मझधार में पाकर, पी. सी. वैद्य ने वी.वी. नार्लीकर का रुख किया। उन्होंने बनारस में नार्लीकर को चिट्ठी लिखकर पूछा कि क्या वे एक अनौपचारिक शोध छात्र के रूप में उनके साथ काम कर सकते हैं। अपनी बचत के भरोसे पी.सी. वैद्य अपने परिवार को लेकर बनारस आ गए, जहां उन्होंने नार्लीकर के मार्गदर्शन में काम करते हुए 1942 से कई शोध पत्र प्रकाशित किए। इनमें से एक – इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स द्वारा प्रकाशित करंट साइन्स में 1943 में प्रकाशित शोध पत्र – उनकी पहली बड़ी सफलता थी। इस शोध पत्र का शीर्षक था: दी एक्सटरनल फील्ड ऑफ ए रेडिएटिंग स्टार इन जनरल रिलेटिविटी। इस पर्चे ने विज्ञान जगत को वैद्य मेट्रिक्स की सूचना दी।
वैद्य ने 1950 के शुरुआती दशक में प्रकाशित शोध पत्रों में इसे विस्तार दिया। ऐसे में कोई अचरज नहीं कि पी.सी. वैद्य ने नार्लीकर के साथ बिताए अपने वर्षों को ‘काशी यात्रा’ की संज्ञा दी जिसने उन्हें अगले जीवन के लिए नहीं बल्कि इसी जीवन के शेष वर्षों के लिए तैयार किया।
संस्था निर्माण
जब बचत के पैसे चुक गए, तो वैद्य ने सूरत के एक कॉलेज में अध्यापक की नौकरी ले ली। आगे चलकर उन्होंने नवोदित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) में एक शोध छात्र के रूप में दाखिला लिया और 1948 में पीएच.डी. पूरी की। टीआईएफआर उस समय विकसित हो रहा था और वैद्य को होमी भाभा के साथ काम करने का मौका मिला। यह बात शायद अविश्वसनीय लगे किंतु पी.सी. वैद्य को बंबई छोड़ना पड़ा था क्योंकि परिवार के रहने के लिए वहां उन्हें मकान नहीं मिला।
तब पी. सी. वैद्य गुजरात में आनंद के नज़दीक उभरते शैक्षणिक शहर वल्लभ विद्यानगर में नए-नए खुले विट्ठलभाई पटेल कॉलेज में प्रोफेसर बने। उनके जीवन पर बनी आयूका-विज्ञान प्रसार की एक फिल्म में उन्होंने बताया है कि उस समय वे बगैर छत के कमरे में पढ़ाया करते थे। मगर वहां उन्होंने अपने छात्रों की जो बुनियाद तैयार की वह बहुत मज़बूत थी। जैसा कि उनके भतीजे अरुण वैद्य (जो स्वयं एक प्रतिष्ठित गणितज्ञ हैं) ने बताया, पी. सी. वैद्य न सिर्फ अपने शोध कार्य के लिए बल्कि उनके द्वारा आयोजित खेलकूद शिविरों व अन्य गतिविधियों के लिए भी याद किए जाते हैं। लगता है व्यायाम संघ के उनके दिन फालतू नहीं गए।
अन्य कॉलेजों में अध्यापन करने के बाद, वैद्य ने गुजरात विश्वविद्यालय में गणित विभाग स्थापित करने में योगदान दिया (1959)। यहीं उन्होंने अपना शेष कार्य-जीवन व्यतीत किया। यहां उन्होंने कई शोध छात्र तैयार किए। आगे चलकर उन्हें प्रशासनिक जि़म्मेदारियां सौंपी गई। 1971 में वे गुजरात लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने और 1977 में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य निर्वाचित किए गए। इसके बाद वे गुजरात विश्वविद्यालय के उपकुलपति रहे।
वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में अपनी हैसियत और उच्च पदों पर आसीन रहने के बावजूद, पी. सी. वैद्य कभी अपनी जड़ें नहीं भूले। आजीवन गांधीवादी रहे वैद्य की पहचान खादी के कुर्ते, सफेद गांधी टोपी और सायकिल से जुड़ी रही। जिन संस्थाओं की स्थापना को लेकर वे गर्व महसूस करते थे वे हर स्तर पर गणित शिक्षण को बेहतर बनाने से सम्बंधित थीं। इनमें गुजरात गणित मंडल (स्थापना 1963) शामिल है जो आज भी एक जीवंत संस्था है। इसी वर्ष उन्होंने एक पत्रिका सुगणितम की स्थापना की थी जो शिक्षकों व छात्रों के लिए गणित का एक उम्दा संसाधन है।
विनम्रता
वैद्य उस समय तक एक परिपक्व शोधकर्ता बन चुके थे जब नव-स्वतंत्र भारत विज्ञान में भारी निवेश कर रहा था। वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद (CSIR) प्रयोगशालाओं के अपने नेटवर्क में विस्तार कर रहा था, अंतरिक्ष कार्यक्रम आकार ले रहा था और परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम पर पैसे और प्रतिष्ठा की बौछार की जा रही थी। मगर इन सबका एक उपयोगितावादी रुझान था जबकि वैद्य ज़्यादा ‘बुनियादी’ अनुसंधान कर रहे थे।
जैसा कि एक भौतिक शास्त्री साथी ने मुझे बताया था, पी. सी. वैद्य का क्षेत्र (सामान्य सापेक्षता) अपेक्षाकृत गूढ़ था। यह विषय भारत में स्नातकोत्तर स्तर भी कहीं-कहीं ही पढ़ाया जाता था। ज़ाहिर है, इसने लोगों का ध्यान उस तरह नहीं खींचा जैसे परमाणु ऊर्जा या रॉकेट खींचते हैं। परिणाम यह रहा कि वैद्य ने अपना लगभग पूरा कैरियर विज्ञान के मान्य केंद्रों से दूर ही व्यतीत किया और शोध में उनके योगदान को बहुत थोड़े से वैज्ञानिक ही समझते हैं।
अलबत्ता, वैद्य का कैरियर सिर्फ इन परिस्थितियों का नहीं बल्कि उनके निर्णयों का भी परिणाम था। वैद्य ने कभी सार्वजनिक परिदृश्य में रहने की इच्छा नहीं की। वे एक ‘जड़ें जमाए विश्व नागरिक’ थे जो पूरी दुनिया से संवाद करते थे किंतु सबसे प्रसन्न अपनी धरती पर ही रहते थे। वे अपनी मातृभाषा और अपने आसपास के लोगों की भाषा की मदद से ज्ञान का प्रजातांत्रीकरण करना चाहते थे। वे गांधीवादी परंपरा में ‘रचनात्मक कार्यकर्ता’ थे।
1990 के दशक के अंतिम वर्षों में भी, बुलेटिन ऑफ दी एस्ट्रॉनॉमिकल सोसायटी ऑफ इंडिया के संपादक के पत्र के जवाब में अपनी निशस्त्र कर देने वाली विनम्रता के साथ उन्होंने कहा था, “मैं हमेशा से स्वयं को एक शिक्षक मानता आया हूं और इतने वर्षों तक गणित पढ़ाकर ही अपनी जीविका अर्जित की है। यदि प्रतिष्ठित खगोल शास्त्रीय सोसायटी मुझे एक प्रतिष्ठित खगोल शास्त्री मानती है, तो मुझे गर्व महसूस हुआ और मैंने सोचना शुरू किया कि यह गणित शिक्षक एक खगोल शास्त्री के रूप में कैसे तबदील हो गया।” शायद यह तबदीली सितारों पर अंकित थी। (स्रोत फीचर्स)
नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
फोटो क्रेडिट : the wire