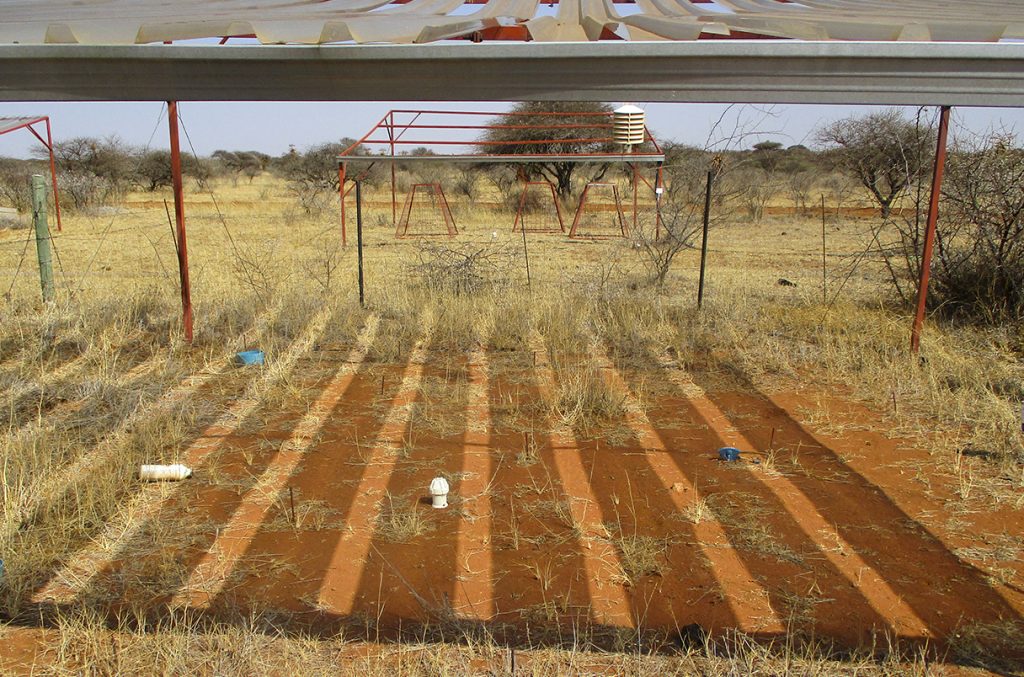हॉलीवुड की एनिमेशन फिल्मों में नाचते, गाते, शरारत करते लीमर ज़रूर दिखेंगे। ये सिर्फ मैडागास्कर द्वीप पर ही पाए जाते हैं जो प्रकृतिविदों के लिए हमेशा से दिलचस्प जंतुओं का आवास स्थल रहा है।
मैडागास्कर में पाए जाने वाले कई जंतुओं का सम्बंध दूरस्थ भारत (दूरी 3800 कि.मी.) में पाए जाने वाले वंशों से दिखता है, बनिस्बत अफ्रीका के जंतुओं से जबकि अफ्रीका यहां से महज 413 कि.मी. दूर है। यह प्रकृतिविदों के लिए एक ‘अबूझ पहेली’ रही है।
प्राणि वैज्ञानिक फिलिप स्क्लेटर हैरान थे कि लीमर और सम्बंधित जंतु व उनके जीवाश्म मैडागास्कर और भारत में तो पाए जाते हैं लेकिन मैडागास्कर के निकट स्थित अफ्रीका या मध्य पूर्व में अनुपस्थित हैं। 1860 के दशक में उन्होंने प्रस्तावित किया था कि किसी समय भारत और मैडागास्कर के बीच एक बड़ा द्वीप या महाद्वीप मौजूद रहा होगा, जो दोनों स्थानों के बीच सेतु का कार्य करता था। समय के साथ यह द्वीप डूब गया। इस प्रस्तावित जलमग्न द्वीप को उन्होंने लेमुरिया नाम दिया था।
स्क्लेटर की इस परिकल्पना ने हेलेना ब्लावात्स्की जैसे तांत्रिकों को आकर्षित किया, जिनका यह मानना था कि यही वह स्थान होना चाहिए जहां मनुष्यों की उत्पत्ति हुई थी।
देवनेया पवनर जैसे तमिल धार्मिक पुनरुत्थानवादियों ने भी इस विचार को अपनाया और इसे एक तमिल सभ्यता की संज्ञा दी। साहित्य और पांडियन दंतकथाओं में यह समुद्र में जलगग्न सभ्यता के रूप में वर्णित है। वे इस जलमग्न महाद्वीप को कुमारी कंदम कहते थे।
महाद्वीपों का खिसकना
स्क्लेटर के विचारों ने तब समर्थन खो दिया जब एक अन्य ‘हैरतअंगेज़’ सिद्धांत – महाद्वीपीय खिसकाव या विस्थापन – ने स्वीकृति प्राप्त करना शुरू किया। प्लेट टेक्टोनिक्स नामक इस सिद्धांत के अनुसार बड़ी-बड़ी प्लेट्स – जिन पर हम खड़े हुए हैं (या चलते-फिरते हैं, रहते हैं) – पिघली हुई भूमिगत चट्टानों पर तैरती हैं और एक-दूसरे के सापेक्ष ये प्रति वर्ष 2-15 से.मी. खिसकती हैं। तकरीबन 16.5 करोड़ वर्ष पहले गोंडवाना नामक विशाल भूखंड दो हिस्सों में बंट गया था – इसके एक टुकड़े में वर्तमान के अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका थे और दूसरे टुकड़े में भारत, मैडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका थे।
फिर लगभग 11.5 करोड़ साल पूर्व मैडागास्कर और भारत एक साथ इससे टूटकर अलग हो गए थे। लगभग 8.8 करोड़ साल पहले, भारत उत्तर की ओर बढ़ने लगा और इसने रास्ते में कुछ छोटे-छोटे भू-भाग (द्वीप) छोड़ दिए जिससे सेशेल्स बना। यह टूटा हुआ हिस्सा लगभग 5 करोड़ साल पहले युरेशियन भू-भाग से टकराया जिससे हिमालय और दक्षिण एशिया बने।
लगभग 11.5 करोड़ साल पहले डायनासौर का राज था। इस समय तक कई जीव रूपों का विकास भी नहीं हुआ था। भारत और मैडागास्कर में पाए जाने वाले डायनासौर के जीवाश्म काफी एक जैसे हैं, और ये अफ्रीका और एशिया में पाई जाने वाली डायनासौर प्रजातियों के समान नहीं हैं जो गोंडवाना के टूटने का समर्थन करता है। भारत और मैडागास्कर दोनों जगहों पर लैप्लेटोसॉरस मेडागास्करेन्सिस के अवशेष पाए गए हैं।
आणविक घड़ियां
आणविक घड़ी एक शक्तिशाली तकनीक है जिसका उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि जैव विकास के दौरान कोई दो जीव एक-दूसरे से कब अलग हुए थे। यह तकनीक इस अवलोकन पर आधारित है कि आरएनए या प्रोटीन अणु की शृंखला में वैकासिक परिवर्तन काफी निश्चित दर पर होते हैं। जैसे दो जीवों के हीमोग्लोबिन जैसे प्रोटीन में अमीनो एसिड में अंतर आपको यह बता सकता है कि उनके पूर्वज कितने वर्ष पहले अलग हो गए थे। आणविक घड़ियां अन्य साक्ष्यों (जैसे जीवाश्म रिकॉर्ड) से काफी मेल खाती हैं।
दक्षिण भारत और श्रीलंका में मीठे पानी और खारे पानी की मछलियों के सिक्लिड परिवार के केवल दो वंश हैं – एट्रोप्लस (जो केरल की एक खाद्य मछली है, जहां इसे पल्लती कहा जाता है) और स्यूडेट्रोप्लस। आणविक तुलना से पता चलता है कि एट्रोप्लस के निकटतम सम्बंधी मैडागास्कर में पाए जाते हैं, और इनके साझा पूर्वज 16 करोड़ वर्ष पहले अफ्रीकी सिक्लिड्स से अलग हो गए थे। चौथे तरह के सिक्लिड दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, इस प्रकार ये गोंडवाना के छिन्न-भिन्न होने का समर्थन करते हैं।
एशिया, मैडागास्कर और अफ्रीका में जीवों के वितरण में भारत एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गोंडवाना के जीव भारत से निकलकर फैले। कुछ अन्य जीव यहां आकर बस गए। उदाहरण के लिए, मीठे पानी के एशियाई केंकड़े (जेकार्सिन्यूसिडी कुल)अब समूचे दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं लेकिन उनके सबसे हालिया साझा पूर्वज भारत में विकसित हुए थे। सूग्लोसिडे नामक मेंढक कुल सिर्फ भारत और सेशेल्स में पाया जाता है।
गढ़वाल के एचएनबी विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय और जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने गुजरात की वस्तान लिग्नाइट खदान से प्राप्त जीवाश्म में प्रारंभिक भारतीय स्तनधारी – चमगादड़ की एक प्रजाति, और प्रारंभिक युप्राइमेट – एक आदिम लीमर की पहचान की है। ये लगभग 5.3 करोड़ वर्ष पूर्व के जीवाश्म हैं, जो भारत-युरेशियन प्लेट्स के टकराने (या उससे ठीक पहले) का समय है।
लीमर्स के बारे में क्या? मैडागास्कर बहुत बड़ा द्वीप है, यहां विविध तरह की जलवायु परिस्थितियां हैं। साक्ष्य बताते हैं कि अफ्रीका से समुद्र पार करके एक पूर्वज प्राइमेट यहां आया था। कोई बंदर, वानर या बड़े शिकारी इसे पार नहीं कर सके थे, इसलिए यहां दर्जनों लीमर प्रजातियां फली-फूलीं।
भारत में लोरिस पाए जाते हैं, जो लीमर के निकटतम सम्बंधी हैं। ये शर्मीले, बड़ी और आकर्षक आंखों वाले निशाचर वनवासी हैं। माना जाता है कि ये भी समुद्री रास्ते से अफ्रीका से यहां की यात्रा में जीवित बच गए। सुस्त लोरिस ज़्यादातर पूर्वोत्तर राज्यों में पाए जाते हैं, और छरहरे लोरिस कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के सीमावर्ती क्षेत्र में पाए जाते हैं। (स्रोत फीचर्स)
नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
Photo Credit : https://th-i.thgim.com/public/incoming/ueffmr/article65728987.ece/alternates/LANDSCAPE_615/AFP_32AD8A8.jpg