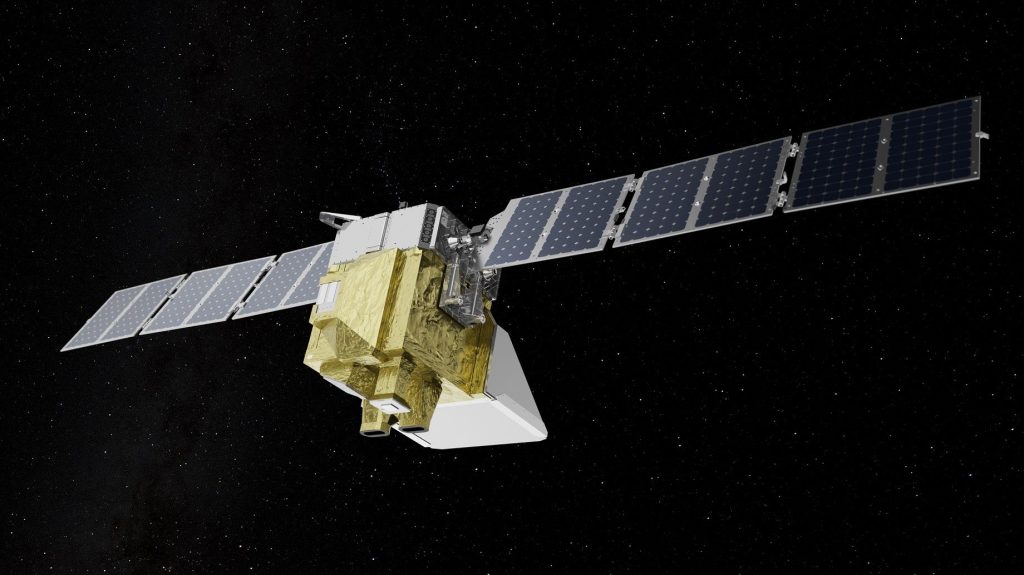डॉ. डी. बालसुब्रमण्यन, सुशील चंदानी

पृथ्वी के गर्माने को लेकर बढ़ती चिंताओं ने ‘हरित’ और ‘टिकाऊ’ जैसे शब्दों को प्रचलित कर दिया है। ‘हरित होने’ से मतलब है पर्यावरण-हितैषी तौर-तरीके (eco-friendly practices) अपनाकर पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास। टिकाऊ से तात्पर्य है ऐसे बदलाव लाना जो पर्यावरण और अर्थव्यवस्था (green economy) के बीच संतुलन बनाए रखे।
शब्द चाहे जो हो, पर्यावरणीय खतरों को कम या खत्म करने का साझा लक्ष्य हमें हरित रसायन विज्ञान (green chemistry) की ओर ले जाता है। और यह सोच हमें विषाक्तता और प्रदूषण (chemical pollution) से दूर ले जाता है। 1998 में पॉल एनेस्टस और जॉन वार्नर द्वारा प्रस्तुत हरित रसायन विज्ञान के 12 सिद्धांत बुनियादी बातों पर केंद्रित हैं; जैसे रासायनिक प्रक्रियाओं में सुरक्षित विलायकों और अभिकर्मकों को अपनाना; ऊर्जा-कुशल तरीके (energy-efficient chemical processes) विकसित करना जिनसे सुरक्षित रसायन प्राप्त हों जो यथासंभव गैर-विषाक्त हों और पर्यावरण में ज़्यादा देर तक मौजूद न रहे; और अपशिष्ट बनने (waste prevention) से रोकना (ताकि बाद में साफ-सफाई न करना पड़े)।
हरित रसायन विज्ञान कैसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है, इसका एक उदाहरण है बायोडीज़ल (biodiesel production) का उत्पादन। इंडियन ऑयल कार्पोरेशन हरित ईंधन मिशन (green fuel initiative) के तहत रतनजोत (जैट्रोफा) जैसे गैर-खाद्य बीजों से बायोडीज़ल का उत्पादन करता है। इन बीजों में 30 प्रतिशत से अधिक तेल होता है, और इसके पेड़ कम वर्षा वाले इलाकों और कम उपजाऊ मिट्टी में भी उग जाते हैं। बायोडीज़ल का उत्पादन ट्रांसएस्टरीफिकेशन अभिक्रिया (transesterification process) से होता है, जिसमें बीज के तेल की मेथनॉल के साथ अभिक्रिया करके बायोडीज़ल बनाता है। इससे उप-उत्पाद के रूप में ग्लिसरॉल भी प्राप्त होता है; यह भी व्यावसायिक रूप से उपयोगी है। कार्बन फुटप्रिंट कम (carbon footprint reduction) करने के लिए मेथनॉल बायोमास से प्राप्त किया जाना चाहिए।
उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं को तेज़ करते हैं। बायोडीज़ल उत्पादन को एक क्षार (alkaline catalyst) द्वारा सुगम बनाया जाता है। क्षार के तौर पर अक्सर सोडियम हाइड्रॉक्साइड का उपयोग (sodium hydroxide in biodiesel) किया जाता है, लेकिन उत्पादन उपरांत इसे बहा देने से पानी संदूषित हो जाता है, जिसे पर्यावरण में छोड़ने से पहले उपचारित करना पड़ता है। कैल्शियम ऑक्साइड इसका एक हरित विकल्प (green alternative to NaOH) है, क्योंकि यह एक ठोस पदार्थ है और प्रत्येक उत्पादन चक्र के बाद इसका 95 प्रतिशत हिस्सा पुन: प्राप्त किया जा सकता है।
औषधीय उत्पादों (दवा वगैरह) (pharmaceutical manufacturing) के निर्माण में भी अत्यधिक विषैले पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ऐसे कुछ कारखानों के आसपास की हवा में एक तीखी गंध आती है जो नाखून पॉलिश जैसी होती है। यह गंध विलायक टॉलुइन की होती है, जिसका व्यापक रूप से उपयोग पैरासिटामोल और कई अन्य दवाओं के संश्लेषण (drug synthesis solvents) या निष्कर्षण में किया जाता है। यह एक तंत्रिका विष (neurotoxic chemical) है। हरित प्रयासों (green alternatives in pharma) के तहत धीरे-धीरे ऐसे वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों के स्थान पर ऐसे विकल्पों का उपयोग होने लगा है जो कम विषाक्त हैं, जैव-विघटनशील (biodegradable solvents) हैं, और गन्ने जैसे बायोमास स्रोतों से प्राप्त किए जा सकते हैं।
हरित रसायन विज्ञान का एक और सिद्धांत जिस पर रसायनज्ञ काम करना पसंद करते हैं, वह है परमाणु किफायत (atom economy principle)। इसका उद्देश्य होता है कि अभिकारकों में मौजूद अधिक से अधिक परमाणुओं से वांछित उत्पाद हासिल कर लिए जाएं। ऊपर वर्णित बायोडीज़ल उत्पादन प्रक्रिया में हरित रसायन विज्ञान की बदौलत 100 प्रतिशत तो नहीं लेकिन 90 प्रतिशत परमाणु किफायत प्राप्त हो पाती है क्योंकि कुछ परमाणु उप-उत्पाद ग्लिसरॉल के निर्माण में खप जाते हैं। लेकिन ग्लिसरॉल का उपयोग अन्य उपयोगी उत्पाद (glycerol as byproduct) बनाने में हो जाता है।
परमाणु किफायत पर ध्यान देना उन उद्योगों में और भी अधिक महत्वपूर्ण है जहां उप-उत्पाद बहुत विषाक्त होते हैं। हरित रसायन विज्ञान की उत्कृष्टता (green chemistry success stories) का एक बेहतरीन उदाहरण बिरला विज्ञान संस्थान, पिलानी के हैदराबाद कैम्पस के रसायनज्ञों ने प्रस्तुत किया है। तन्मय चटर्जी और उनके साथियों की हरित विधि ने कैंसर-रोधी दवा टैमॉक्सीफेन (tamoxifen synthesis) और अन्य औषधियों के उत्पादन में 100 प्रतिशत परमाणु किफायत हासिल की है। यह विधि लागत-क्षम (cost-effective green method) भी है और इससे बड़े पैमाने पर उत्पादन भी संभव है। ऐसी विधियां हमारे पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाने की उम्मीद जगाती हैं। (स्रोत फीचर्स)
नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
Photo Credit : https://th-i.thgim.com/public/todays-paper/tp-national/tp-karnataka/u4rotb/article69707021.ece/alternates/LANDSCAPE_1200/mysuruMysuru-baGR2EH1L72.3.jpg.jpg