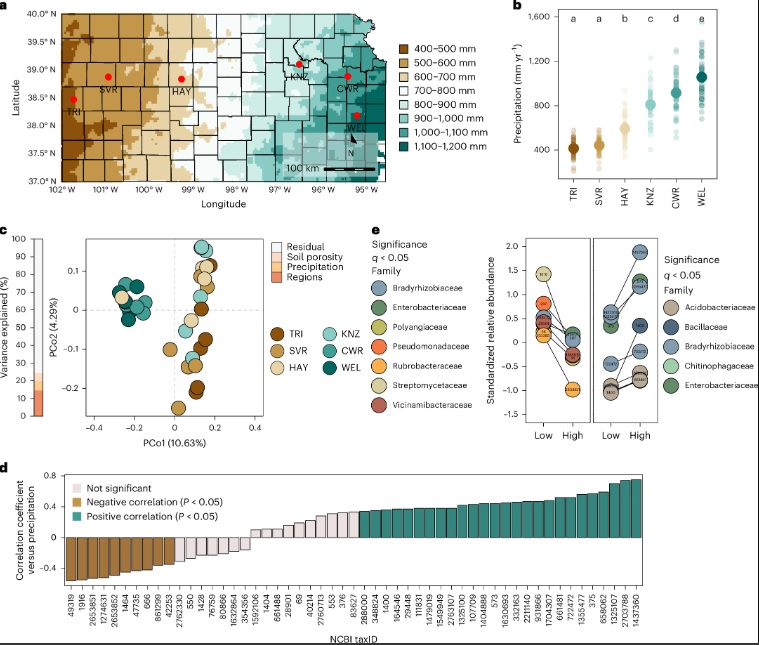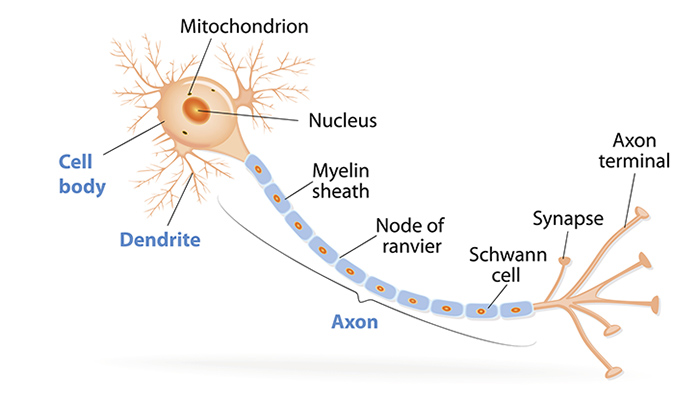जीवजगत में तमाम किस्म के सम्बंध पाए जाते हैं। सारे जंतु परपोषी (heterotrophic organisms) होते हैं यानी वे अपने भोजन के लिए किसी अन्य पर निर्भर रहते हैं। अधिकांश जंतु तो वनस्पतियों को खाते हैं (शाकाहारी) लेकिन कई जीव दूसरों का भक्षण करते हैं (मांसाहारी- carnivores), कुछ जंतु दूसरे जंतुओं से भोजन चुराते हैं लेकिन उन्हें मारते नहीं (परजीवी), जबकि कई जीव किसी अन्य जीव के साथ परस्पर फायदे का सम्बंध बना लेते हैं (symbiosis)।
लंबे समय से कीट सूक्ष्मजीवों (microorganisms) पर निर्भर रहे हैं। जैसे एम्ब्रोसिया गुबरैले (ambrosia beetles) पेड़ों में बिल बनाते समय साथ में फफूंद भी जमा कर लेते हैं, जो उन्हें भोजन मुहैया कराती हैं। कुछ गुबरैले अपने अंडों और इल्लियों को मकड़ियों से बचाने के लिए उन पर घातक बैक्टीरिया (bacteria) का लेप कर देते हैं। और अब इसी क्रम में एक और उदाहरण खोजा गया है।
स्टिंकबग (बदबूदार कीड़ा – stink bug) अपने अंडों पर फफूंद (protective fungus) का एक आवरण चढ़ा देता है जो उस अंडे में पनपते भ्रूण को परजीवी ततैया (parasitic wasp) से सुरक्षा प्रदान करता है।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड इंडस्ट्रियल साइन्स एंड टेक्नॉलॉजी (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology) के टेकेमा फुकात्सु (Takema Fukatsu) कई वर्षों से कीटों में सहजीविता का अध्ययन कर रहे हैं। उन्हें खास तौर से स्टिंकबग की प्रजाति मेजिमेनम ग्रेसिलिकोर्न (Megymenum gracilicorne) ने आकर्षित किया था। वैसे फुकात्सु के अध्ययन का मकसद इस कीट और फफूंद के सम्बंधों को समझना नहीं था। वे तो संयोगवश यहां तक पहुंच गए।
इसी से सम्बंधित अन्य कीटों के समान मेजिमेनम ग्रेसिलिकोर्न की पिछली टांगों का एक हिस्सा काफी फूला हुआ होता है। ऐसा माना जाता था कि यह रचना कान के पर्दे (टिम्पेनल झिल्ली – tympanal membrane) के समान है और कई तरह के कीटों में पाई जाती है। लेकिन फुकात्सु को इस बात पर हैरानी हुई कि यह रचना सिर्फ मादा कीट (female insect) में पाई जाती है। आम तौर पर ऐसी श्रवण संरचनाएं (hearing structures) दोनों लिंगों में पाई जाती हैं।
तब फुकुत्सा का संपर्क एक सेवानिवृत्त स्टिंकबग विशेषज्ञ (stink bug expert) शुजी ताचीकावा (Shuji Tachikawa) से हुआ। ताचीकावा ने अपने अध्ययनों में देखा था मेजिमेनम ग्रेसिलिकोर्न की मादा की टांगों पर एक सफेद पदार्थ पाया जाता है और यह पदार्थ उनके अंडों पर भी पुता होता है।
जब फुकात्सु और उनके साथियों ने एक नदी के किनारे खीरे की बेल से मेजिमेनम ग्रेसिलिकोर्न के नमूने एकत्रित किए तो उन्होंने भी देखा कि लैंगिक रूप से परिपक्व मादाओं पर ऐसे रेशे चिपके हुए थे। यह पट्टी चावल के दाने से भी छोटी थी और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी (electron microscope) से देखने पर पता चला कि इसकी सतह कान के पर्दे के समान चिकनी नहीं बल्कि खुरदरी है और उस पर महीन छिद्र थे जिनमें से फफूंद पनप रही थी। सावधानीपूर्वक विच्छेदन करने पर दिखा कि हरेक छिद्र में एक ग्रंथि है जिसमें से तरल रिस रहा है।
इसी दौरान कीट के एक विचित्र व्यवहार (insect behavior) ने शोधकर्ताओं का ध्यान खींचा। अंडे देते समय मादा हरेक टांग पर उग रही फफूंद को कुरेद रही थी। इसके बाद मादा ने प्रत्येक नवीन अंडे को रगड़ा। यह देखा गया कि इसके बाद हरेक अंडे पर फफूंद फैल गई। तीन दिनों के अंदर फफूंद ने अंडों पर 2-2 मिलीमीटर मोटी परत बना डाली। ज़ाहिर था कि फफूंद की परत अंडे से कहीं अधिक वज़नी थी।
प्रयोगशाला (laboratory experiment) में देखा गया कि मादा स्टिंकबग अपने नखरों से अपनी पिछली टांगों पर बनी फफूंद की पट्टी को छूती है और फिर उसे अंडों पर पोत देती है।
देखा जाए तो अंडों पर फफूंद का उगना अच्छी बात नहीं है। लेकिन डीएनए अनुक्रमण (DNA sequencing) से पता चला कि वहां उपस्थित सारी फफूंदें कीट के लिए लाभदायक (beneficial microbes) हैं। तो सवाल उठा कि क्या यह फफूंद आवरण उस ततैया (Trissolcus brevinotaulus) को अंडों से दूर रखने काम करेगी जो स्टिंकबग के अंडों के अंदर अपने अंडे देती है। यह जानने के लिए शोधकर्ताओं ने प्रयोगशाला में तैयार की गई पांच ततैया मादाओं (wasp females) को एक चेम्बर में रख दिया। इस चेम्बर में स्टिंकबग के करीब 20 अंडे रखे गए थे। इनमें से आधे अंडों पर फफूंद का आवरण था जबकि शेष आधे अंडों पर से फफूंद को पोंछकर हटा दिया गया था।
यानी फफूंद का आवरण स्टिंकबग के अंडों को सुरक्षा (egg protection) प्रदान करता है। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात सामने आई है। शोधकर्ताओं को फफूंद आवरण में किसी रासायनिक सुरक्षा (जैसे कोई बैक्टीरिया वगैरह) (chemical defense) के संकेत नहीं मिले। दूसरा, शोधकर्ताओं का विचार है कि संभवत: फफूंद को उस ग्रंथि के स्राव से कुछ पोषण (nutrient secretion) मिलता है।
आगे और प्रयोगों में पता चला कि जब फफूंद आवरण वाले अंडे फूटते हैं, तो उनमें से निकलने वाले शिशु स्टिंकबग थोडी फफूंद साथ लेकर जाते हैं (fungal transfer) लेकिन निर्मोचन के बाद वे उसे झड़ा देते हैं। यानी वयस्क होने पर अगली पीढ़ी को यह फफूंद फिर से हासिल करनी होगी। तो एक सवाल जिस पर फुकुत्सा काम करने जा रहे हैं, वह यही है कि हर मादा स्टिंकबग दोस्ताना फफूंद (symbiotic fungi) का चयन कैसे करती है। (स्रोत फीचर्स)
नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
Photo Credit : https://www.science.org/do/10.1126/science.zlhmcem/full/_20251016_on_stinkbugs.jpg