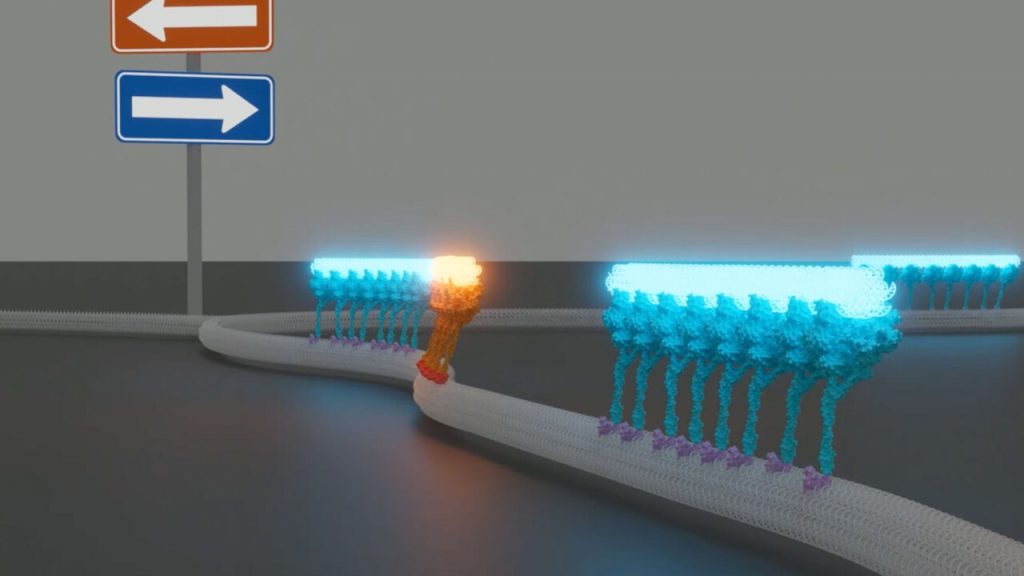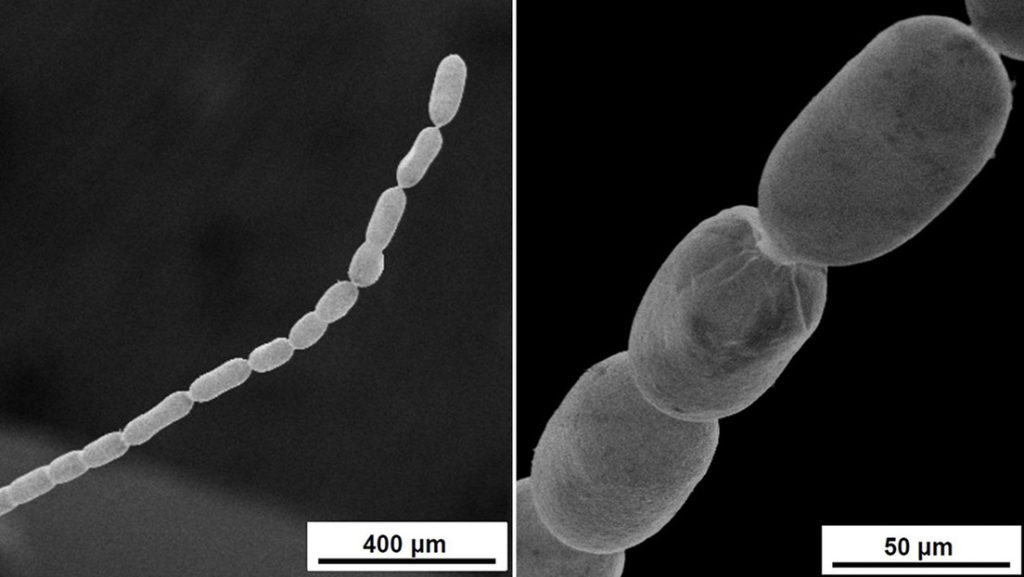भारत में करीब 12 करोड़ लोग धूम्रपान करते हैं। जन स्वास्थ्य के लिहाज़ से इसे कम किया जाना चाहिए।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) तथा यूएस के खाद्य व औषधि प्रशासन के अनुमान के मुताबिक दुनिया की 7.9 अरब की आबादी में से 1.3 अरब लोग धूम्रपान करते हैं और इनमें से 80 प्रतिशत निम्न व मध्यम आमदनी वाले देशों के निवासी हैं। अर्थात धूम्रपान एक महामारी है जो जन स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है। साल भर में यह 80 लाख लोगों से ज़्यादा की जान लेता है। इनमें से 70 लाख लोग तो खुद तंबाकू के इस्तेमाल से मरते हैं जबकि 12 लाख अन्य लोग सेकंड-हैंड धुएं के संपर्क के कारण जान गंवाते हैं। अमेरिकन जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन के मुताबिक लंबे समय से धूम्रपान करने वालों में टाइप-2 डायबिटीज़ की संभावना गैर-धूम्रपानियों की तुलना में 30 से 40 प्रतिशत तक ज़्यादा होती है। डॉ. स्मीलिएनिक स्टेशा के एक हालिया लेख में बताया गया है कि
1. धूम्रपान प्रति वर्ष 70 लाख से अधिक अधिक लोगों की मृत्यु का कारण बनता है;
2. 56 लाख युवा अमरीकी धूम्रपान के कारण जान गंवा सकते हैं;
3. सेकंड-हैंड धुआं दुनिया में 12 लाख लोगों की जान लेता है;
4. धूम्रपान दुनिया में निर्धनीकरण का प्रमुख कारण है; और
5. 2015 में 10 में से 7 धूम्रपानियों (68 प्रतिशत) ने कहा था कि वे छोड़ना चाहते हैं।
नेचर मेडिसिन के हालिया अंक में बताया गया है कि 2003 में डब्लूएचओ द्वारा तंबाकू नियंत्रण संधि पारित किए जाने के बाद इसे 2030 के टिकाऊ विकास अजेंडा में वैश्विक विकास लक्ष्य माना गया है। यदि संधि पर हस्ताक्षर करने वाले समस्त 155 देश धूम्रपान पर प्रतिबंध, स्वास्थ्य सम्बंधी चेतावनी, विज्ञापनों पर प्रतिबंध के साथ-साथ सिगरेटों की कीमतें बढ़ाने जैसे उपाय लागू करें तो यह लक्ष्य वाकई संभव है।
भारत की स्थिति
भारत निम्न-आमदनी वाले देश की श्रेणी से उबरकर विकसित देश बन चुका है, और अनुमानत: यहां 12 करोड़ धूम्रपानी हैं (कुल 138 करोड़ में से 9 प्रतिशत)। एक समय पर भारत व पड़ोसी देशों में गांजा-भांग काफी प्रचलित थे। इनका सेवन करने के बाद व्यक्ति को नशा चढ़ता है। इसे कैनेबिस के नाम से भी जानते हैं। कैनेबिस में सक्रिय पदार्थ टेट्राहायड्रोकेनेबिऑल होता है जो मनोवैज्ञानिक असर व नशे का कारण है। आज भी होली वगैरह पर लोग भांग चढ़ाते हैं।
तंबाकू
तंबाकू की बात करें, तो इसकी उत्पत्ति, औषधि के रूप में उपयोग, त्योहारों तथा नशे के लिए इसके उपयोग का विस्तृत विवरण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान (राजामुंदरी, आंध्र प्रदेश) द्वारा दिया गया है। ऐसा लगता है कि तंबाकू का पौधा दक्षिण अमेरिका में पेरुवियन/इक्वेडोरियन एंडीज़ में उगाया जाता था। इस नशीले पौधों का स्पैनिश नाम ‘टोबेको’ था।
तंबाकू का लुत्फ उठाने के लिए युरोपीय लोग जिस ‘पाइप’ का उपयोग करते थे वह शायद रेड इंडियन्स के फोर्क्ड केन से उभरा था। युरोप में तंबाकू लाने का श्रेय कोलंबस को जाता है। वहां से यह उनके उपनिवेशों (भारत व दक्षिण एशिया) में पहुंची। पुर्तगाली लोगों ने तंबाकू की खेती गुजरात के उत्तर-पश्चिमी ज़िलों में तथा ब्रिटिश हुक्मरानों ने उ.प्र., बिहार व बंगाल में शुरू करवाई थी।
इम्पीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1903 में हुई और उसने तंबाकू का वानस्पतिक व आनुवंशिक अध्ययन शुरू कर दिया। संक्षेप में कहें, तो तंबाकू का पौधा और उसके नशीले असर के बारे में भारतीयों को तब तक पता नहीं था, जब तक कि पश्चिमी लोग इसे यहां लेकर नहीं आए थे।
तंबाकू में सक्रिय अणु निकोटीन होता है। इसका नाम ज़्यां निकोट के नाम पर पड़ा है, जो पुर्तगाल में फ्रांसीसी राजदूत थे। उन्होंने 1560 में तंबाकू के बीज ब्राज़ील से पेरिस भेजे थे। तंबाकू के पौधे में से निकोटीन को अलग करने का काम 1858 में जर्मनी के डब्लू. एच. पोसेल्ट तथा के. एल. रीमान ने किया था। उनका मानना था कि यह एक विष है और यदि इसे स्लो-रिलीज़ ढंग से इस्तेमाल न किया जाए तो इसकी लत लग सकती है। (यही कारण है कि फिल्टर सिगरेटों का उपयोग स्लो-रिलीज़ के लिए किया जाता है)
लुइस मेल्सेन्स ने 1843 निकोटीन का अणु सूत्र ज्ञात किया और इसकी आणविक संरचना का खुलासा 1893 में एडोल्फ पिनर और रिटर्ड वोल्फेंस्टाइन ने किया था। इसका संश्लेषण सबसे पहले 1904 में ऑगस्ट पिक्टेट और क्रेपो द्वारा किया गया था। ताज़ा अनुसंधान से पता चला है कि नियमित धूम्रपानियों को टाइप-2 डायबिटीज़ का खतरा भी ज़्यादा रहता है।
प्रतिबंध
भारत में करीब 12 करोड़ लोग धूम्रपान करते हैं। जन स्वास्थ्य की दृष्टि से यह संख्या बहुत कम करना ज़रूरी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सिगरेट की बिक्री पर रोक लगाने की तैयारी कर रहा है। भारत डब्लूएचओ की तंबाकू नियंत्रण संधि पर 27 फरवरी 2005 को हस्ताक्षर कर चुका है।
इस संधि तथा टिकाऊ विकास लक्ष्यों के अनुरूप भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई सार्वजनिक स्थानों व कार्यस्थलों पर धूम्रपान की मनाही कर दी है – जैसे स्वास्थ्य सेवा से जुड़े स्थान, शैक्षणिक व शासकीय स्थान तथा सार्वजनिक परिवहन। ये सारे कदम स्वागत-योग्य हैं और लोगों को सहयोग करना चाहिए। (स्रोत फीचर्स)
नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
Photo Credit : https://img2.thejournal.ie/article/3597257/river?version=3597445&width=1340