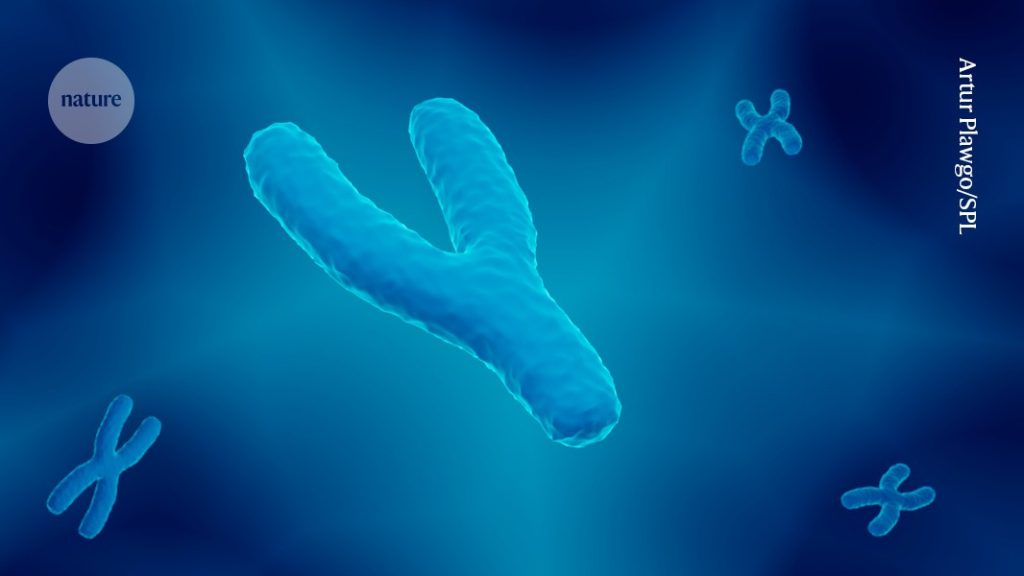डॉ. डी. बालसुब्रमण्यन

सोने के बाद चांदी सबसे कीमती धातु मानी जाती है। कई परिवारों में खुशी के मौकों पर सोने-चांदी की चेन-अंगूठियां ली-दी जाती हैं (या पहनी जाती हैं)। बेशक, चांदी सोने से सस्ती है।
लेकिन जब उद्योग (silver in industry) और ऊर्जा उत्पादन (silver in clean energy) में उपयोग की बात आती है तो चांदी सोने को पछाड़ देती है। पूरे भारत में चांदी का इस्तेमाल छतों पर लगे सौर पैनलों (solar panels) के माध्यम से सौर ऊर्जा को कैद करने में किया जाता है। इससे पूरे देश में सालाना लगभग 108 गीगावॉट स्वच्छ एवं हरित बिजली पैदा होती है। यह मात्रा कोयले से पैदा होने वाली बिजली की लगभग 10 प्रतिशत है। इसके अलावा, भारत की लगभग 1.4 अरब आबादी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मोबाइल फोन (silver in mobile phones) में विद्युत चालन और भंडारण के लिए चांदी का इस्तेमाल किया जाता है। हर मोबाइल फोन में लगभग 100-200 मिलीग्राम चांदी होती है। इसी तरह, एक सामान्य लैपटॉप में 350 मिलीग्राम चांदी उपयोग होती है, और वर्तमान में भारत में लगभग 5 करोड़ लैपटॉप हैं।
यदि भारत में मोबाइल फोन और लैपटॉप इतनी संख्या में हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में इनकी संख्या कितनी होगी। अनुमान है कि मोबाइल-लैपटॉप या ऐसी ही अन्य चीज़ों में पूरे विश्व में लगभग 7275 मीट्रिक टन चांदी लगती है। लेकिन (इन उपकरणों के खराब होने पर इनसे) बमुश्किल 15 प्रतिशत चांदी ही वापस निकालकर पुनर्चक्रित (silver recycling) की जाती है। जब कोई फोन या कंप्यूटर खराब हो जाता है या फेंक दिया जाता है तो उसमें मौजूद चांदी भी कूड़े में चली जाती है। काश! हम इन बेकार उपकरणों से यह चांदी वापिस निकाल पाते…
यह तो साफ है कि स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में चांदी (silver in renewable energy) एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस संदर्भ में मारिया स्मिरनोवा एक हालिया रिपोर्ट स्प्रॉट सिल्वर रिपोर्ट (Sprott Silver Report) में लिखती हैं कि जैसे-जैसे अधिकाधिक देश सौर पैनलों का उपयोग करके अक्षय ऊर्जा बनाएंगे, वैसे-वैसे चांदी की मांग (silver demand in solar industry) में लगातार वृद्धि होगी। वे आगे बताती हैं कि भले ही कुछ समूह सौर ऊर्जा के लिए अन्य धातुओं (जैसे लीथियम, कोबाल्ट और निकल) का उपयोग करने पर विचार कर रहे हैं, फिर भी स्वच्छ और हरित ऊर्जा उत्पादन में चांदी एक प्रमुख भूमिका निभाती है। और, इस साल चांदी की मांग में लगभग 170 प्रतिशत वृद्धि होने की उम्मीद है। इसके अलावा, कारों, बसों और ट्रेनों (electric vehicles) में ईंधन के रूप में पेट्रोल की जगह सौर ऊर्जा का उपयोग होना शुरू हुआ है। स्मिरनोवा आगे बताती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का अनुमान है कि 2035 तक, दुनिया भर में बिकने वाली हर दूसरी कार इलेक्ट्रिक होगी। इसका मतलब होगा कि हमें और चांदी चाहिए होगी।
इसी संदर्भ में, फिनलैंड के प्रोफेसर टिमो रेपो और उनके साथियों ने अपने शोधपत्र में चांदी को पुनःचक्रित करने की एक कुशल रासायनिक विधि (green silver recovery) प्रस्तुत की है। इस विधि में कार्बनिक वसीय अम्लों (जैसे लिनोलेनिक या ओलिक एसिड) (fatty acids for silver extraction) का उपयोग चांदी निकालने में किया गया है। ये कार्बनिक वसीय अम्ल तिलहन, मेवों और वनस्पति तेलों (जैसे जैतून का तेल या मूंगफली का तेल) में पाए जाते हैं, जिनका दैनिक भोजन में उपयोग होता है।
गौरतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक कचरे (e-waste silver recovery) से चांदी को पुन: प्राप्त करना आसान नहीं है: प्रबल अम्लों और साइनाइड के उपयोग की वजह से इस प्रक्रिया में विषाक्त पदार्थ पैदा हो सकते हैं। अन्य धातुओं और मिश्र धातुओं से चांदी को अलग करने की पारंपरिक विधियों का उपयोग करने की बजाय उपरोक्त समूह ने सूरजमुखी, मूंगफली और अन्य तेलों में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले साधारण असंतृप्त वसीय अम्लों के उपयोग से चांदी को अलग करके पुन: हासिल करने की एक विधि विकसित की है। समूह ने पाया कि इनका पुनर्चक्रण किया जा सकता है और इस प्रकार ये कार्बनिक विलायक और जलीय माध्यम से बेहतर हैं।
शोधकर्ताओं ने इस विधि को ‘शहरी खनन’ (urban mining of silver) में भी कारगर पाया है, जहां कबाड़ या कचरे में फेंके गए कंप्यूटर के मदरबोर्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक पुर्ज़ों के कचरे से चांदी पुन: निकाली जा सकती है। शोध दल का निष्कर्ष है, “वसीय अम्ल बहुमूल्य बहु-धातु अपशिष्ट के निपटान का उन्नत माध्यम बन सकते हैं।” (स्रोत फीचर्स)
नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
Photo Credit : https://assets.technologynetworks.com/production/dynamic/images/content/399617/fatty-acids-extract-silver-from-electronic-waste-399617-960×540.jpg?cb=13342110