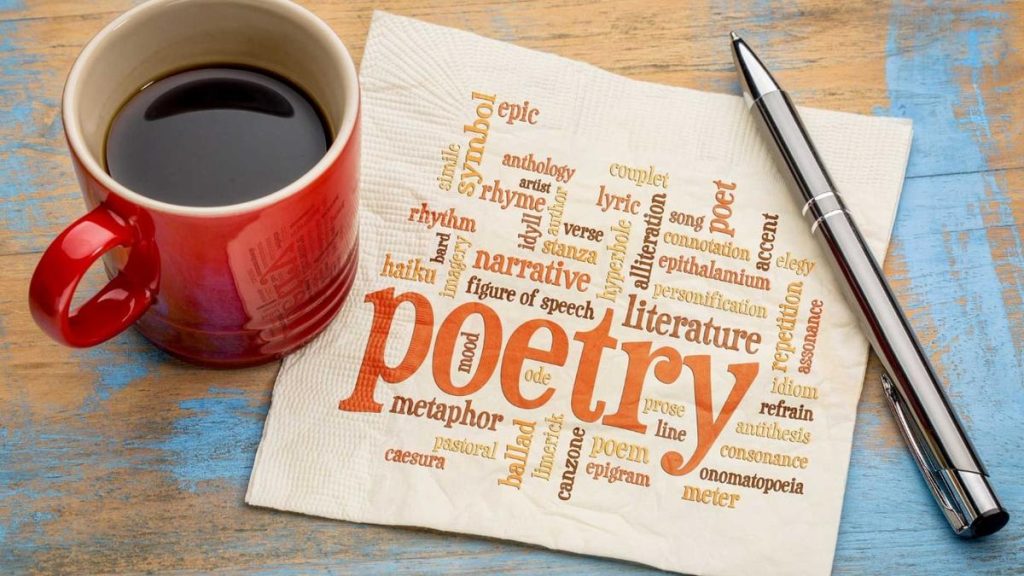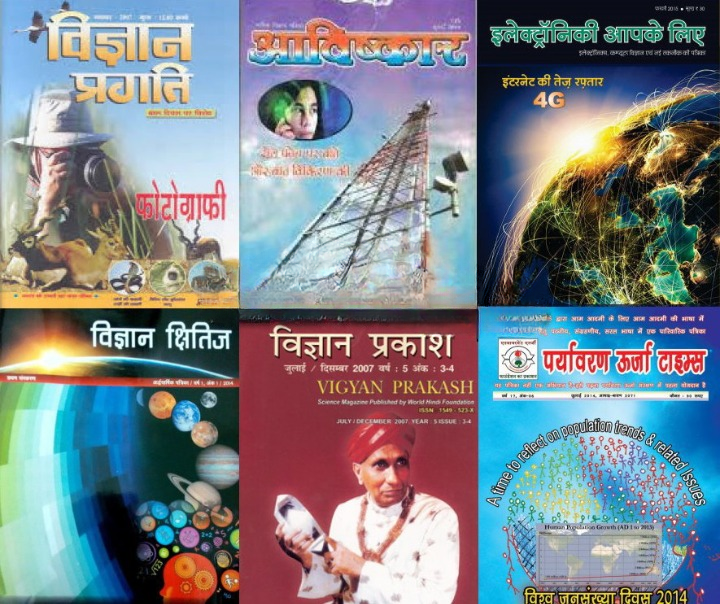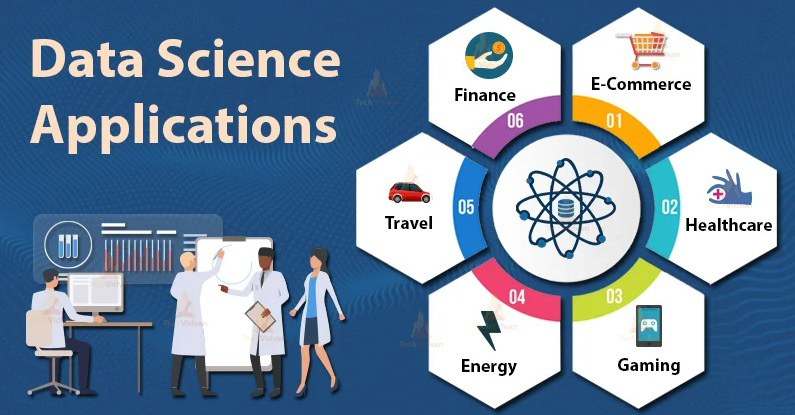अरविंद सरदाना
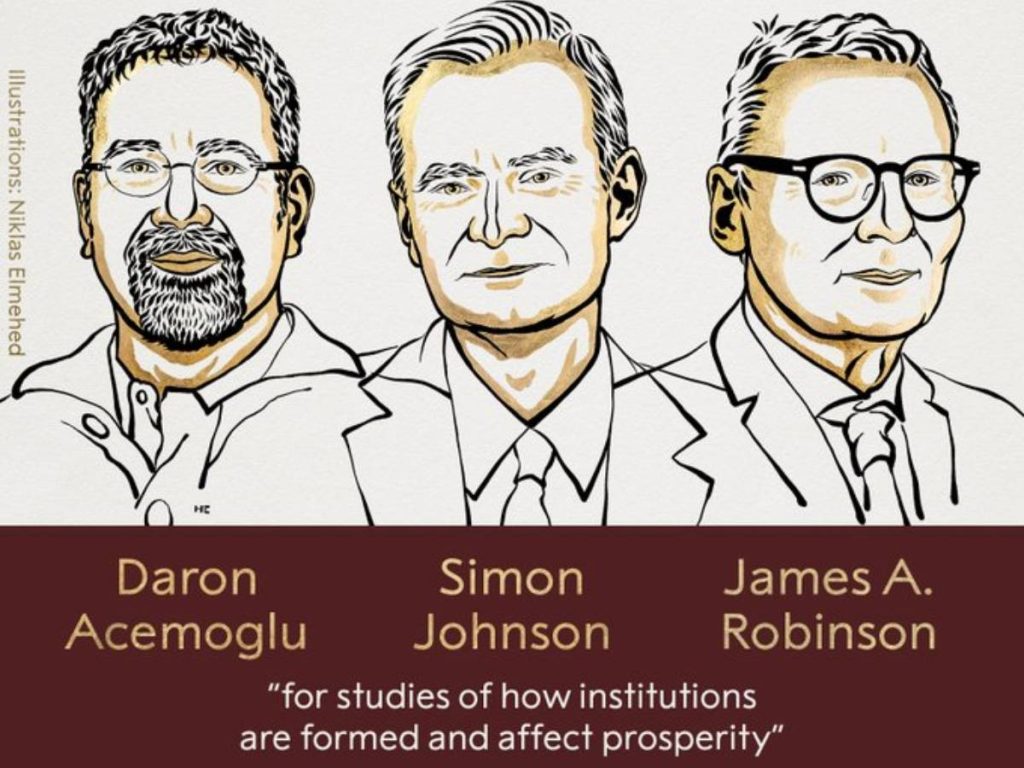
डैरन ऐसीमोगुलू (Daron Acemoglu), जेम्स रॉबिन्सन (James Robinson) एवं साइमन जॉनसन (Simon Johnson) को इस वर्ष के अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार (Nobel Prize in Economics) से नवाज़ा गया है। यह कई मायनों में महत्वपूर्ण है। उनका अध्ययन किसी भी देश में विकास (Economic Growth) के न होने पर केंद्रित है।
डैरन ऐसीमोगुलू और जेम्स रॉबिन्सन अपनी चर्चित किताब व्हाय नेशन्स फेल: दी ओरिजिन ऑफ पॉवर, प्रॉस्पेरिटी एंड पॉवर्टी (Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty) में पूछते हैं कि विभिन्न देशों में किस प्रकार की सामाजिक और आर्थिक संस्थाएं बनीं और उनमें क्या अंतर रहा, जिसने विकास की राह को प्रभावित किया?
यह राजनीतिक अर्थशास्त्र (Political Economy) का पुराना सवाल है। जैसे लगभग ढाई सौ वर्ष पूर्व एडम स्मिथ (Adam Smith) की मशहूर किताब दी वेल्थ ऑफ नेशन्स (The Wealth of Nations) थी। इस वर्ष का पुरस्कार इस बात की स्वीकार्यता का द्योतक है कि अर्थशास्त्रीय अध्ययन (Economic Analysis) में विभिन्न दृष्टिकोणों से विश्लेषण किया जाता है।
“विभाजन के लगभग आधी सदी बाद, 1990 के दशक के आखिर में, दक्षिण कोरिया (South Korea) का विकास और उत्तर कोरिया (North Korea) के ठहराव ने इस एक देश के दो हिस्सों के बीच दस गुना का अंतर पैदा कर दिया है। उत्तर कोरिया की आर्थिक आपदा (Economic Crisis), जिसके कारण लाखों लोग भुखमरी का शिकार हुए, की तुलना जब दक्षिण कोरिया की आर्थिक सफलता (Economic Success) के साथ की जाती है, तो यह चौंकाने वाली बात है: उत्तर और दक्षिण कोरिया के अलग-अलग विकास मार्ग की व्याख्या न तो संस्कृति (Culture), न भूगोल (Geography) और न ही अज्ञानता (Ignorance) कर सकती है। हमें जवाब के लिए संस्थाओं (Institutions) को देखना होगा (व्हाय नेशन्स फेल)।”
उनका मुख्य फोकस इस बात पर है कि किसी देश में सामाजिक और आर्थिक संस्थाओं का स्वररूप समावेशी यानी इंक्लूसिव (Inclusive Institutions) रहा है या फिर शोषणकारी। उनका विश्लेषण बताता है कि समावेशी संस्थाएं आम लोगों को मौके देती हैं, बाज़ार व्यवस्था (Market Economy) को बढ़ने का अवसर प्रधान करती हैं और नई टेक्नोलॉजी (New Technology) को अपनाने का वातावरण बनाए रखती हैं। किसी भी व्यवस्था में जब विकास का लाभ अधिक लोगों में बंटता है और उसकी नींव संस्थानों में है, तो यह समावेशी स्वरूप लेता है। इसके विपरीत जब विकास एक सीमित वर्ग की ओर केन्द्रित होता है तो वहां शोषणकारी संस्थाएं बनती हैं और उन्हें पोषित करती रहती हैं। इस प्रकार एक अभिजात्य वर्ग का मज़बूत वर्चस्व लगातार बना रहता है।
यह बात इतनी नई नहीं है, परंतु उनका शोध अलग-अलग देशों का तुलनात्मक विश्लेषण (Comparative Analysis) इस दृष्टिकोण को आंकड़ों के साथ अनूठे रूप से प्रस्तुत करता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। स्वतंत्रता के समय 1966 में बोत्सवाना (Botswana), दुनिया के सबसे गरीब देशों (Poorest Countries) में से एक था। यहां “कुल बारह किलोमीटर पक्की सड़कें थीं, बाईस व्यक्ति विश्वविद्यालय से स्नातक थे, और सौ माध्यमिक विद्यालय थे। यह दक्षिण अफ्रीका (South Africa), नामीबिया (Namibia) और रोडेशिया (Rhodesia) के श्वेत शासनों से घिरा हुआ था, जो सभी अश्वेतों द्वारा संचालित स्वतंत्र अफ्रीकी देशों (Independent African Nations) के प्रति नफरत पालते थे। फिर भी अगले चालीस वर्षों में, बोत्सवाना दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते देशों (Fastest Growing Economies) में शुमार हो गया। आज सब-सहारा अफ्रीका (Sub-Saharan Africa) में बोत्सवाना की प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) सबसे अधिक है, और यह एस्टोनिया (Estonia) और हंगरी (Hungary) जैसे सफल पूर्वी युरोपीय देशों के बराबर के स्तर पर है।
बोत्सवाना ने तेज़ी से समावेशी आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं (Inclusive Economic and Political Institutions) का विकास किया। वह लोकतांत्रिक (Democratic Governance) बना रहा है और वहां नियमित रूप से चुनाव होते रहे हैं। उसने कभी भी गृह युद्ध (Civil War) या सैन्य हस्तक्षेप (Military Intervention) का सामना नहीं किया है। सरकार ने संपत्ति के अधिकार (Property Rights) को लागू करने, व्यापक आर्थिक स्थिरता (Economic Stability) सुनिश्चित करने और समावेशी बाज़ार अर्थव्यवस्था (Inclusive Market Economy) के विकास को प्रोत्साहित किया। सब-सहारा अफ्रीका के अधिकांश देशों, जैसे सिएरा लियोन और जिम्बाब्वे, में स्वतंत्रता के बाद बदलाव का जो अवसर मिला था, उसे उन्होंने खो दिया। आज़ादी के बाद, औपनिवेशिक काल के दौरान मौजूद शोषणकारी संस्थाओं का फिर से निर्माण हुआ। इनकी तुलना में स्वतंत्रता के शुरुआती चरण में बोत्सवाना अलग था और कबीला मुखियाओं का लोगों के प्रति कुछ हद तक जवाबदेही वाली संस्थाओं का इतिहास बना रहा। “इस तरह की संस्थाओं के लिए बोत्सवाना निश्चित रूप से अफ्रीका में अद्वितीय नहीं था लेकिन इस हद तक तो अद्वितीय था कि ये संस्थाएं औपनिवेशिक काल में बिना ज़्यादा नुकसान के बची रहीं।”
उदाहरण के लिए, आज़ादी के बाद बोत्सवाना में बने मांस आयोग ने पशु अर्थव्यवस्था को विकसित करने में केंद्रीय भूमिका निभाई, फुट एण्ड माउथ रोग को नियंत्रित करने के लिए काम किया और निर्यात को बढ़ावा दिया। इससे आर्थिक विकास में योगदान मिला और समावेशी आर्थिक संस्थाओं के लिए समर्थन बढ़ा। बोत्सवाना में शुरुआती विकास मांस निर्यात पर निर्भर था, लेकिन हीरे की खोज के बाद चीज़ें नाटकीय रूप से बदल गईं। बोत्सवाना में प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन भी अन्य अफ्रीकी देशों से काफी अलग था। औपनिवेशिक काल के दौरान, बोत्सवाना प्रमुखों ने खनिजों की खोज को रोकने का प्रयास किया था क्योंकि वे जानते थे कि अगर युरोपीय लोगों ने कीमती धातुओं या पत्थरों की खोज की, तो उनकी स्वायत्तता खत्म हो जाएगी। आज़ादी के बाद सबसे बड़ी हीरे की खोज नग्वाटो भूमि के नीचे हुई थी, जो एक कबीले की पारंपरिक मातृभूमि थी। देश के नेताओं ने खोज की घोषणा से पहले, कानून में बदलाव किया ताकि खनिज सम्पदा का अधिकार राष्ट्र में निहित हो, न कि जनजाति में। इसने राज्य में केंद्रीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया। हीरे के राजस्व का इस्तेमाल अब नौकरशाही, बुनियादी ढांचे के निर्माण और शिक्षा में निवेश के लिए किया गया। यह अन्य अफ्रीकी देशों से अलग है।
इस प्रकार कई तुलनात्मक अध्ययनों (Comparative Studies) से यह स्पष्ट होता है कि विकास के लिए समावेशी संस्थाओं का बनना ज़रूरी है। इनके बनने के पीछे राजनीतिक समीकरण (Political Equations) और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Context) का विश्लेषण करना होगा। बदलाव के खास मौके कुछ देशों में कैसे बने? इस अध्ययन से कुछ सीख ली जा सकती है पर इतिहास भविष्य के लिए कोई नुस्खे नहीं प्रदान करता। पुस्तक में बताया गया है कि आजकल एक्सपर्ट यह भ्रम पालते हैं कि विकास को ढांचाबद्ध किया जा सकता है, बस जानकारी की कमी है। पर वास्तव में वे संस्थाओं की जटिलता को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं जो उनकी योजनाओं को विफल कर देती हैं। उसी प्रकार, यह भी बताया गया है कि विदेशी मदद की भूमिका नहीं है। इसी प्रकार से, आजकल कई मुल्कों में तानाशाही व्यवस्था विकास के लिए लुभावनी दिखती है और कुछ समय के लिए इसका असर होता भी है, परन्तु यह एक समय बाद बिखरने लगता है क्योंकि केंद्रीकृत सत्ता समय के साथ आने वाले आवश्यक बदलाव नहीं होने देती।
बहरहाल, चाहे हम सहमत हों या नहीं, इनकी पुस्तक पढ़ने योग्य है। (स्रोत फीचर्स)
नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
Photo Credit : https://d3pc1xvrcw35tl.cloudfront.net/ln/images/1200×900/nobel-prize-in-economics_202410822885.jpg