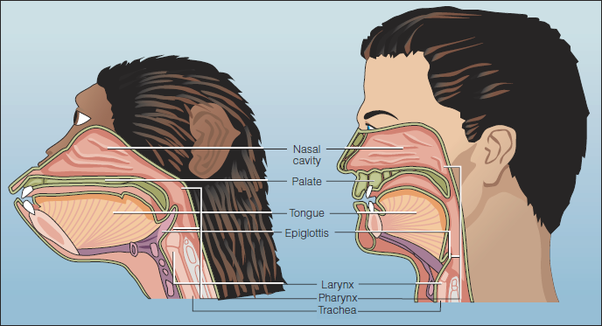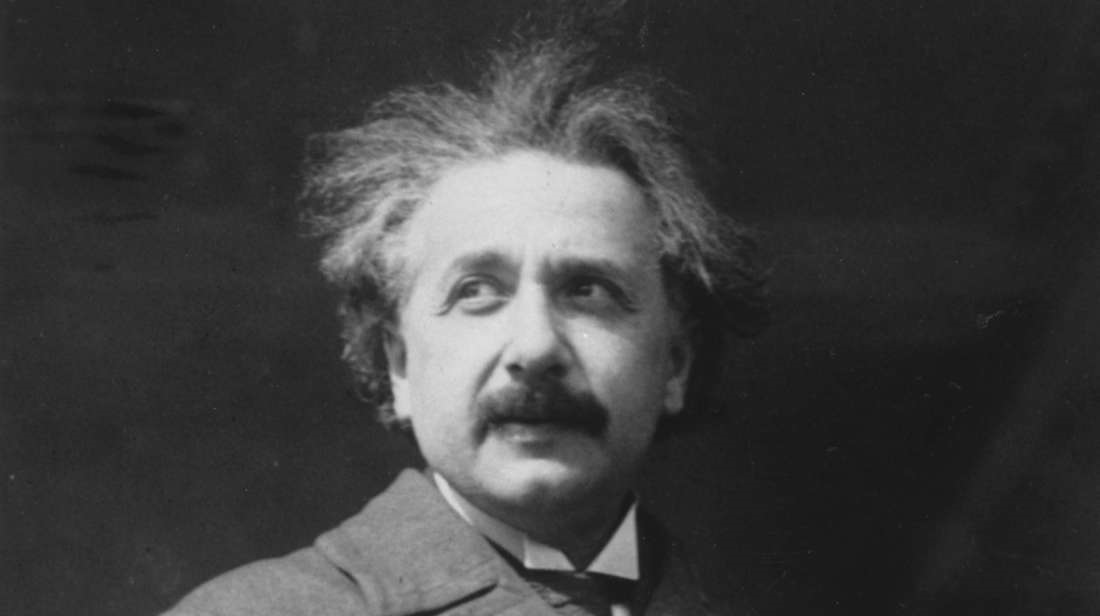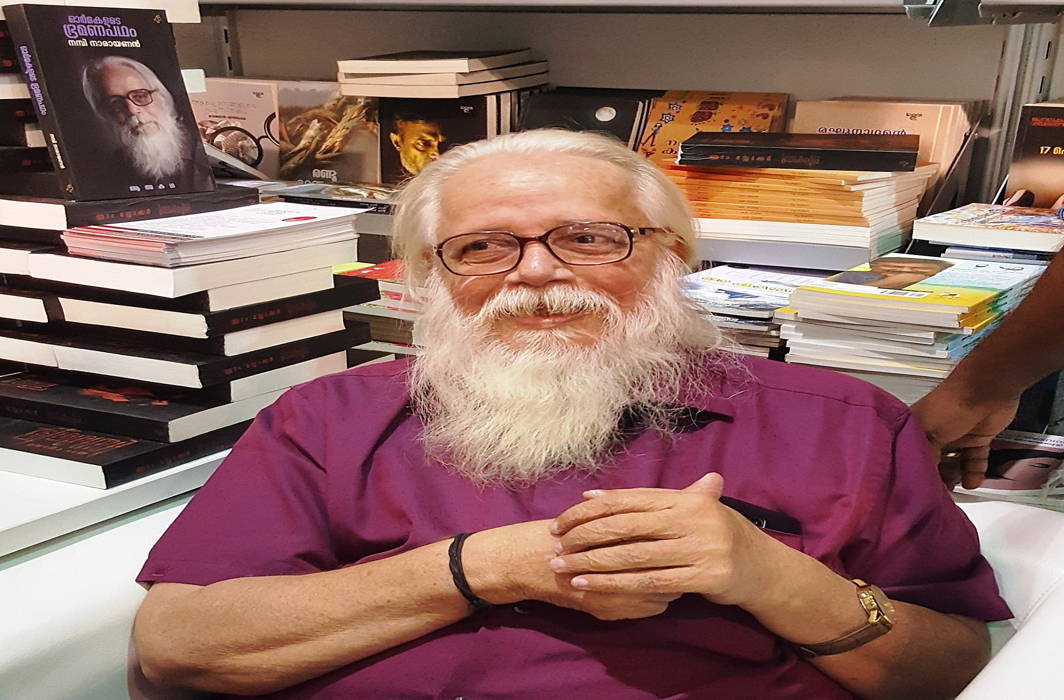नोबेल समिति ने इस साल के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए इराक की यजीदी मूल की नौजवान लड़की नादिया मुराद और कांगो के डॉ. डेनिस मुकवेगे को चुना है। इन दोनों बेमिसाल शख्सियतों को यौन हिंसा के खिलाफ प्रभावी मुहिम चलाने और महिला अधिकारों के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया जा रहा है। दोनों ने अपने-अपने कामों से दुनिया में अमन और लैंगिक समानता बढ़ाने की बेजोड़ कोशिश की और यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है।
नोबेल समिति की अध्यक्ष बेरिट रेइस एंडरसन ने पत्रकार वार्ता में इन नामों का ऐलान करते हुए कहा कि दोनों ही विजेताओं ने युद्ध क्षेत्र में यौन हिंसा को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की मानसिकता के खिलाफ सराहनीय काम किया है। दोनों इस वैश्विक अभिशाप के खिलाफ संघर्ष की एक मिसाल हैं। एक शांतिपूर्ण दुनिया केवल तभी हासिल की जा सकती है, जब महिलाओं और उनके मौलिक अधिकारों एवं सुरक्षा को युद्ध में पहचाना और संरक्षित किया जाए। मुकवेगे और मुराद दोनों एक वैश्विक संकट के खिलाफ संघर्ष की नुमाइंदगी करते आए हैं, जो कि किसी भी संघर्ष से परे है, जिसे बढ़ते हुए ‘मी टू’ आंदोलन ने भी दिखाया है। उन्होंने कहा कि यौन हिंसा के खिलाफ इनके महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए इन्हें नोबेल शांति सम्मान दिया जा रहा है।
पाकिस्तान की मलाला युसुफजई के बाद नादिया मुराद दूसरी ऐसी महिला हैं, जिन्हें इतनी कम उम्र में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। एक ऐसे वक्त में जब दुनिया में महिलाओं के साथ कई तरह की यौन हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हों, तमाम काशिशों के बाद भी उनका यौन उत्पीड़न रुका नहीं हो, पुरुष आज भी उन्हें अपनी यौन दासी के अलावा कुछ न समझते हों, नादिया मुराद और डॉ. डेनिस मुकवेगे का सम्मानित होना यह आश्वस्ति प्रदान करता है कि यौन हिंसा पीड़िताओं की सिसकियां अनसुनी नहीं है। कोई न सिर्फ उनकी आवाज़ सुन रहा है, बल्कि उसे सारी दुनिया के सामने भी ला रहा है। उनके ज़ख्मों पर अपने कामों से मरहम लगा रहा है। आईएस के आतंक से ग्रस्त इराक में नादिया मुराद और गृहयुद्ध में घिरे कांगो में डेनिस मुकवेगे ने यौन हिंसा की पीड़िताओं के मानवाधिकार की रक्षा के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी है। नोबेल शांति पुरस्कार इन दोनों के साहस को मान्यता प्रदान करना है।
नादिया मुराद बसी ताहा का जन्म इराक के कोजो शहर में साल 1993 में हुआ था। वे इराक की यजीदी मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। मुराद ‘नादिया अभियान’ की संस्थापक हैं। यह संस्था नरसंहार, सामूहिक अत्याचार और मानव तस्करी के पीड़ित महिलाओं और बच्चों की मदद करती है। संस्था उन्हें अपनी ज़िंदगी दोबारा जीने और उन बुरी यादों से उबरने में मदद करती है।
नादिया यौन पीड़िताओं की मददगार और दुनिया भर में उनकी आवाज़ क्यों बनी? इसकी कहानी भी बड़ी हैरतअंगेज़ है। नादिया उन 3,000 यजीदी लड़कियों और महिलाओं में से एक है, जिन्हें साल 2014 में इस्लामिक स्टेट (आईएस) के आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया था और उनके साथ लगातार बलात्कार और दुर्व्यवहार किया था। वे करीब तीन महीने तक आईएस के आतंकियों के कब्जे में रहीं, जहां उनके साथ दिन-रात बलात्कार किया गया। वह कई बार खरीदी और बेची गई। किसी तरह से वहां से वह अपनी जान बचाकर निकली। उनके चंगुल से छूटने के बाद, उन्होंने यौन हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए काम करना शुरू कर दिया। इस वक्त वे पूरी दुनिया में महिलाओं को यौन हिंसा के खिलाफ जागरूक करने का काम कर रही हैं। नादिया मानव तस्करी के पीड़ितों के लिए संयुक्त राष्ट्र की गुडविल एंबेसडर भी हैं। नादिया मुराद ने अपने अनुभवों पर एक किताब भी लिखी है, जिसका नाम ‘दी लॉस्ट गर्ल : माई स्टोरी ऑफ कैप्टिविटी एंड माई फाइट अगेंस्ट द इस्लामिक स्टेट’ है। इस किताब में आईएस आतंकियों की हैवानियत के किस्से भरे पड़े हैं।
नादिया मुराद की तरह डॉ. डेनिस मुकवेगे भी यौन हिंसा के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। वे पेशे से स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और यौन हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए लंबे समय से काम कर रहे हैं। ‘दी ग्लोब एंड मॉल’ के मुताबिक डॉ. मुकवेगे, बलात्कार की चोटों को ठीक करने के मामले में दुनिया के अग्रणी विशेषज्ञ हैं। डॉ. मुकवेगे को उनके द्वारा युद्धग्रस्त पूर्वी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में महिलाओं को हिंसा, बलात्कार और यौन हिंसा के सदमे से बाहर निकालने में दो दशकों तक किए गए काम के लिए मान्यता मिली है। मुकवेगे कांगो में डॉक्टर चमत्कार के रूप में जाने जाते हैं। कांगो ही नहीं, अन्य अफ्रीकी देशों की महिलाएं भी उन्हें एक रहनुमा की तरह देखती हैं। मुकवेगे ने अपने द्वारा 1999 में स्थापित पांजी अस्पताल में बलात्कार के हज़ारों पीड़ितों का इलाज किया है। साल 2015 में उनके जीवन पर आधारित फिल्म ‘दी मैन हू मेंड्स विमन’ आई थी। मुकवेगे ने फ्रांसीसी में अपनी आत्मकथा ‘प्ली फॉर लाइफ’ भी लिखी है जिसमें उन्होंने ऐसे तमाम हादसों का ज़िक्र किया है, जिन्होंने उन्हें कांगो में पांजी अस्पताल खोलने को मजबूर किया। अस्पताल में वे संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की हिफाज़त का काम करते हैं। डॉ. मुकवेगे युद्ध के दौरान महिलाओं के दुरुपयोग के एक मुखर आलोचक हैं। उन्होंने अपने भाषणों में कई बार बलात्कार को सामूहिक विनाश का हथियार बताया है। मुकवेगे ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार दुष्कर्म और यौन हिंसा से प्रभावित सभी महिलाओं को समर्पित किया है।
शांति का नोबेल पुरस्कार किसी ऐसे शख्स या संस्था को दिया जाता है, जो दो देशों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देते हैं या फिर समाज के लिए अच्छा काम करते हैं, जिससे लोगों को नई जिंदगी-नई राह मिलती है। नादिया मुराद और डॉ. डेनिस मुकवेगे के नाम सुनकर पहली बार ज़रूर सबको हैरानी हुई, लेकिन बाद में जब इनके काम सामने आए, तो सभी ने इनकी जी भरकर तारीफ की। पूरी दुनिया में घरों से लेकर कार्यस्थलों तक और जंग के मैदान एवं गृहयुद्ध की मार झेल रहे देशों में यौन उत्पीड़न को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे न सिर्फ महिलाएं प्रभावित हैं, बल्कि मासूम बच्चियों को भी यौन हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि कई युद्धग्रस्त देशों में काम कर रहे संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर भी महिलाओं के यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे हैं।
एक तरफ हम महिलाओं के लिए लैंगिक समानता और बराबरी की बात करते हैं, तो दूसरी ओर लगातर उनका यौन उत्पीड़न और उनके साथ यौन हिंसा हो रही है। तमाम बड़े-बड़े दावों और कानूनों के बाद भी उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न, यौन हिंसा में कोई कमी नहीं आई है। विकसित देश हों या विकासशील देश, दुनिया के सभी देशों में महिलाओं की स्थिति कमोबेश एक जैसी है। उन्हें अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी यौन उत्पीड़न या यौन हिंसा का सामना करना पड़ता है। यह वाकई चिंता का विषय है कि दुनिया की आधी आबादी के प्रति हमारा नज़रिया आज भी नहीं बदला है। हम आज भी उन्हें यौन गुड़िया से ज़्यादा नहीं समझते। यह सोचे बिना उनके साथ शारीरिक या मानसिक यौन हिंसा करते हैं कि इससे उनकी भावी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा। कहीं इससे उनकी कार्यक्षमता पर तो गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा? महिलाओं को यौन उत्पीडन से मुक्ति दिलाकर ही एक समृद्ध एवं सुन्दर दुनिया बनाई जा सकती है। दोनों पुरस्कार विजेता इसी दिशा में काम कर रहे हैं और हमें उनका खुलकर और सक्रिय समर्थन करना चाहिए।(स्रोत फीचर्स)
नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
Photo Credit : https://gdb.voanews.com/835BBC8A-C0BE-4258-9A4C-0F02F2A40CBA_w1023_r1_s.jpg