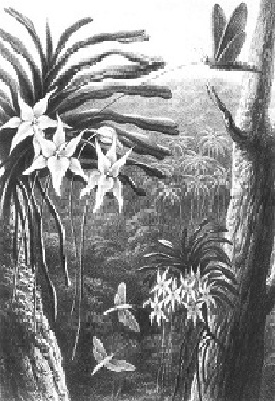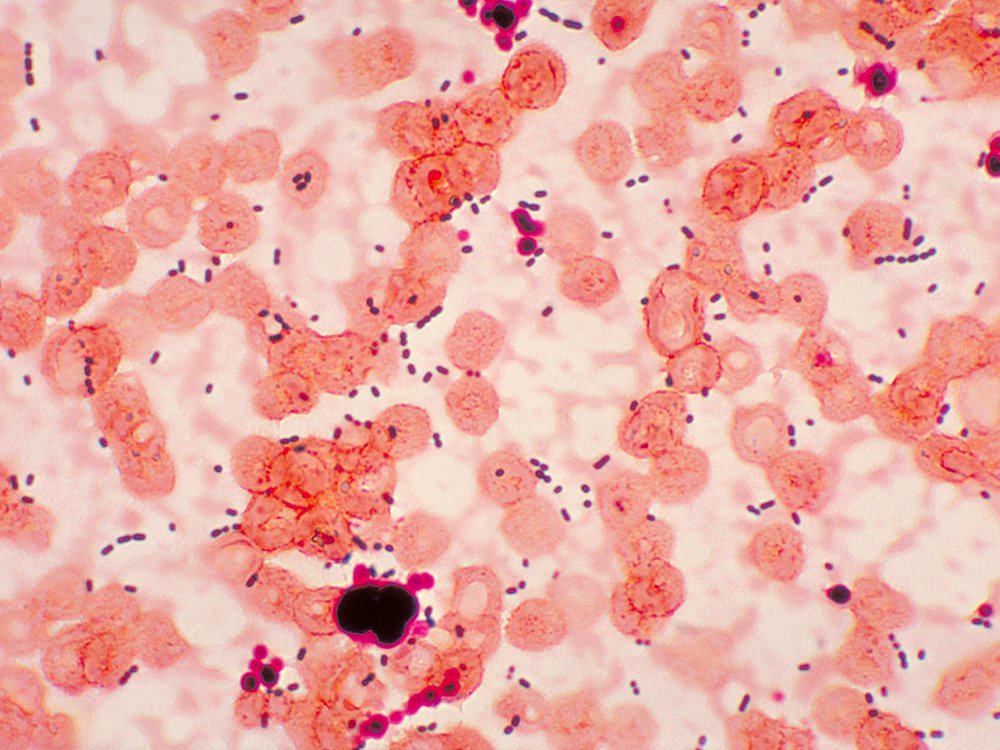पश्चिम अफ्रीका के चिम्पैंज़ी ताड़ के फल से गिरी निकालने के लिए एक युक्ति इस्तेमाल करते हैं – फल को एक सपाट पत्थर पर रखकर दूसरे पत्थर का हथौड़े की तरह इस्तेमाल करते हुए फल पर मारते हैं, ताकि उसकी बाहरी सख्त खोल चटक जाए।
अब तक वैज्ञानिकों को चिम्पैंज़ी के इस औज़ार के बारे में अधिक जानने के लिए चिम्पैंजियों की घंटों लंबी रिकॉर्डिंग को निहारना पड़ता जिसमें हफ्तों लग जाते थे। अब इस काम में कृत्रिम बुद्धि मदद कर सकती है, जो चिम्पैंजि़यों के वीडियो फुटेज में से सही क्लिप को ढूंढ सकती है।
युनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की प्राइमेटोलॉजिस्ट सुज़ाना कार्वाल्हो और उनके साथियों ने चिम्पैंज़ी के दो व्यवहारों का अध्ययन किया: फल से गिरी निकालना और नगाड़ेबाज़ी (चिम्पैंज़ी द्वारा हाथों या पैरों से पेड़ की सहारा जड़ों को पीटना।) वैज्ञानिकों के अनुसार ये दोनों व्यवहार प्राइमेट्स में सीखने की प्रक्रिया और संवाद को समझने की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा इन हरकतों के दौरान आवाज़ भी उत्पन्न होती है, यानी शोधकर्ता दृश्य के साथ-साथ ध्वनि से भी कंप्यूटर मॉडल को प्रशिक्षित कर सकते हैं।
उक्त मॉडल को गिरी निकालने का व्यवहार समझाने के लिए शोधकर्ताओं ने लगभग 40 घंटे की और ड्रमिंग के लिए लगभग 10 घंटे लंबी वीडियो रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल किया। ड्रमिंग की क्लिप खास तौर से उग्र व्यवहार की थी जिसे “बट्रेस ड्रमिंग” कहा जाता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि अलग-अलग चिम्पैंज़ी-समूहों में ड्रमिंग का तरीका अलग-अलग हो सकता है।
पहले तो शोधकर्ताओं ने ऑडियो और वीडियो की कोडिंग के ज़रिए कंप्यूटर को प्रशिक्षित किया। वीडियो में जहां-जहां चिम्पैंज़ी थे उनके आसपास चौकोर दायरा खींचा और उनमें वे क्या गतिविधि कर रहे हैं उसे लिखा। इस तरह उन्होंने कंप्यूटर को सिखाया कि क्या देखना है और क्या अनदेखा करना है। कभी-कभी चिम्पैंज़ी नज़र नहीं आते थे। इसलिए शोधकर्ताओं ने ध्वनि से पहचानने के लिए भी प्रशिक्षित किया।
जब कंप्यूटर का प्रशिक्षण पूरा हो गया तो शोधकर्ताओं ने उसका परीक्षण किया। उन्होंने उसे दोनों व्यवहारों के ऐसे वीडियो दिखाए जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। साइंस एडवांसेस में प्रकाशित शोध पत्र के अनुसार कंप्यूटर ने गिरी निकालने के व्यवहार 77 प्रतिशत और नगाड़ेबाज़ी का व्यवहार 86 प्रतिशत बार सही-सही पहचाना।
शोधकर्ताओं ने इस कंप्यूटर के ज़रिए पता किया कि चिम्पैंज़ी गिरी निकालने और नगाड़ेबाज़ी जैसे व्यवहार में कितना वक्त बिताते हैं, और नर और मादा में कोई अंतर है क्या। उम्मीद है कि नए मॉडल को अन्य प्रजातियों और अन्य व्यवहारों की निगरानी के लिए भी प्रशिक्षित किया जा सकेगा। यह भी देखा जा सकता है कि कोई एक चिम्पैंज़ी कौशल कैसे विकसित करता है। फुटेज का विश्लेषण यह समझने में मदद कर सकता है कि जलवायु परिवर्तन और आवास की क्षति प्राइमेट्स के व्यवहार को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। संभावनाएं तो अपार हैं। (स्रोत फीचर्स)
नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
Photo Credit : https://im.indiatimes.in/media/content/2017/Oct/chim_1506840084_725x725.jpg