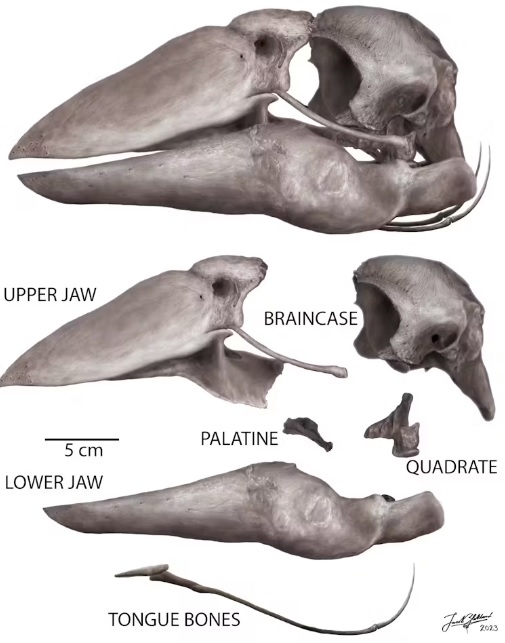आम तौर पर जेनेटिक सूचना एक ही दिशा में बहती है – डीएनए नामक अणु में जीन्स होते हैं, ये जीन्स एक सांचे की तरह काम करते हैं और एक अन्य अणु आरएनए का निर्माण करते हैं और आरएनए प्रोटीन बनवाता है। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और यह जिन एंज़ाइमों के दम पर चलती है उन्हें ट्रांसक्रिप्टेस कहते हैं। यह सीधी-सरल कथा 1970 में पेचीदा हो गई। उस साल वैज्ञानिकों ने खोजा कि कुछ वायरसों में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस नामक एंज़ाइम होता है। और यह एंज़ाइम उपरोक्त एकदिशीय प्रक्रिया को उल्टा चला सकता है यानी आरएनए से डीएनए बनवा सकता है।
अब नई खोज से इसमें एक और पेंच आ गया है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस का बैक्टीरिया संस्करण खोजा गया है। यह आरएनए अणु का इस्तेमाल सांचे के रूप में करके डीएनए में सर्वथा नए जीन्स जोड़ सकता है। ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए ये जीन फिर से आएनए में बदल सकते हैं और प्रोटीन का निर्माण करवा सकते हैं। ऐसे प्रोटीन का निर्माण तब किया जाता है जब कोई वायरस बैक्टीरिया को संक्रमित कर दे। यहां बताना मुनासिब है कि वायरस का रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस नए जीन्स का निर्माण नहीं करता; वह तो मात्र आरएनए में लिखी सूचना को डीएनए में बदलता है।
एक मायने में यह बैक्टीरिया के सुरक्षा तंत्र का हिस्सा है। वायरस संक्रमण के विरुद्ध बैक्टीरिया की एक और सुरक्षा व्यवस्था होती है जो आजकल क्रिस्पर नामक जीन संपादन तकनीक के रूप में मशहूर है। इस तकनीक से बैक्टीरिया वायरस के डीएनए/आरएनए के कुछ अंशों को अपने डीएनए में जोड़ लेता है और फिर ये उस वायरस की पहचान में काम आते हैं।
जिस नई व्यवस्था की खोज हुई है वह थोड़ी ज़्यादा रहस्यमय है। इस तंत्र की कार्यविधि का खुलासा कोलंबिया विश्वविद्यालय के स्टीफन टैंग और सैमुअल स्टर्नबर्ग ने किया है। यह देखा गया था कि कतिपय बैक्टीरिया के डीएनए में एक जीन होता है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस का कोड होता है और आरएनए का छोटा-सा खंड होता है जिसका कोई प्रकट काम नहीं होता यानी यह किसी प्रोटीन का निर्माण नहीं करवाता। टैंग और स्टर्नबर्ग ने क्लेबसिएला न्यूमोनिए (Klebsiella pneumoniae) में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस द्वारा बनाए गए डीएनए अणु की तलाश की। पता चला कि यह डीएनए की अति दीर्घ शृंखला थी जिसमें एक सरीखे खंड बार-बार दोहराए गए थे और प्रत्येक खंड का अनुक्रम उस रहस्यमय आरएनए के खंडों से मेल खाता था।
ऐसा कैसे होता है? शोधकर्ताओं का मत है कि लंबे-लंबे आरएनए सूत्र मुड़कर हेयरपिन का आकार ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा होने पर एक ही शृंखला के दो दूर-दूर के खंड पास-पास आ जाते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि क्लेबसिएला न्यूमोनिए का ट्रांसक्रिप्टेस इस आरएनए शृंखला को डीएनए में तबदील करते समय बार-बार उसी स्थान की नकल बनाता है और इस तरह दोहराव वाली डीएनए शृंखला बन जाती है।
इस तरह बनी दोहराव वाली शृंखला प्रोटीन-कोडिंग शृंखला बन जाती है जिसमें प्रोटीन निर्माण के समापन को दर्शाने वाला कोई संकेत नहीं होता – इसलिए इसे ओपन रीडिंग फ्रेम कहते हैं और शोधकर्ताओं ने इस शृंखला को नाम दिया है नेवर एंडिंग ओपन रीडिंग फ्रेम (neo – नीयो)। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि वायरस का संक्रमण नीयो प्रोटीन के निर्माण को प्रेरित करता है। इस प्रोटीन का असर यह होता है कि उस प्रोटीन से युक्त कोशिका विभाजन करना बंद कर देती है। इससे तो लगता है कि यह उस कोशिका के लिए एक नया प्रोटीन है। अर्थात यहां रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस की मदद से एक सर्वथा नया जीन बैक्टीरिया के जीनोम में जुड़ रहा है। यह खोज जीव विज्ञान में एक नई कार्य प्रणाली की उपस्थिति का संकेत है। (स्रोत फीचर्स)
नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
Photo Credit : https://www.science.org/do/10.1126/science.z7w7tq5/abs/klebsiella_pneumoniae_bacteria_13743456084_resize.jpg