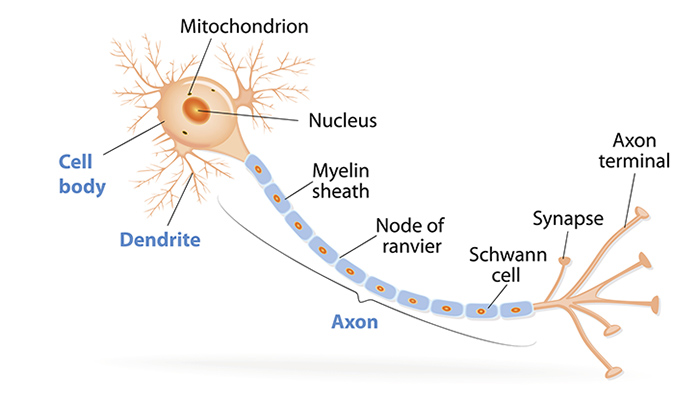ज़ुबैर सिद्दिकी

पिछले सौ साल से भी ज़्यादा समय से च्यूइंग गम (chewing gum) सिर्फ मुखवास के तौर पर नहीं, बल्कि मन को सुकून देने वाली चीज़ के रूप में बेचा जाता रहा है। दावा किया जाता था कि च्यूइंग गम तंत्रिकाओं को शांत करता है और मन को हल्का (stress relief) करता है। आज वही दावे आ रहे हैं – फर्क यह है कि अब लग रहा है कि इसमें थोड़ा हाथ शायद मनोविज्ञान और तंत्रिका विज्ञान (neuroscience) का भी है।
हालांकि, थोड़ी सतर्कता ज़रूरी भी है क्योंकि ऐसे वैज्ञानिक दावे तब आ रहे हैं जब कोविड-19 के बाद च्यूइंग गम की बिक्री तेज़ी से घटी है। कोविड-19 (covid-19 pandemic) महामारी के दौरान अमेरिका में च्यूइंग गम का इस्तेमाल काफी कम हो गया था। लोग कम बाहर निकलते, कम मिलते-जुलते और सांस की ताज़गी की चिंता में कमी भी थी। अब कंपनियां लोगों को लुभाने के लिए च्यूइंग गम को मानसिक सेहत से जोड़कर पेश कर रही हैं।
च्यूइंग गम एक अजीब लत है। इससे कोई पोषण नहीं मिलता और यह जल्द ही बेस्वाद हो जाती है; फिर भी लोग इसे लंबे समय तक चबाते रहते हैं। क्यों?
यह सवाल वैज्ञानिकों को लंबे समय से परेशान करता रहा है। शोध बताते हैं कि च्यूइंग गम चबाने से ध्यान (concentration) थोड़ा बेहतर होता है और कुछ हद तक तनाव कम (stress reduction) होता है, लेकिन इसका कारण अब तक पूरी तरह समझ में नहीं आया है। दिलचस्प बात यह है कि मनुष्य हज़ारों सालों से च्यूइंग गम जैसी चीज़ें चबा रहे हैं।
पुरातात्विक सबूत (archaeological evidence) बताते हैं कि मनुष्य करीब 8000 साल पहले भी चिपचिपी चीज़ें चबाया करते थे। स्कैंडिनेविया में पेड़ों की छाल से बनी प्राचीन गम (ancient chewing gum) मिली है, जिस पर दांतों के निशान मौजूद हैं। कुछ निशान छोटे बच्चों के भी थे। इससे लगता है कि पुराने समय में गोंद चबाना सिर्फ औज़ारों के लिए गोंद नरम करने तक सीमित नहीं था, बल्कि लोगों को इससे आनंद भी मिलता होगा।
अमेरिका में च्यूइंग गम
आधुनिक समय में च्यूइंग गम की शुरुआत अमेरिका में 1800 के दशक में हुई थी। अलबत्ता, च्यूइंग गम को लोकप्रिय बनाने का काम विलियम रिग्ले जूनियर (William Wrigley Jr.) ने किया। पहले साबुन और बेकिंग सोडा के साथ च्यूइंग गम मुफ्त दिए गए। लोकप्रियता बढ़ने पर 1890 के दशक में सिर्फ च्यूइंग गम का कारोबार शुरू कर दिया। 20वीं सदी की शुरुआत तक च्यूइंग गम हर जगह दिखने लगी। हालांकि इससे सभी खुश नहीं थे – सार्वजनिक जगहों पर च्यूइंग गम चबाने की आलोचना हुई और सड़कों पर थूके गए च्यूइंग गम से प्रशासन परेशान रहने लगे।
युद्ध में च्यूइंग गम
पहले विश्व युद्ध (World War I) के दौरान विलियम रिग्ले ने अमेरिकी सेना को सुझाव दिया कि च्यूइंग गम सैनिकों के लिए फायदेमंद हो सकता है। उनका कहना था कि इससे भूख कुछ हद तक दबाई जा सकती है, दांत साफ रहते हैं और तनाव कम होता है। सेना ने यह बात मान ली।
इसके बाद च्यूइंग गम सैनिकों के राशन (military ration) का हिस्सा बन गई। अमेरिकी सैनिकों के साथ च्यूइंग गम युरोप, एशिया और बाकी दुनिया में फैली। इसी दौरान अखबारों में यह बातें छपने लगीं कि च्यूइंग गम चबाने से चिंता कम होती है, नींद अच्छी आती है और उदासी दूर होती है। इन्हीं दावों से वैज्ञानिकों की इसमें रुचि बढ़नी शुरू हुई।
शुरुआती अध्ययन
1940 के दशक में अमेरिका के बार्नार्ड कॉलेज (Barnard College) में च्यूइंग गम पर किए गए शोध में पाया गया कि च्यूइंग गम चबाने वाले लोग थोड़ा कम तनाव महसूस करते थे और उनका काम करने का तरीका कुछ बेहतर लगता था। तब वैज्ञानिक यह नहीं समझ पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है।
कई साल बाद कार्डिफ युनिवर्सिटी (Cardiff University) के मनोवैज्ञानिक एंड्र्यू स्मिथ (Andrew Smith) ने करीब 15 साल तक च्यूइंग गम चबाने के असर का अध्ययन किया। उनके कुछ शोध च्यूइंग गम बनाने वाली कंपनी के सहयोग से हुए थे, इसलिए नतीजों पर सवाल भी उठे। स्मिथ ने पाया कि च्यूइंग गम चबाने से याददाश्त में कोई खास सुधार नहीं होता – लोग कहानियां या शब्द दूसरों से बेहतर याद नहीं रख पाते। अलबत्ता, कुछ और असर ज़रूर देखने को मिले। कई शोधों में यह बात सामने आई कि च्यूइंग गम के दो असर साफ हैं। पहला, इससे सतर्कता और एकाग्रता थोड़ी देर तक बेहतर बनी रहती है। दूसरा, कुछ स्थितियों में तनाव कम महसूस होता है।
अध्ययनों के अनुसार च्यूइंग गम चबाने से सतर्कता (alertness) लगभग 10 प्रतिशत तक बढ़ सकती है, खासकर तब जब काम बहुत लंबा, उबाऊ या मशीनी हो। जैव-मनोवैज्ञानिक (biopsychology) क्रिस्टल हैस्केल-रैम्से के शोध में भी यही नतीजे मिले। उन्होंने पाया कि च्यूइंग गम चबाने से ध्यान लगाने में तब ज़्यादा मदद मिलती है, जब व्यक्ति पहले से थका हुआ या मानसिक रूप से बोझिल हो (mental benefit)। लेकिन अगर कोई पहले ही पूरी तरह सतर्क है, तो गम से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तनाव कम होने के मामले में, इसके असर के प्रमाण अपेक्षाकृत ज़्यादा मज़बूत पाए गए।
प्रयोगशाला (laboratory studies) में किए गए अध्ययनों में पाया गया कि जब लोग सार्वजनिक भाषण देने या गणित के कठिन सवाल हल करने जैसे तनाव वाले काम के दौरान च्यूइंग गम चबाते हैं, तो उनकी घबराहट कुछ कम हो जाती है। अस्पतालों में हुए अध्ययनों में दिखा कि कुछ सर्जरी से पहले च्यूइंग गम चबाने वाली महिलाओं की चिंता कम थी।
हालांकि च्यूइंग गम कोई जादू नहीं है। बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति में – जैसे ऑपरेशन से ठीक पहले या बेहद कठिन हालात में – यह मददगार साबित नहीं होता। कुल मिलाकर, च्यूइंग गम मानसिक रूप से थोड़ा फायदा ज़रूर देता है। लेकिन इसके पीछे के कारण अब भी पूरी तरह समझ में नहीं आए हैं। अलबत्ता, कुछ संभावनाएं बताई गई हैं।
एक विचार यह है कि चबाने से चेहरे की मांसपेशियां सक्रिय होती हैं, जिससे मस्तिष्क तक खून का प्रवाह बढ़ जाता है। दूसरी धारणा यह है कि मांसपेशियों की हल्की गतिविधि एकाग्रता में मदद करती है, जिससे दिमाग अधिक सक्रिय रहता है।
तीसरा विचार है कि चबाना शरीर की तनाव-नियंत्रण प्रणाली को प्रभावित कर सकता है, जो कॉर्टिसोल नामक हार्मोन को नियंत्रित करती है। यह हार्मोन सतर्कता और तनाव दोनों से जुड़ा होता है। अध्ययनों में इसके नतीजे मिले-जुले रहे हैं – कभी कॉर्टिसोल (cortisol hormone) बढ़ा, जो ध्यान बढ़ने के संकेत है, तो कभी यह घटा, जो तनाव कम होने का संकेत है।
चबाना क्या नैसर्गिक आदत है?
कुछ वैज्ञानिकों ने यह सवाल उठाया है कि क्या चबाने की आदत (chewing behavior) बहुत पुराने समय से हमारे भीतर मौजूद है। कई जानवर तनाव में कुछ न कुछ चबाते हैं – जैसे कुत्ते खिलौने कुतरते हैं और शाकाहारी जानवर लगातार जुगाली करते रहते हैं। इसलिए माना गया कि शायद चबाना एक स्वाभाविक तरीके से मन को शांत करने वाली क्रिया हो।
लेकिन वैज्ञानिक एडम वैन कैस्टरेन (Adam van Casteren) इससे अलग बात कहते हैं। उनके अनुसार इंसान अपने करीबी प्राइमेट (primates) रिश्तेदारों की तुलना में बहुत कम चबाता है। चिंपैंज़ी दिन में 4–5 घंटे और गोरिल्ला करीब 6 घंटे तक चबाते रहते हैं, जबकि इंसान औसतन सिर्फ 35 मिनट ही भोजन चबाता है। खाना पकाने और औज़ारों के विकास से इंसानों को ज़्यादा चबाने की ज़रूरत नहीं रही, और बची हुई ऊर्जा मस्तिष्क के विकास में लगी।
इसलिए च्यूइंग गम को किसी पुरानी जीवन-रक्षा आदत का हिस्सा नहीं माना जाता। वैन कैस्टरेन का मानना है कि इसकी वजह कहीं ज़्यादा सरल है – इंसानों को बार-बार होने वाली हल्की और दोहराई जाने वाली गतिविधियां पसंद आती हैं।
सोचते वक्त लोग अक्सर पैर हिलाते हैं, पेन क्लिक करते हैं, स्ट्रेस बॉल दबाते हैं या कागज़ पर कुछ बनाते रहते हैं। शोध बताते हैं कि ऐसी छोटी-छोटी दोहराई जाने वाली हरकतें लंबे काम के दौरान ध्यान बनाए रखने में मदद करती हैं।
कैलिफोर्निया युनिवर्सिटी (University of California) के शोध में पाया गया कि जब एकाग्रता के अभाव और अति सक्रियता (ADHD) से पीड़ित बच्चों को काम करते समय खुलकर हिलने-डुलने दिया गया तो उनका प्रदर्शन बेहतर रहा। च्यूइंग गम भी कुछ ऐसा ही काम करता है और दिमाग बेहतर तरीके से ध्यान लगा पाता है।
आज की तेज़ रफ्तार, स्क्रीन और तनाव से भरी दुनिया में च्यूइंग गम से मिलने वाली ज़रा-सी राहत शायद इसकी सबसे बड़ी ताकत है। वैज्ञानिक जब यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि शरीर की हलचल मस्तिष्क (brain function) को कैसे प्रभावित करती है, तब च्यूइंग गम हमें याद दिलाता है कि मस्तिष्क अकेले काम नहीं करता। कई बार जबड़ा हिलाने जैसी क्रिया भी हमारे सोचने और महसूस करने के तरीके को बदल सकती है। (स्रोत फीचर्स)
नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
Photo Credit : https://m.economictimes.com/thumb/msid-126467722,width-1200,height-900,resizemode-4,imgsize-32812/chewing-gum-health-benefits.jpg