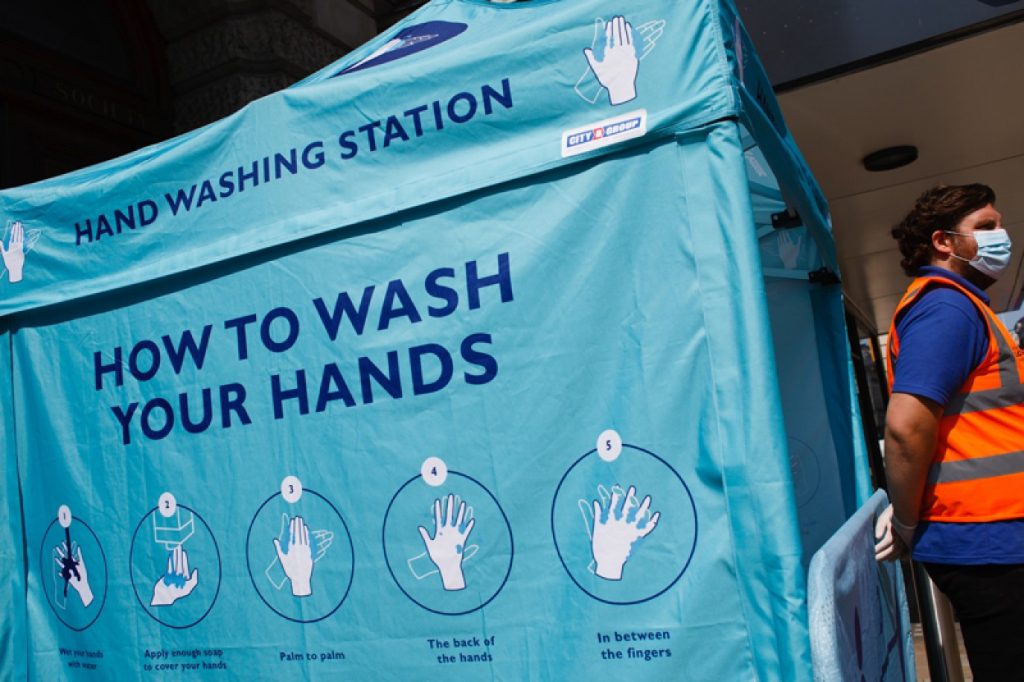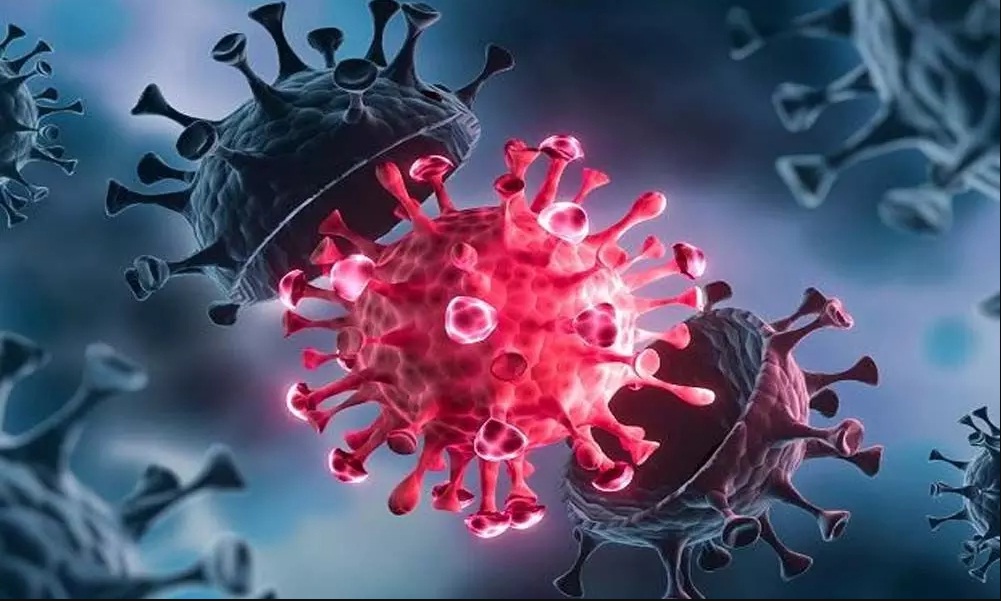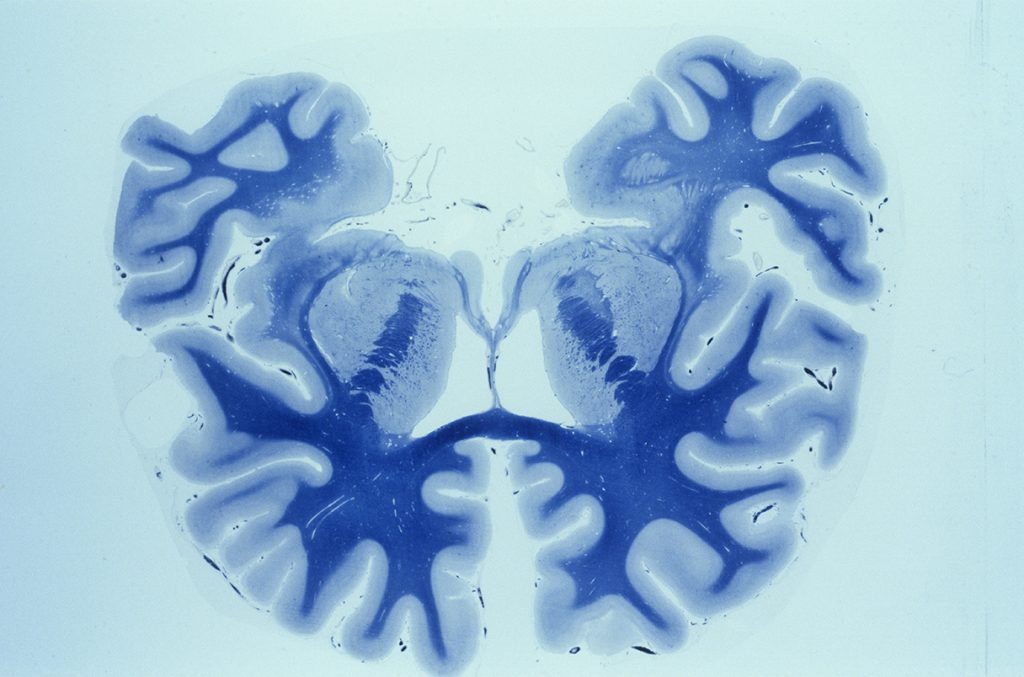हाल ही में अमेरिकी सरकार ने mRNA आधारित टीकों की दूसरी खुराक के आठ महीने बाद अधिकांश लोगों को बूस्टर शॉट देने का निर्णय लिया है। टीका सलाहकार समिति की स्वीकृति के बाद 20 सितंबर से बूस्टर शॉट देना शुरू किए जाएंगे। इसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और नर्सिंग होम कर्मियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
वैज्ञानिक समुदाय में बूस्टर शॉट देने पर काफी पहले से बहस चल रही है कि यह किन लोगों को और कब दिया जाना चाहिए। दुर्बल प्रतिरक्षा वाले लोगों में दो खुराक पर्याप्त नहीं हैं इसलिए सीडीसी ने ऐसे लोगों को बूस्टर शॉट देने का सुझाव दिया था। वर्तमान घोषणा इस्राइल, टीका निर्माताओं और अमेरिका में किए गए विभिन्न अध्ययनों से प्राप्त डैटा के आधार पर लिया गया है। इन अध्ययनों के अनुसार कोविड के विरुद्ध टीकों से मिलने वाली प्रतिरक्षा 6 माह में कम हो सकती है और डेल्टा संस्करण को रोकने में कम प्रभावी होगी।
कई विशेषज्ञ स्वस्थ लोगों को बूस्टर शॉट देने के पक्ष में नहीं हैं। जब कई देशों में लोगों को एक खुराक भी नहीं मिली है तब उच्च आय वाले देशों द्वारा बूस्टर शॉट देने को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अनैतिक बताया है। लेकिन अमेरिकी सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा पर अधिक ज़ोर दे रही है। कुछ विशेषज्ञों का मत है कि बूस्टर शॉट की बजाय अधिक से अधिक लोगों के टीकाकरण पर ध्यान देना अधिक प्रभावी होगा।
इस विषय में साइंटिफिक अमेरिकन ने ला जोला इंस्टिट्यूट फॉर इम्यूनोलॉजी के वायरोलॉजिस्ट और प्रोफेसर शेन क्रोटी और बाइडेन-हैरिस ट्रांज़ीशन कोविड-19 एडवाइज़री बोर्ड की सदस्य सेलिन गाउंडर से बूस्टर शॉट के सम्बंध में कुछ सवाल किए हैं।
क्या बूस्टर शॉट आवश्यक है? और किसके लिए?
सेलिन गाउंडर: डैटा के अनुसार टीके गंभीर रूप से बीमार होने, अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु से सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह सुरक्षा डेल्टा संस्करण के विरुद्ध भी देखने को मिली है। हालांकि, हमें डेल्टा संस्करण के विरुद्ध कम प्रतिरक्षा देखने को मिली है। यहां जिन समूहों को बूस्टर शॉट देने की बात की जा रही है वे अत्यधिक दुर्बल प्रतिरक्षा वाले लोग हैं जिनमें टीकाकरण से कम प्रतिक्रिया देखने को मिली है। इनमें से सभी तो नहीं लेकिन कुछ लोगों में अतिरिक्त खुराक से प्रतिक्रिया अवश्य विकसित होगी। इसके अलावा नर्सिंग होम जैसे स्थान, जहां ब्रेकथ्रू संक्रमण का खतरा है, वहां भी अतिरिक्त खुराक देना समझदारी का निर्णय है। इससे आगे बढ़कर, आम जनता को अतिरिक्त खुराक देने के लिए कोई स्पष्ट डैटा अभी उपलब्ध नहीं है।
शेन क्रोटी: डेल्टा संस्करण के बारे में अनिश्चितता और इसके विरुद्ध सुरक्षा को लेकर अस्पष्टता के कारण सरकार ने बूस्टर शॉट देने का निर्णय लिया होगा। निश्चित रूप से दुर्बल प्रतिरक्षा वाले लोगों को बूस्टर शॉट दिया जाना चाहिए। मई, जून और जुलाई के डैटा से पता चला है कि दुर्बल प्रतिरक्षा वाले लोगों को दो खुराक मिलने पर अच्छी प्रतिक्रिया तो नहीं मिली लेकिन तीसरी खुराक से बेहतर प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। यह स्पष्ट हुआ है कि दुर्बल प्रतिरक्षा वाले कुछ लोगों को तीसरी खुराक से फायदा हुआ है। 80 से अधिक आयु के लोगों को बूस्टर देने की बात भी उचित लगती है। लेकिन 70, 60, 50 वर्ष की आयु वर्ग के लिए निर्णय मुश्किल है।
टीकों द्वारा उत्पन्न प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया कितनी प्रभावी है?
क्रोटी: अभी तक ऐसा प्रतीत होता है कि टीका उच्च-गुणवत्ता वाली प्रतिरक्षा स्मृति उत्पन्न करता है। साइंस में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार मॉडर्ना टीके की दूसरी खुराक के छ: माह बाद भी एंटीबॉडीज़ में कोई कमी नहीं पाई गई। टीकाकरण के एक से छ: माह के दौरान स्मृति टी-कोशिका में भी लगभग कोई बदलाव नहीं आया। इंग्लैंड का डैटा दर्शाता है कि टीका डेल्टा संस्करण के विरुद्ध बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। सर्दियों में आई लहर के दौरान अस्पताल में भर्ती होने और मौतों के बीच भारी अंतर था। मेरे खयाल से अस्पताल में दाखिले और मौतों से बचाव के लिए तो बूस्टर नहीं चाहिए।
इस्राइल के डैटा के बारे में आपका क्या विचार है जो समय के साथ प्रतिरक्षा कम होना दर्शाता है?
क्रोटी: टीके की प्रभाविता कम होने के मामले में इस्राइल का डैटा काफी अच्छा है। लेकिन अभी तक इस्राइली अधिकारियों ने इसे किसी वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशित नहीं किया है। भ्रमित करने वाले कारक भी काफी अधिक हैं। सबसे पहले इस्राइल को फरवरी और मार्च में टीके की प्रभाविता को लेकर काफी समस्याएं थीं। उसके बाद उन्होंने एक पेपर प्रकशित किया जिसमें टीके को अच्छा बताया गया। अब इस्राइल को लग रहा है कि टीके की प्रभाविता में कमी आ रही है।
गाउंडर: इस्राइल के डैटा के साथ काफी समस्याएं हैं। उनमें उम्र एवं अन्य कारकों को अलग-अलग नहीं किया गया है। इसके लिए मूल डैटा प्रदान करना होगा। इस्राइल के डैटा के आधार पर कोई निर्णय लेना मुझे उचित नहीं लगता है। इसके अलावा, प्रयोगशाला डैटा से भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तथाकथित न्यूट्रलाइज़िंग एंटीबॉडी सुरक्षा का सबसे अच्छा मापदंड है। लेकिन यदि उन्हें छ: माह बाद मापा जाए तो यह स्पष्ट नहीं होता है। यदि आपके पास अब तक के हर संक्रमण की एंटीबॉडी होगी तो आपका रक्त वास्तव में एंटीबॉडी से पट जाएगा।
क्या टीकों का मिला-जुला उपयोग किया जा सकता है?
क्रोटी: जिन लोगों को वायरस आधारित (जैसे एस्ट्राज़ेनेका या जॉनसन एंड जॉनसन टीका) टीका मिला है उनके लिए उसी टीके की एक और खुराक की बजाय mRNA टीका लेना बेहतर है। टीकों का क्रम काफी महत्वपूर्ण है।
गाउंडर: इसके अलावा हमें नाक से दिए जाने वाले टीकों पर भी विचार करना चाहिए। इनसे नाक और ऊपरी श्वसन मार्ग में प्रतिरक्षा विकसित की जा सकती है।
क्या तीसरी खुराक के कुछ दुष्प्रभाव होंगे? यदि हां, तो कितने गंभीर हो सकते हैं?
गाउंडर: लक्षण कमोबेश हल्का बुखार, बदनदर्द, थकान जैसे हो सकते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि सभी को ऐसे लक्षण हों।
जब विश्व के अधिकांश लोगों को टीका नहीं लगा है तब टीकाकृत लोगों को बूस्टर शॉट देना कितना नैतिक है?
क्रोटी: मुझे लगता है कि यह एक झूठा विवाद है। समय के साथ टीके एक्सपायर हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में बेहतर तो यह है कि अमेरिका में जिन लोगों को टीका नहीं लगा है उनको टीकाकृत कर दिया जाए। यह विकल्प बूस्टर शॉट देने से बेहतर होगा।
गाउंडर: यह तो स्पष्ट है कि लोगों को अतिरिक्त खुराक देने से कुछ खास परिणाम नहीं मिलने वाले हैं। बल्कि बिना टीका लगे लोगों का टीकाकरण करना सामुदायिक रूप से प्रसार को थामने के लिए अधिक प्रभावी हो सकता है।(स्रोत फीचर्स)
नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
Photo Credit : https://static.scientificamerican.com/sciam/cache/file/45882622-B7C5-4384-83C86CB283E0ADBA_source.jpg?w=590&h=800&F1000449-DBC9-462A-A1A54C9CBEF04B14