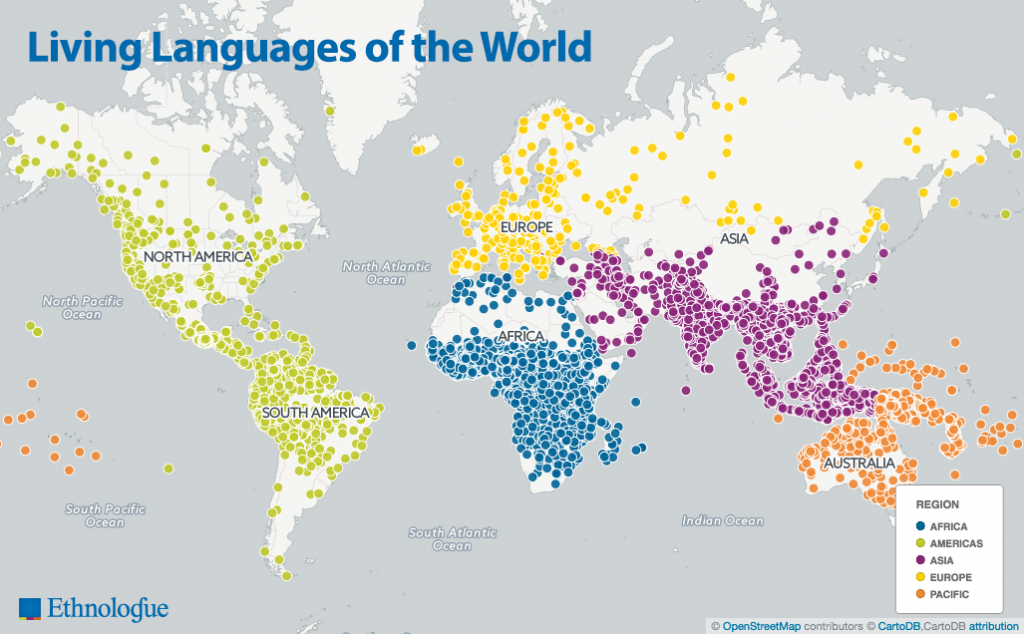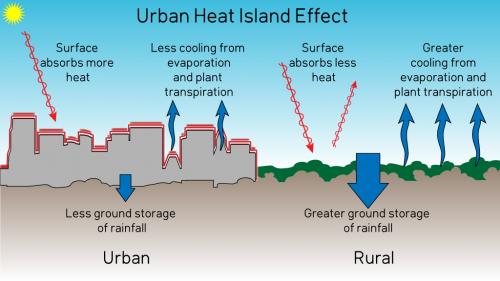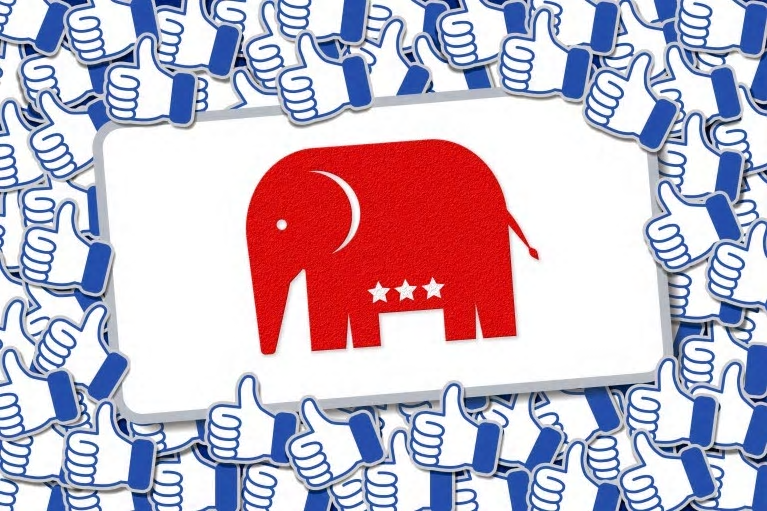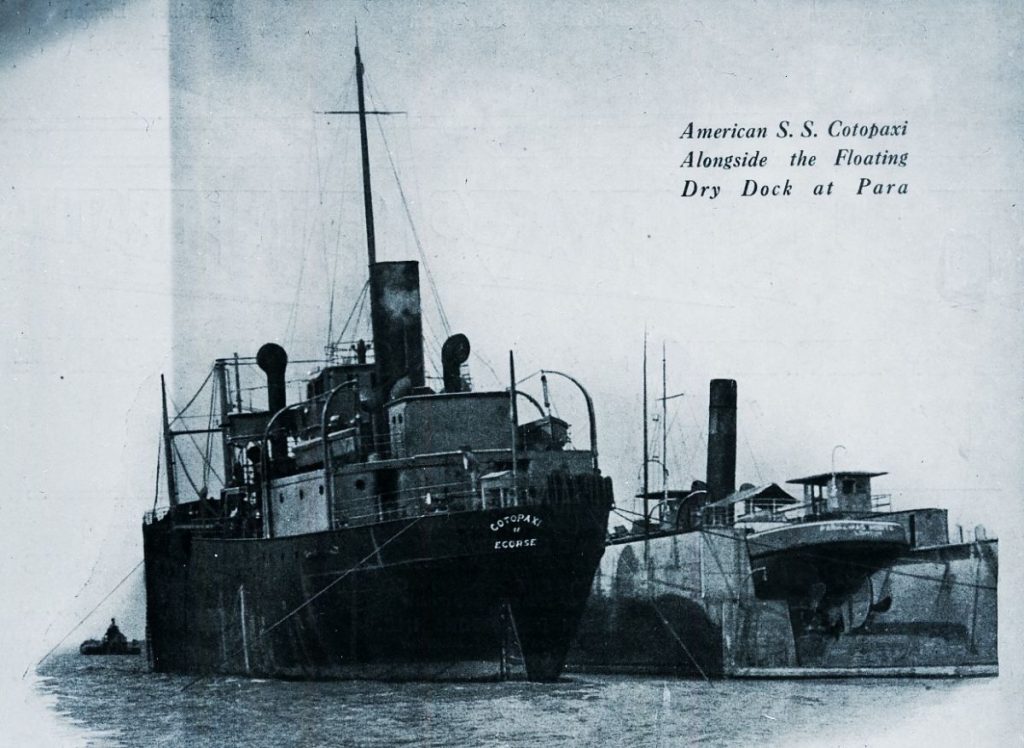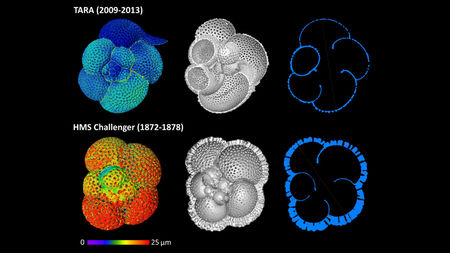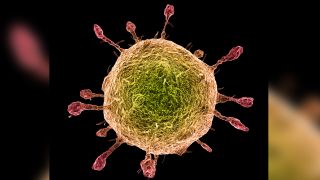हैंस लिपरशे द्वारा दूरबीन के आविष्कार के बाद गैलीलियो ने स्वयं दूरबीन का पुनर्निर्माण करके पहली बार खगोलीय अवलोकन में उपयोग किया था। तब से लगभग चार शताब्दियां बीत चुकी हैं। तब से अब तक दूरबीनों ने खगोल विज्ञान में कई आकर्षक और पेचीदा खोजों को संभव बनाया है। इनमें हमारे सूर्य से परे अन्य तारों की परिक्रमा कर रहे ग्रहों की खोज, ब्राहृांड के फैलने की गति में तेज़ी के सबूत, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का अस्तित्व, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं वगैरह की खोज शामिल है।
आज बहुत-सी विशालकाय दूरबीनों का निर्माण किया जा चुका है। इनमें कई धरती पर लगी हैं तो कुछ अंतरिक्ष में भी स्थापित हैं। खगोलीय पिंड दृश्य प्रकाश के अलावा कई तरह के विद्युत चुंबकीय विकिरण (इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक रेडिएशन) का भी उत्सर्जन करते हैं। दूरस्थ खगोलीय पिंडों से उत्सर्जित विद्युत-चुंबकीय विकिरण का ज़्यादातर हिस्सा पृथ्वी का वायुमंडल सोख लेता है और इस वजह से पृथ्वी पर स्थित विशाल प्रकाशीय (ऑप्टिकल) दूरबीनों से उन खगोलीय पिंडों को भलीभांति नहीं देखा जा सकता है। पृथ्वी की वायुमंडलीय बाधा को दूर करने एवं दूरस्थ खगोलीय पिंडों के सटीक प्रेक्षण के लिए ‘अंतरिक्ष दूरबीनों’ का निर्माण किया गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चार बड़ी दूरबीनों या वेधशालाओं को अंतरिक्ष में उतारा है – हबल स्पेस टेलीस्कोप, कॉम्पटन गामा रे आब्ज़र्वेटरी (सीजीआरओ), चंद्रा एक्स-रे टेलीस्कोप और आखरी स्पिट्ज़र टेलीस्कोप।
30 जनवरी 2020 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने ‘स्पिट्ज़र टेलीस्कोप मिशन’ की समाप्ति की घोषणा कर दी। हालांकि इसका निर्धारित जीवनकाल केवल ढाई वर्ष था फिर भी इसने लगभग 16 वर्षों तक अपनी भूमिका दक्षतापूर्वक निभाई। गौरतलब है कि स्पिट्ज़र स्पेस टेलीस्कोप 950 किलोग्राम वज़नी एक ऐसा खगोलीय टेलीस्कोप है जिसे अंतरिक्ष में एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया है, इसलिए यह सूर्य के चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाता है। यह ब्राहृांड की विभिन्न वस्तुओं की इन्फ्रारेड प्रकाश में जांच करता है। दरअसल, स्पिट्ज़र अंतरिक्ष में वह सब कुछ देखने में सक्षम था जिसे प्रकाशीय दूरबीनों के जरिए नहीं देखा जा सकता है। अंतरिक्ष का ज़्यादातर हिस्सा गैस और धूल के विशाल बादलों से भरा है जिसके पार देखने की क्षमता हमारे पास नहीं हैं। मगर इन्फ्रारेड प्रकाश गैस और धूल के बादलों की बड़ी से बड़ी दीवारों को भी भेद सकता है। स्पिट्ज़र अपने विशाल टेलीस्कोप और क्रायोजनिक सिस्टम से ठंडे रखे जाने वाले तीन वैज्ञानिक उपकरणों के साथ अब तक का सबसे बड़ा इन्फ्रारेड टेलीस्कोप है।
स्पिट्ज़र को 25 अगस्त, 2003 को अमेरिका के केप कैनवरेल से डेल्टा रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया था। शुरुआत में इसका नाम ‘स्पेस इन्फ्रारेड टेलीस्कोप फेसिलिटी’ था लेकिन नासा की परंपरा के अनुसार ऑपरेशन के सफल प्रदर्शन के बाद बीसवीं सदी के एक महान खगोलविद लिमन स्पिट्ज़र के सम्मान में ‘स्पिट्ज़र’ नाम दिया गया। गौरतलब है कि लिमन स्पिट्ज़र 1940 के दशक में अंतरिक्ष दूरबीनों की अवधारणा को बढ़ावा देने वाले अग्रणी व्यक्तियों में से एक थे। स्पिट्ज़र टेलीस्कोप में इन्फ्रारेड ऐरे कैमरा, इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ और मल्टीबैंड इमेजिंग फोटोमीटर नामक तीन उपकरणों को रखा गया था। इन्फ्रारेड चूंकि एक तरह का गर्म विकिरण होता है, इसलिए इन तीनों उपकरणों को विकिरण से भस्म होने से बचाने और ठंडा रखने के लिए एब्सोल्यूट ज़ीरो यानी शून्य से 273 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक तापमान रखने के लिए तरल हीलियम का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा सौर विकिरण से बचाव के लिए स्पिट्ज़र को सौर कवच से भी सुसज्जित किया गया था।
यों तो स्पिट्ज़र टेलीस्कोप द्वारा की गई खोजों की सूची काफी लंबी है, मगर उसके ज़रिए की गई प्रमुख खोजों की चर्चा ज़रूरी है। इस टेलीस्कोप ने न केवल ब्राहृांड की सबसे पुरानी निहारिकाओं के बारे में हमें जानकारी उपलब्ध कराई है बल्कि शनि के चारों ओर मौजूद एक करोड़ तीस लाख किलोमीटर के दायरे में एक नए वलय का भी खुलासा किया है। इसने धूल कणों के विशालकाय भंडार के माध्यम से नए तारों और ब्लैक होल्स का भी अध्ययन किया। स्पिट्ज़र ने हमारे सौर मंडल से परे अन्य ग्रहों की खोज में सहायता की, जिसमें पृथ्वी के आकार वाले सात ग्रह जो ट्रैपिस्ट-1 नामक तारे के चारों ओर परिक्रमा कर रहे थे, के बारे में पता लगाना भी शामिल है। इसके अलावा क्षुद्रग्रहों और ग्रहों के टुकड़ों, बेबी ब्लैक होल्स, तारों की नर्सरियों यानी नेब्युला (जहां नए तारों का निर्माण होता है) की खोज, अंतरिक्ष में 60 कार्बन परमाणुओं से बनी त्रि-आयामी और गोलाकार संरचनाओं यानी बकीबॉल्स की खोज, निहारिकाओं के विशाल समूहों की खोज, हमारी आकाशगंगा (मिल्की-वे) का सबसे विस्तृत मानचित्रण आदि स्पिट्ज़र टेलीस्कोप की प्रमुख उपलब्धियों में शामिल हैं।
स्पिट्ज़र को ठंडा रखने के लिए तरल हीलियम बेहद ज़रूरी था, लेकिन 15 मई 2009 को इसका तरल हीलियम का टैंक खाली हो गया। वर्तमान में इसके ज़्यादातर उपकरण खराब हो चुके हैं। अलबत्ता, इसके दो कैमरे अभी भी काम कर रहे हैं और स्पिट्ज़र सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। नासा ने स्पिट्ज़र मिशन की हालिया समीक्षा की और पाया कि इसके कैमरे अभी भी काम कर रहे हैं। मगर इस टेलीस्कोप को अब संचालन के योग्य नहीं पाया गया, तो इसे रिटायर करने का फैसला लिया। नासा डीप स्पेस नेटवर्क के जरिए प्राप्त स्पिट्ज़र के सभी आंकड़ों के विश्लेषण में लगा हुआ है।
नासा में खगोल भौतिकी विभाग के निदेशक पॉल हर्ट्ज़ कहना है कि “अच्छा होगा अगर हमारे सभी टेलीस्कोप हमेशा के लिए कार्य करने में सक्षम होते, लेकिन यह संभव नहीं है। 16 साल से अधिक समय तक स्पिट्ज़र ने खगोलविदों को अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर अंतरिक्ष में काम करने का मौका दिया।” कुल मिलाकर, स्पिट्ज़र ने अपने 140 करोड़ डॉलर के मिशन के तहत 8 लाख आकाशीय लक्ष्यों की छानबीन की।
बहरहाल, ब्राहृांड की गहराइयों में झांकने के लिए और खोजों के इस सिलसिले को जारी रखने के लिए स्पिट्ज़र की जगह लेने को तैयार है लंबे समय से प्रतीक्षित इसका उत्तराधिकारी बेहद शक्तिशाली ‘जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप’। हालांकि जेम्स वेब और स्पिट्ज़र की कार्यप्रणाली में ज़मीन-आसमान का अंतर होगा, मगर जेम्स वेब भी स्पिट्ज़र की भांति इन्फ्रारेड की खिड़की का इस्तेमाल करके ब्राहृांड के अध्ययन में सक्षम होगा। अलविदा स्पिट्ज़र! (स्रोत फीचर्स)
नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
Photo Credit : https://solarsystem.nasa.gov/system/news_items/main_images/513_TOP-SpitzerPlanets_ArtistConcept.jpg