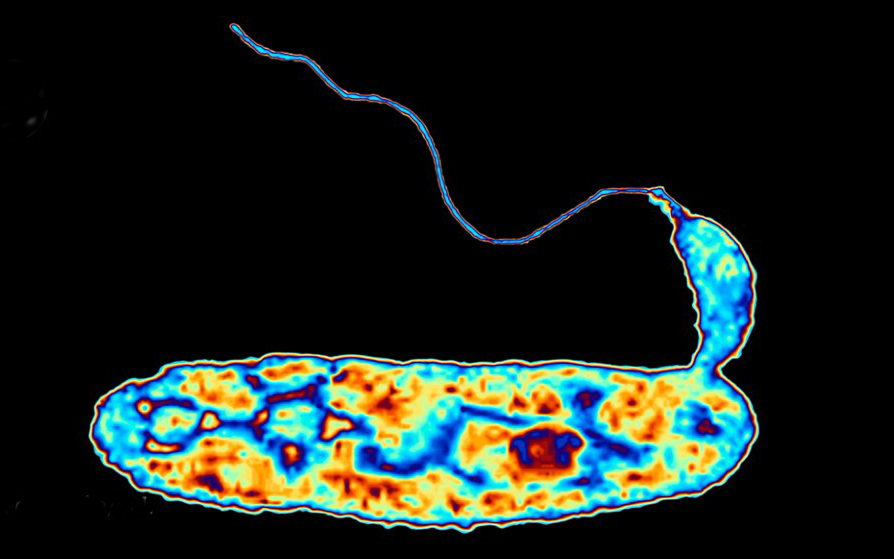किलर व्हेल के पुत्र मां के लाड़ले होते हैं। ये पुत्र काफी बड़े होने के बाद भी मां के पिछलग्गू बने रहते हैं जबकि पुत्रियां बड़ी होकर खुद संतानें पैदा करने लगती हैं। ऐसा क्यों है और किलर व्हेल मांएं इसकी क्या कीमत चुकाती हैं?
यह अवलोकन पहली बार किया गया है। यह तो पता रहा है कि किलर व्हेल मांएं अपने पुत्रों की बढ़िया देखभाल करती हैं लेकिन हाल के अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि मां इसकी क्या कीमत चुकाती हैं।
युनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर और सेंटर फॉर व्हेल रिसर्च के पारिस्थितिकीविद माइकल वाइस ने किलर व्हेल में मां-बेटे के सम्बंध के प्रत्यक्ष अवलोकन के आधार पर बताया है कि ये प्राणि दशकों तक जीते हैं लेकिन पूर्ण विकसित नर भी ऐसे व्यवहार करते हैं मानो वे छोटे बच्चे हों।
वाइस जानना चाहते थे कि गहन देखभाल में पल रहे इन बेटों की मां क्या कीमत चुकाती हैं – क्या ये उनकी और संतान पैदा करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं? इसके लिए वाइस के दल ने प्रशांत महासागर के तीन व्हेल समूहों के पिछले 40 वर्षों के आंकड़े खंगाले। इन समूहों को पॉड कहते हैं और इनमें प्राय: दो दर्जन तक सदस्य होते हैं। ये सभी मातृवंशीय होते हैं, साथ-साथ घूमते और शिकार करते हैं।
करंट बायोलॉजी में प्रकाशित शोध के मुताबिक इसका गहरा असर होता है। किसी भी वर्ष में बेटों की मांओं द्वारा एक और संतान पैदा करने की संभावना निसंतान मांओं और सिर्फ बेटियों की मांओं की तुलना में आधी होती है। आश्चर्यजनक बात यह रही कि संभावना में यह गिरावट पुत्रों की उम्र से स्वतंत्र थी। कहने का आशय यह है कि तीन साल का बेटा और 18 साल का बेटा मां की आगे संतानोत्पत्ति की संभावना में बराबर कमी लाता है।
शोधकर्ताओं का मत है कि मां द्वारा बेटों को तरजीह दिया जाना इनकी पॉड संरचना से सम्बंधित है। जब कोई मादा किलर व्हेल बच्चे जनती है और अपनी मां के समूह में बनी रहती है, तो वह और उसके बच्चे भोजन और ध्यान के लिए शेष बच्चों से होड़ करते हैं। दूसरी ओर, बेटे उस पॉड में और खाने वाले नहीं लाते। बेटे तो पास से गुज़रते समूहों की मादाओं के साथ समागम करते हैं जिसके फलस्वरूप बच्चे उन समूहों में पैदा होते हैं। यानी बेटों के बच्चे किसी और की ज़िम्मेदारी होते हैं। शोधकर्ताओं का मत है कि यदि मां चाहती है कि उसके अधिक से अधिक पोते-पोतियां हों तो उसके लिए बेटे में निवेश करना ज़्यादा फायदे का सौदा है।
यह अभी एक परिकल्पना है क्योंकि वाइस की टीम ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि बेटे मां के प्रजनन में व्यवधान कैसे कैसे डालते हैं। लेकिन उन्हें यदि अपने बच्चों की भोजन की ज़रूरतें पूरी करना पड़े तो उनकी प्रजनन क्षमता कमज़ोर पड़ ही जाएगी। वैसे अन्य विशेषज्ञों का कहना है कि शायद यह मात्र उन पॉड्स की समस्या हो जिनका अवलोकन वाइस ने किया है। एक मत यह भी है कि व्हेल उन चंद प्रजातियों में से है जिनमें रजोनिवृत्ति (मेनोपॉज़) होती है। यह भी संभव है कि ये बेटे बड़ा शिकार पकड़ने में मदद करते हों। इस संदर्भ में किलर व्हेल की अन्य प्रजातियों का अध्ययन मददगार होगा। (स्रोत फीचर्स)
नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
Photo Credit : https://imgs.mongabay.com/wp-content/uploads/sites/20/2019/04/10070731/1024px-Killerwhales_jumping.jpg