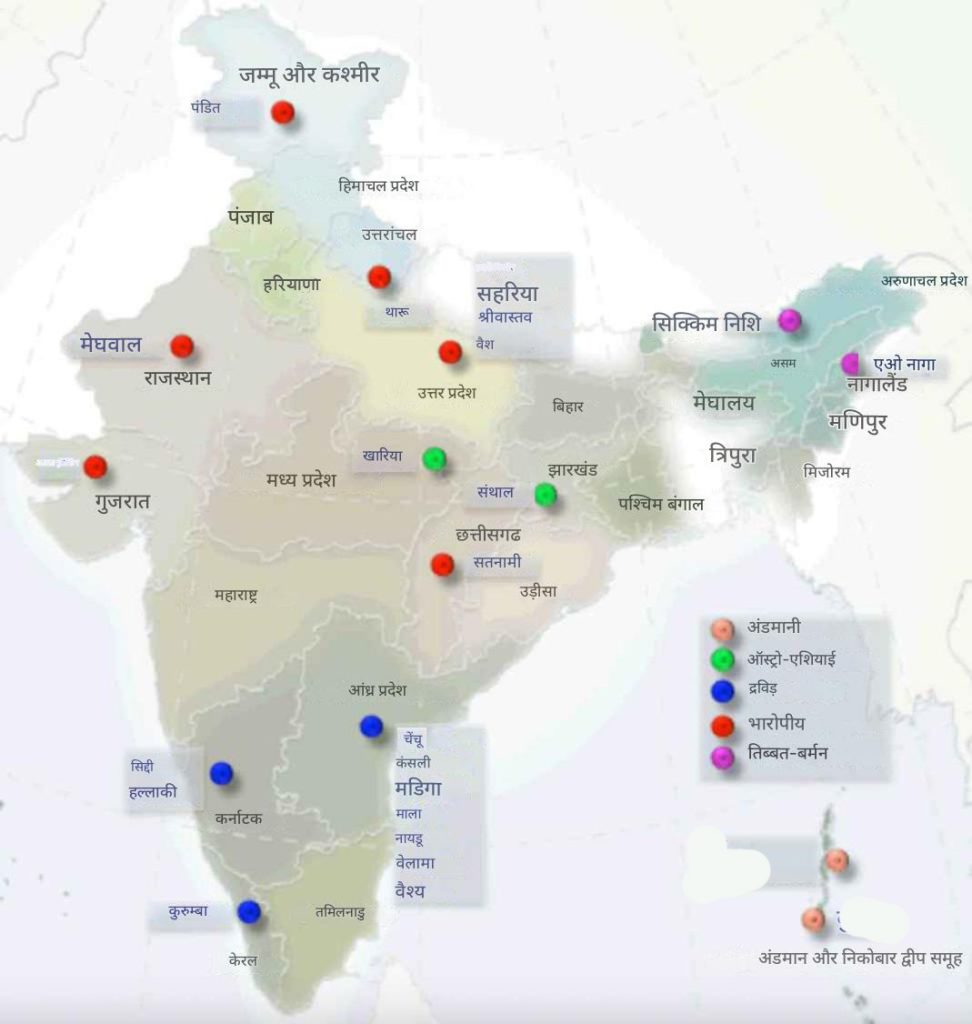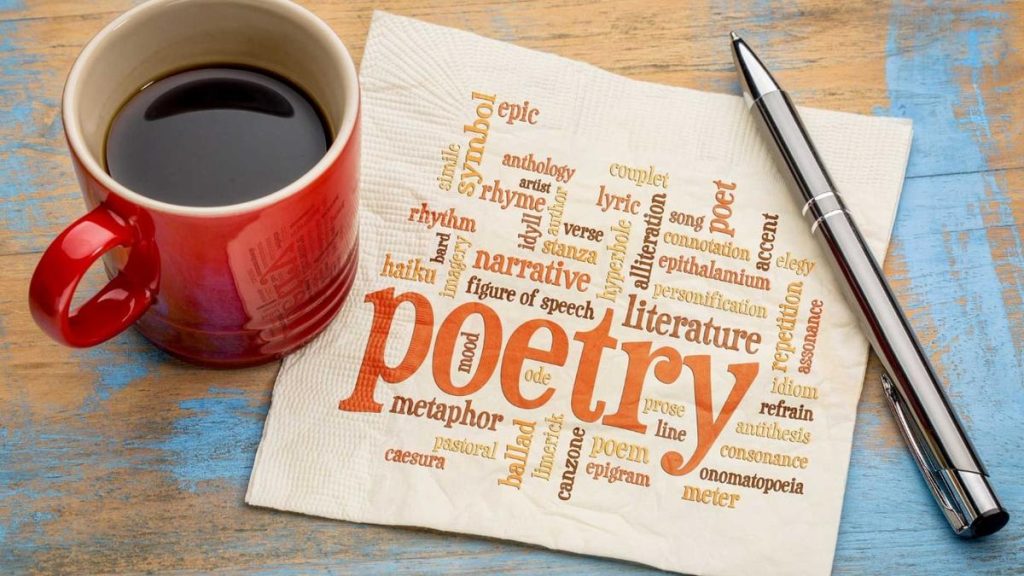हर्षदा अकोलकर, श्वेता कुलकर्णी

भारत की बढ़ती आबादी के लिए आवास और बुनियादी निर्माण की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए देश में भवन निर्माण (construction sector) और निर्माण सामग्री तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लेकिन यह बढ़त ऊर्जा खपत और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (greenhouse gas emissions) में भी काफी योगदान देती है। भवन-निर्माणों के पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए भारत सरकार ने ऊर्जा दक्षता और टिकाऊपन/वहनीयता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम लागू किए हैं।
सरकार की प्रमुख पहलों में से एक है ऊर्जा संरक्षण टिकाऊ भवन संहिता (Energy Conservation Sustainable Building Code, ECSBC)। इसे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) द्वारा विकसित किया गया है और विद्युत मंत्रालय (MoP) द्वारा लागू किया गया है। ECSBC में नए वाणिज्यिक और आवासीय भवनों के लिए न्यूनतम ऊर्जा दक्षता मानक निर्धारित हैं, और मूलत: इन्हें ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ECBC) के आधार पर विकसित किया गया है। इसमें ऊर्जा संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग और भवन के लिए अन्य हरित भवन आवश्यकताओं के मानदंड/मानक भी शामिल हैं। ECSBC के अलावा, कई निजी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा समर्थित स्वैच्छिक हरित बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम्स भी व्यापक रूप से लागू हैं।
ये हरित बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम ऊर्जा और जल दक्षता, टिकाऊ/वहनीय निर्माण सामग्री का उपयोग, अपशिष्ट प्रबंधन और भीतरी पर्यावरण गुणवत्ता सहित कई टिकाऊ/वहनीय मानकों के आधार पर परियोजनाओं का आकलन और प्रमाणन करते हैं। हालांकि ये रेटिंग सिस्टम्स आवासीय और वाणिज्यिक दोनों तरह के भवनों के लिए हैं, लेकिन इनका उपयोग अभी भी सीमित है – विशेष रूप से आवासीय क्षेत्र में। हालांकि न केवल केंद्र स्तर पर बल्कि नगर पालिकाओं के स्तर पर भी इन नीतियों को समर्थन हासिल है, लेकिन भारत की कुल भवन निर्माण/सामग्री का केवल 5 प्रतिशत हिस्सा ही हरित प्रमाणित है। हरित भवन निर्माण अपनाने में एक प्रमुख बाधा है हरित इमारतों के जीवनपर्यंत मिलने वाले लाभों के बारे में सीमित जागरूकता और समझ। पूरी जानकारी का अभाव उपभोक्ताओं की सोच-समझकर निर्णय लेने की क्षमता को सीमित करता है।
सूचना हस्तक्षेप
हमारा मानना है कि यदि उपभोक्ताओं को हरित प्रमाणन (green certification) के लाभ बताने वाली सही और प्रासंगिक जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी तो हरित भवनों को अपनाने/बनाने में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।
इस कमी को दूर करने के लिए हमारा सुझाव है कि मानकीकृत वहनीयता दर्शाने वाला एक प्रारूप (standard sustainability disclosure) बनाया जाए, जिसका उपयोग निर्माता अपनी परियोजनाओं का प्रचार-प्रसार करते समय करें। यह प्रारूप संभावित खरीदारों को भवन के पर्यावरणीय फायदों और टिकाऊ/वहनीय विशेषताओं के बारे में बताने का एक स्पष्ट, विश्वसनीय और तुलनीय तरीका होगा। ऊर्जा दक्षता, जल खपत, प्रयुक्त सामग्री और प्रमाणन जैसी महत्वपूर्ण जानकारी को सुलभ और समझने योग्य बनाकर यह प्रारूप रियल एस्टेट बाज़ार में पारदर्शिता (real estate transparency) बढ़ा सकता है।
महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उपभोक्ताओं को विकल्प चुनने में सक्षम बनाएगा और हरित भवनों के लाभों के बारे में उनकी जागरूकता बढ़ाएगा। जैसे-जैसे उपभोक्ताओं की जागरूकता बढ़ेगी, पर्यावरण के प्रति ज़िम्मेदार निर्माण की मांग भी बढ़ सकती है, जिससे बाज़ार भी टिकाऊ/वहनीय प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित होगा। भारत के तेज़ी से हो रहे शहरीकरण (urbanization in India) के मद्देनज़र, ऐसा अनुमान है कि वर्ष 2047 तक 50 प्रतिशत से अधिक आबादी शहरी क्षेत्रों में रहेगी। यह तरीका हरित भवन प्रथाओं को मुख्यधारा में लाने और संसाधन-कुशल, कम कार्बन वाले शहरी भवन निर्माण को तेज़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
हरित भवन रेटिंग प्रणालियां
पिछले दो दशकों में, भारत में हरित भवन प्रमाणन की इकोसिस्टम (green building ecosystem) अच्छी तरह से स्थापित हो चुकी है। भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) द्वारा शुरू की गई भारतीय हरित भवन परिषद (IGBC) पहली और व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली प्रणाली थी। इसके अलावा अन्य प्रमुख रेटिंग प्रणालियां हैं – दी एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट (TERI) की GRIHA, एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (ASSOCHAM) की GEM और यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की LEED। ये रेटिंग प्रणालियां विभिन्न प्रकार की इमारतों के लिए दिशानिर्देश देती हैं, जिनमें व्यक्तिगत भवनों से लेकर भवन परिसरों, आस-पड़ोस और यहां तक कि शहर-स्तरीय विकास परियोजनाएं भी शामिल हैं।
परियोजनाओं को हासिल टिकाऊ स्कोर के आधार पर प्रमाण-पत्र मिलता है। हर रेटिंग सिस्टम की रेटिंग वैधता अवधि अलग है; आम तौर पर किसी परियोजना को हासिल रेटिंग 3 से 5 वर्षों तक वैध रहती है। वैधता अवधि समाप्त होने के बाद परियोजनाओं को पुन: प्रमाणन लेना पड़ता है, जो पहले से विद्यमान इमारतों के लिए अलग होता है। पुन: प्रमाणन के समय रेटिंग बदल सकती है। इसमें रहवास-उपरांत ऑडिट के आधार पर परियोजना का मूल्यांकन किया जाता है, क्योंकि किसी परियोजना की वहनीयता की स्थिति समय के साथ बदल सकती है।
समस्त रेटिंग प्रणालियां ऊर्जा दक्षता, जल दक्षता, निर्माण सामग्री एवं संसाधन, अपशिष्ट प्रबंधन आदि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में कुछ अनिवार्य और कुछ वैकल्पिक मानदंड निर्धारित करती हैं। इनमें से कुछ रेटिंग प्रणालियां कुछ मानदंडों के अनुपालन के लिए ECBC के उपयोग की भी अनुशंसा करती हैं। गौरतलब है कि हर रेटिंग सिस्टम का समान वहनीय उपायों के लिए वेटेज और स्कोर करने का तरीका अलग होता है। इसलिए, किसी भवन को मिली हरित रेटिंग बस यह बताती है कि वह पारंपरिक/सामान्य भवनों से बेहतर है। अत: यह संभव है कि हरित रेटिंग प्राप्त भवन, हरित भवन का प्रमाणन हासिल करने के लिए निर्धारित पर्याप्त हरित विशेषताओं को पूरा न करता हो।
हरित भवन पदचिह्न
भवन की हरित भवन पदचिह्न की नवीनतम जानकारी हरित भवन रेटिंग सिस्टम के पोर्टल (green building portal) पर डाली जाती है, और उद्योग विशेषज्ञों द्वारा भवन स्टॉक संख्या का अनुमान भी लगाया जाता है। इन आंकड़ों के आधार पर, देश में कुल भवन निर्माणों में से 5 प्रतिशत भवन IGBC प्रमाणित हैं, 0.4 प्रतिशत GRIHA प्रमाणित भवन हैं और 0.04 प्रतिशत भवन LEED प्रमाणित हैं। यह दर्शाता है कि भारत में हरित भवनों का उपयोग/निर्माण अभी भी काफी कम है।
मानक वहनीयता प्रारूप
हरित विशेषताओं के प्रचार-प्रसार में सुधार और जागरूकता बढ़ाने का एक तरीका हो सकता है कि भवन विशेषताओं की रिपोर्टिंग का एक मानकीकृत प्रारूप (standard reporting format) बनाया जाए। इस प्रारूप से उपभोक्ता हरित रेटेड बनाम गैर-हरित रेटेड भवन की वहनीयता लागत की तुलना कर पाएंगे।
हरित बिल्डिंग काउंसिल भवन की हरित या वहनीय विशेषताओं को उजागर करने के लिए एक मानकीकृत प्रारूप बनाने में मदद कर सकती है। मानक प्रारूप दो महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा कर सकता है। एक तो यह किसी भवन की विशिष्ट वहनीय/टिकाऊ विशेषताओं के बारे में उपभोक्ताओं की समझ में सुधार कर सकता है। दूसरा यह तकनीकी रेटिंग को खरीदारों और उपयोगकर्ताओं के लिए स्पष्ट और सुलभ जानकारी के रूप में पेश कर सकता है, और सोचे-समझे निर्णय लेने में मदद कर सकता है।
वर्तमान में, IGBC, GRIHA, LEED और GEM जैसी विभिन्न ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणन प्रणालियां हैं, जो वहनीयता का आकलन करने के लिए अलग-अलग वेटेज और स्कोर पद्धतियों का उपयोग करती हैं। मसलन, ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण या सामग्री के पुन: उपयोग जैसे मापदंड पर हर रेटिंग प्रणाली का ज़ोर अलग है। इसके अलावा, दक्षता लाभ या वित्तीय लाभ का अनुमान लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियां विभिन्न कारकों के आधार पर भी अलग-अलग होती हैं, जैसे परियोजना के चरण (डिज़ाइन बनाम रहवास-उपरांत), आधारभूत तुलना के लिए प्रयुक्त मान्यताओं और कार्यान्वित की जाने वाली तकनीकों या प्रथाओं के प्रकार के आधार पर।
मापदंडों और प्रचार प्रारूपों, दोनों में यह भिन्नता उपभोक्ताओं के लिए परियोजनाओं को दिए गए प्रमाणपत्र को पूरी तरह से समझना मुश्किल बना देती है। एक सुसंगत पैमाने या तुलना बिंदु की अनुपस्थिति में भवनों की हरित विशेषताओं की तुलना करना भ्रामक हो जाता है और अक्सर गलत समझ और निर्णय लेने में असमर्थता का कारण बनता है। इसलिए शब्दावली, मानकों को सुसंगत बनाने वाला मानकीकृत प्रारूप जानकारी को सरल बना सकता है, तुलना को आसान कर सकता है और हरित भवन के वादों पर उपभोक्ता का विश्वास बढ़ा सकता है।
टिकाऊ मानदंड
हरित रेटिंग सिस्टम द्वारा परिभाषित टिकाऊ मानदंडों का हमने विश्लेषण किया। इस आधार पर हम कुछ ऐसे चुनिंदा मानदंड सुझा रहे हैं जो उपभोक्ताओं को सोचे-समझे और पर्यावरण के प्रति ज़िम्मेदार विकल्प चुनने में सक्षम बना सकते हैं। यही मानदंड मानकीकृत रिपोर्टिंग के प्रारूप भी बन सकते हैं।
1. दिनांक और वैधता के साथ हरित रेटिंग (rating validity): रेटिंग जारी करने की तिथि और वैधता की जानकारी उपभोक्ता के लिए अहम है। यह जानकारी उपभोक्ता को यह विश्वास दिलाती है कि प्रमाणपत्र हालिया है और यह भवन टिकाऊ है।
2. भवन के जीवनकाल में होने वाली बचत का अनुमानित आंकड़ा (lifecycle savings): भवन और इकाई दोनों स्तर पर ऊर्जा, जल और अपशिष्ट प्रबंधनों से होने वाली अनुमानित आर्थिक बचत दिखाई जा सकती है।
भवन स्तर पर – नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, पानी की बचत और उसके पुनर्चक्रण एवं पुनर्उपयोग, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि के लिए लगाई गई प्रणालियां बताई जा सकती हैं।
व्यक्तिगत इकाई स्तर पर – कुशल भवन आवरण बनाकर, नलों में पानी प्रवाह कम करने वाले उपाय लगाकर किए गए ऊर्जा संरक्षण के बारे में जानकारी देना। मौजूदा विभिन्न उपकरणों/सॉफ्टवेयर से हरित भवन की लागत का आकलन दर्शाया जा सकता है।
3. ऊर्जा दक्षता का मापन:
- बिजली बचत की मात्रा द्वारा
- सौर, SWH प्रणालियों द्वारा
- कुशल उपकरणों द्वारा
- नवीकरणीय प्रौद्योगिकियां अपनाकर और कुशल उपकरण लगाकर बिजली बिल कम आएगा।
4. तापीय आराम का मापन:
- (एसी के साथ और बिना बिताए आरामदायक घंटे/वर्ष
- दीवार और खिड़की की सामग्री के आधार पर
- HVAC दक्षता (U value, WWR, RETV, EER) के आधार पर
- एसी के बिना यदि भवन के भीतर आरामदायक वक्त बीतता है तो इससे बिजली बचेगी। दिए गए अंक उपभोक्ताओं को यह आकलन करने में मदद कर सकते हैं कि गर्मी से राहत पाने के लिए क्या वास्तव में एसी में ज़रूरी है?
5. ऊर्जा प्रदर्शन सूचकांक (Energy Performance Index – EPI): यह विभिन्न परियोजनाओं में ऊर्जा खपत की तुलना करने में मदद करता है – कम EPI यानी उच्च दक्षता।
6. जल दक्षता का मापन (water efficiency metrics)
- प्रतिशत पानी की बचत
- वर्षा जल संचयन की मात्रा
- रीसायकल पानी की मात्रा और उसका उपयोग
- यह मीठे पानी की बचत करेगा, स्थिरता को बढ़ाएगा और पानी का बिल कम करेगा
7. अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियां (on-site waste management): ऑन-साइट अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों और उनकी दक्षता के बारे में जानकारी देना।
8. सार्वजनिक परिवहन से निकटता (public transport accessibility): नज़दीकी सार्वजनिक परिवहन सेवा तक पैदल जाने में लगने वाला समय – उपभोक्ताओं को रोज़ाना आने-जाने में लगने वाले समय की योजना बनाने में मददगार होगा।
9. सबकी पहुंच (universal accessibility): बुज़ुर्गों और विकलांग व्यक्तियों सहित सभी के लिए आसान पहुंच।
वर्तमान में भी कुछ हरित भवन सलाहकार और डेवलपर अपने-अपने प्रारूपों के ज़रिए (खासकर विपणन या प्रमाणन के दौरान) परियोजना की वहनीयता सम्बंधी विशेषताएं बताते हैं। हालांकि ये प्रयास पारदर्शिता के प्रति बढ़ती प्रतिबद्धता दर्शाते हैं लेकिन प्रारूपों में एकरूपता के अभाव के चलते उपभोक्ताओं के लिए विभिन्न परियोजनाओं के लाभों की तुलना करना और मूल्यांकन एक चुनौती बन जाता है।
आगे की राह
एक मानक प्रारूप से हरित और टिकाऊ भवन विशेषताओं के बारे में जागरूकता लाने में काफी मदद मिल सकती है, और प्रमाणित हरित भवनों को खरीदने/बनाने में तेज़ी आ सकती है। यह प्रारूप उपभोक्ताओं को पारंपरिक भवनों की तुलना में टिकाऊ भवनों के लाभों के बारे में विश्वसनीय, तुलनीय और समझने में आसान जानकारी दे सकता है। इसका उपयोग रियल एस्टेट परियोजनाओं के विपणन(real estate marketing), बिक्री और प्रचार सामग्री में किया जा सकता है।
यह प्रारूप भारतीय राष्ट्रीय भवन परिषद (National Building Council) द्वारा गठित एक अंतर-परिषद समिति द्वारा तैयार करके लागू किया जा सकता है। इस समिति में केंद्र सरकार, प्रमुख हरित भवन परिषद और रियल एस्टेट हितधारक और राज्य RERA प्राधिकरणों (Real Estate Regulatory Authority) के प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं।
प्रस्तावित समिति को ये प्रमुख नीतिगत कार्य सौंपे जा सकते हैं:
1. विभिन्न हरित भवन रेटिंग सिस्टम के मुख्य टिकाऊ मापदंडों का समन्वय करके एकरूप प्रारूप बनाना और अधिसूचित करना।
2. सभी मान्यता प्राप्त ढांचों में सामंजस्य बनाना, जिससे एकरूपता और तुलनीयता सुनिश्चित हो।
3. कार्यान्वयन दिशानिर्देश और अनुपालन प्रोटोकॉल स्थापित करना, जिसमें राज्य-स्तरीय RERA जैसे मौजूदा प्लेटफार्मों के साथ एकीकरण शामिल है, ताकि इसे अपनाना आसान हो।
4. वहनीयता के दावों को सत्यापित करने व गलतबयानी से सम्बंधित शिकायतों के समाधान के लिए एक निगरानी एवं शिकायत निवारण तंत्र बनाना।
5. प्रारूप की प्रभावशीलता की समीक्षा करने और इसके बेहतर होते वहनीयता मानकों, नियामकों और उपभोक्ता अपेक्षाओं के अनुरूप अपडेट करने के लिए सतत परामर्श करना।
प्रमुख हितधारकों के बीच समन्वय को बढ़ावा देकर समिति उपभोक्ता और डेवलपर्स के बीच मौजूदा सूचना अंतर को पाट सकती है। भारत तेज़ी से शहरीकृत हो रहा है। ऐसे प्रयास अधिक टिकाऊ निर्मित परिवेश (sustainable urban development) बनाने में मदद कर सकते हैं। (स्रोत फीचर्स)
नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
Photo Credit : https://img.etimg.com/thumb/width-1200,height-900,imgsize-28874,resizemode-75,msid-111003760/industry/services/property-/-cstruction/green-buildings-market-in-india-to-reach-39-billion-by-2025.jpg