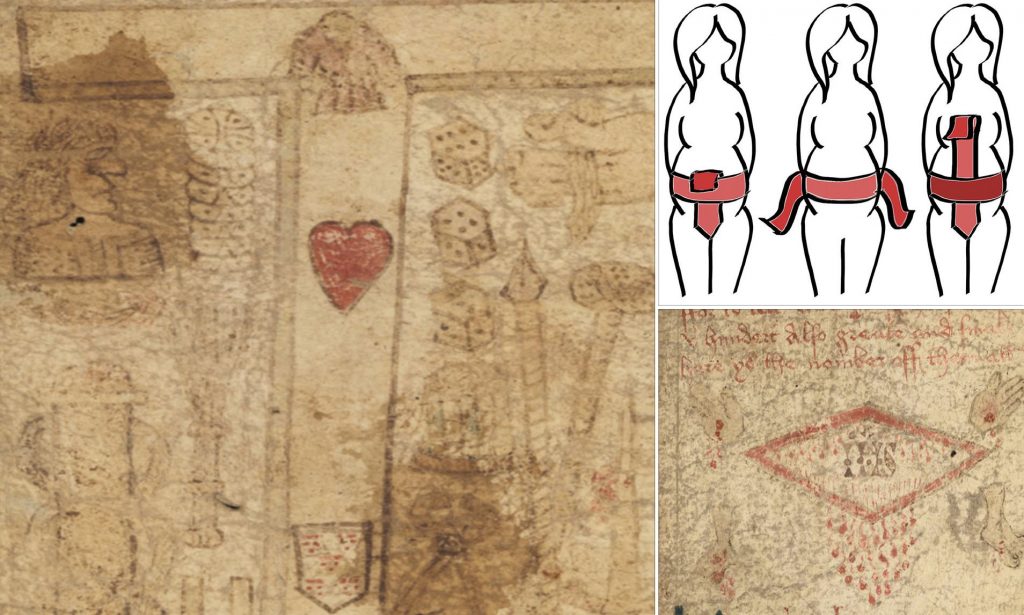आज के दौर के सोशल मीडिया ने एक ओर जहां लोगों को जोड़ने का काम किया है, वहीं दूसरी ओर इसके माध्यम से भ्रामक खबरों को साझा करने के चलते ध्रुवीकरण, हिंसक उग्रवाद और नस्लवाद में भी काफी तेज़ी से वृद्धि हुई है। सवाल यह है कि वे कौन लोग हैं जो भ्रामक खबरों को साझा करते हैं? एक विश्लेषण के अनुसार रूढ़िवादी लोग काफी हद तक भ्रामक सूचनाओं के प्रसार के लिए ज़िम्मेदार हैं।
इन भ्रामक सूचनाओं के संकट का समाधान खोजने के लिए एक ऐसे स्पष्ट आकलन की आवश्यकता है जिससे यह पता लगाया जा सके कि झूठ और षडयंत्र के सिद्धांतों को कौन फैला रहा है। इस विषय में ड्यूक युनिवर्सिटी के मैनेजमेंट एंड आर्गेनाइज़ेशन के शोध छात्र अशर लॉसन और इसी युनिवर्सिटी में फुकुआ स्कूल ऑफ बिज़नेस के असिस्टेंट प्रोफेसर हेमंत कक्कड़ ने लोगों के व्यक्तित्व को मुख्य निर्धारक के रूप में जांचने का काम किया।
व्यक्तित्व लक्षणों की पहचान और मापन के लिए उन्होंने प्रचलित फाइव-फैक्टर थ्योरी का इस्तेमाल किया जिसे बिग फाइव भी कहा जाता है। यह थ्योरी व्यक्तित्वों को 5 श्रेणियों में बांटती है: अनुभव के प्रति खुलापन, कर्तव्यनिष्ठा, बहिर्मुखता, सहमत होने की तैयारी और उन्माद। इस ढांचे के अंतर्गत कर्तव्यनिष्ठा पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया जिससे लोगों की सलीकापसंदगी, उत्तेजित होने पर आत्म-नियंत्रण, रूढ़िवादिता और विश्वसनीयता में अंतरों का पता चलता है।
शोधकर्ताओं का अनुमान था कि कम-कर्तव्यनिष्ठ रूढ़िवादी लोग (एलसीसी) अन्य रूढ़िवादियों या कम-कर्तव्यनिष्ठ उदारवादियों की तुलना में अधिक भ्रामक समाचार साझा करते हैं। उन्होंने व्यक्तित्व, राजनीति और भ्रामक समाचारों को साझा करने के बीच सम्बंधों का पता लगाने के लिए 8 अध्ययन किए जिनमें 4642 प्रतिभागी शामिल थे।
सबसे पहले शोधकर्ताओं ने विभिन्न आकलनों के माध्यम से लोगों की राजनीतिक विचारधारा और कर्तव्यनिष्ठा को मापा जिसमें प्रतिभागियों से उनके मूल्यों और व्यवहारों के बारे में पूछा गया था। इसके बाद प्रतिभागियों को कोविड से सम्बंधित कुछ सत्य और भ्रामक समाचारों की शृंखला दिखाई गई और इन समाचारों की सटीकता के बारे में सवाल किए गए। यह भी पूछा गया कि वे इन समाचारों को साझा करेंगे या नहीं। उन्होंने पाया कि उदारवादी और रूढ़िवादी, दोनों ही प्रकार के लोग कभी-कभी भ्रामक समाचार को सही मान लेते हैं। शायद उन्होंने इन समाचारों को सटीक इसलिए माना क्योंकि ये उनके विश्वासों से मेल खाते थे।
यह भी देखा गया कि विभिन्न राजनैतिक विचारधाराओं से जुड़े लोगों ने भ्रामक समाचार साझा करने की बात कही लेकिन अन्य सभी प्रतिभागियों की तुलना में एलसीसी के बीच यह व्यवहार काफी अधिक देखा गया। हालांकि, उच्च स्तर के कर्तव्यनिष्ठ उदारवादियों और रूढ़िवादियों के बीच कोई अंतर देखने को नहीं मिला जबकि कम-कर्तव्यनिष्ठ उदारवादियों ने उच्च-कर्तव्यनिष्ठ उदारवादियों की तुलना भ्रामक समाचार ज़्यादा साझा नहीं किए।
दूसरे अध्ययन में, शोधकर्ताओं ने इन परिणामों को स्पष्ट राजनीतिक रुझान वाले भ्रामक समाचारों के साथ दोहराया और पिछले अध्ययन से भी अधिक प्रभाव देखा। इस बार भी विभिन्न स्तर की कर्तव्यनिष्ठा वाले उदारवादी और उच्च कर्तव्यनिष्ठ रूढ़िवादी व्यापक स्तर पर भ्रामक जानकारी फैलाने में शामिल नहीं थे। भ्रामक समाचार फैलाने वालों में कम कर्तव्यनिष्ठ रूढ़िवादी (एलसीसी) आगे रहे।
सवाल यह था कि एलसीसी में भ्रामक समाचार को साझा करने की प्रवृत्ति क्यों होती है। इसके लिए शोधकर्ताओं ने एक ऐसा प्रयोग किया जिसमें प्रतिभागियों की राजनीतिक विचारधारा और व्यक्तित्व के बारे में जानकारी के अलावा उनमें अराजकता की चाहत, सामाजिक और आर्थिक रूप से रूढ़िवादी मुद्दों के समर्थन, मुख्यधारा मीडिया पर भरोसे और सोशल मीडिया पर बिताए गए समय का आकलन किया गया। शोधकर्ताओं के अनुसार एलसीसी ने अराजकता की ज़रूरत ज़ाहिर की, और साथ ही वर्तमान राजनीतिक-सामाजिक संस्थाओं को बाधित करने और नष्ट करने की इच्छा भी व्यक्त की। इनसे भ्रामक जानकारियों को फैलाने की उनकी प्रवृत्ति की व्याख्या हो जाती है। यह किसी अन्य विचारों और समूहों की तुलना में स्वयं को श्रेष्ठ मानने की इच्छा को भी दर्शाता है जो कम कर्तव्यनिष्ठ रूढ़िवादियों में अधिक देखने को मिलती है।
दुर्भाग्य से, शोधकर्ताओं को यह भी पता चला कि समाचारों पर सटीकता का लेबल लगाने से भी भ्रामक जानकारी की समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है। इसके लिए शोधकर्ताओं ने एक प्रयोग अंजाम दिया जिसमें सोशल मीडिया पर साझा किए गए सही समाचार के लिए ‘पुष्ट’ और भ्रामक समाचार के लिए ‘विवादित’ टैग का उपयोग किया गया। उन्होंने पाया कि उदारवादियों और रूढ़िवादियों ने ‘पुष्ट’ टैग वाले समाचार को अधिक साझा किया। हालांकि, एलसीसी ने अभी भी जानकारी को गलत या भ्रामक जानते हुए भी साझा करना जारी रखा।
इसके बाद शोधकर्ताओं ने एक और अध्ययन किया जिसमें प्रतिभागियों को स्पष्ट रूप से बताया गया कि जिस जानकारी को वे साझा करना चाहते हैं वह गलत है। इसके बाद उनको अपने निर्णय को बदलने का मौका भी दिया गया। इसके बाद भी एलसीसी द्वारा भ्रामक समाचार साझा करने की दर काफी उच्च रही और वे समाचार के गलत होने की चेतावनियों को भी अनदेखा करते रहे।
यह परिणाम काफी चिंताजनक है जिसमें एलसीसी भ्रामक समाचारों के प्रसार के प्राथमिक चालक नज़र आते हैं। इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को चेतावनी का लेबल लगाने के बजाय कोई और समाधान खोजना होगा। एक अन्य विकल्प के रूप में सोशल मीडिया कंपनियों को ऐसे समाचारों को अपने प्लेटफॉर्म्स से हटाने के प्रयास करने चाहिए जो किसी व्यक्ति समुदाय को चोट पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। कुल मिलाकर मुद्दा सिर्फ इतना है कि जब तक सोशल मीडिया कंपनियां कोई ठोस तरीका खोज नहीं निकालती हैं तब तक यह समस्या बनी रहेगी। (स्रोत फीचर्स)
नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
Photo Credit : https://static.scientificamerican.com/sciam/cache/file/29641891-B59E-4081-9382EC78FA3AB9E5_source.jpg