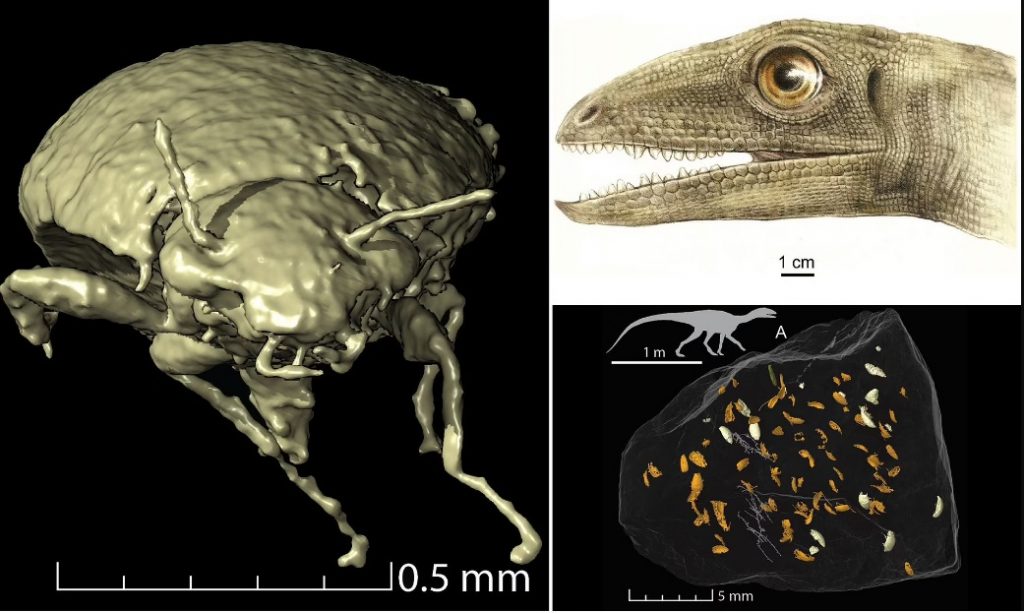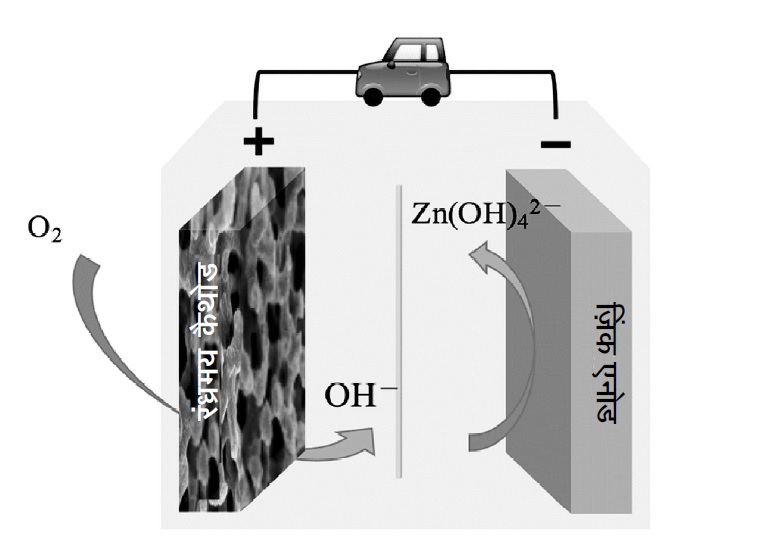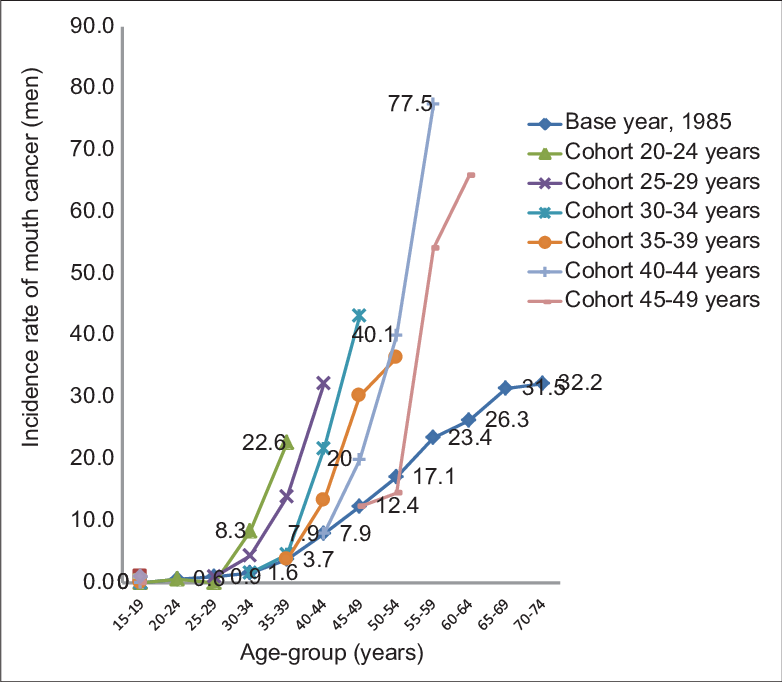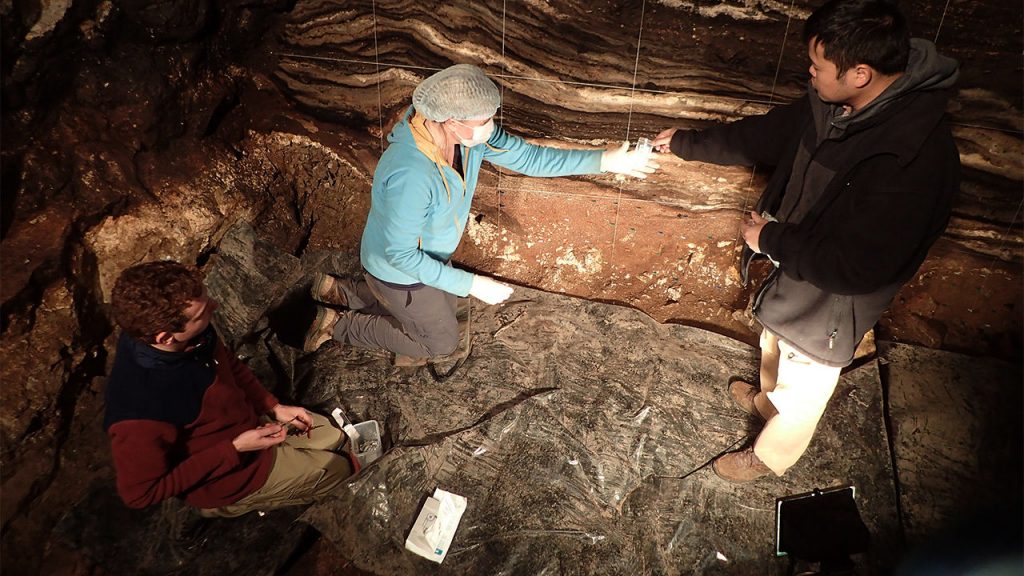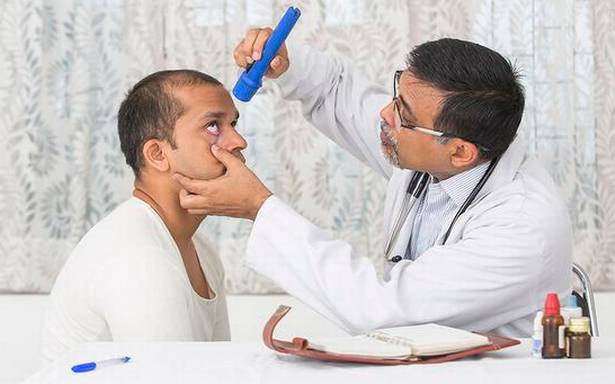वर्ष 2020 के सहस्राब्दी टेक्नॉलॉजी पुरस्कार की घोषणा मई में की गई। यह पुरस्कार डीएनए अनुक्रमण (सिक्वेंसिंग) की क्रांतिकारी तकनीक के विकास हेतु शंकर बालसुब्रमण्यन और डेविड क्लेनरमैन को दिया गया है। उनका काम विज्ञान और नवाचार का उत्कृष्ट संगम है। यह बहुत प्रासंगिक भी है क्योंकि वर्तमान महामारी के संदर्भ में हम सबने जीनोम अनुक्रमण के बारे में खूब सुना है।
नवाचार पर ज़ोर
यह पुरस्कार फिनलैंड की सर्वोच्च अकादमियों और उद्योगों के साथ मिलकर फिनलैंड गणतंत्र द्वारा दिया जाता है। सहस्राब्दी पुरस्कार में इक्कीसवीं सदी का नज़रिया है जिसमें नवाचार पर बहुत ज़ोर है। अतीत में इस पुरस्कार के विजेताओं में टिम बर्नर्स ली (वर्ल्ड वाइड वेब के क्रियांवयन के लिए) और फ्रांसिस अरनॉल्ड (प्रयोगशाला की परिस्थितियों में निर्देशित जैव विकास पर शोध के लिए) शामिल रहे हैं। एक गौरतलब बात है कि ग्यारह में से सात पुरस्कार विजेताओं को आगे चलकर नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो हम दिल थामकर बालसुब्रमण्यन और क्लेरमैन का इन्तज़ार करें।
शंकर बालसुब्रमण्यन का जन्म चेन्नै में हुआ था और उन्होंने अपना अधिकांश जीवन इंग्लैंड में बिताया। पीएच.डी. करने के बाद वे कैम्ब्रिज विश्वविशलय के रसायन विभाग से जुड़ गए। लगभग उसी समय क्लेरमैन भी विभाग में आए और दोनों की टीम बन गई। शुरुआती लक्ष्य तो एक ऐसा सूक्ष्मदर्शी बनाने का था जो इकलौते अणुओं को देख सके। बालसुब्रमण्यन की विशेष रुचि उस आणविक मशीनरी में थी जिसका उपयोग डीएनए अपनी प्रतिलिपि बनाने में करता है। बातचीत में कभी इस विचार का कीड़ा कुलबुलाया कि डीएनए की वर्णमाला को पढ़ने का कोई नया तरीका निकाला जाए ताकि डीएनए में संग्रहित सूचना तक आसानी से पहुंचा जा सके।
डीएनए (या कुछ वायरसों में आरएनए) सजीवों की जेनेटिक सामग्री होती है। यह चार क्षारों से बना होता है – ए, टी, जी और सी। आरएन के संदर्भ में टी का स्थान यू नामक क्षार ले लेता है। गुणसूत्र इन्हीं क्षारों की एक रैखीय दोहरी शृंखला होता है। डीएनए में क्षारों का क्रम ही सूचना होता है। यही जीवन की कुंडली है। जीवन अपनी प्रतिलिपि बना सकता है और डीएनए एक एंज़ाइम – डीएनए पोलीमरेज़ – की मदद से स्वयं की प्रतिलिपि बनाता है। इस एंज़ाइम की मदद से डीएनए का कोई भी सूत्र अपना पूरक सूत्र बना सकता है।
नवाचारी विचार
बालसुब्रमण्यन और क्लेरमैन का नवाचारी विचार यह था कि सूत्र के संश्लेषण की इस प्रक्रिया की मदद से डीएनए (या आरएनए) का अनुक्रमण किया जाए। उन्होंने चतुराई से ए, टी, जी और सी क्षारों को इस तरह बदला कि हरेक एक अलग रंग में चमकता था। जब प्रतिलिपि बनती तो डीएनए की ‘रंगीन’ प्रति के मात्र रंगों के आधार पर क्षारों का पता लगाया जा सकता था। इसके लिए सूक्ष्म प्रकाशीय व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की ज़रूरत पड़ती थी।
उनके इस ‘नई पीढ़ी के अनुक्रमण’ (NGS) की महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी मदद से एक बार में डीएनए की बड़ी साइज़ का अनुक्रमण किया जा सकता है – एक बार में 10 लाख से ज़्यादा क्षार जोड़ियों का अनुक्रमण संभव है। इसका मतलब है कि एक बार में सैकड़ों जीन्स और किसी-किसी जीव के पूरे जीनोम का अनुक्रमण हो सकता है। यह संभव हो पाता है एक साथ डीएनए के सैकड़ों खंडों का अनुक्रमण करके। एक लंबे डीएनए अणु को बेतरतीबी से छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। प्रत्येक टुकड़े में चंद सैकड़ा क्षार होते हैं। इन सबका अनुक्रमण एक साथ किया जाता है। इसके बाद इन अलग-अलग अनुक्रमों को किसी पहेली के समान आपस में जोड़कर पूरी शृंखला पता की जाती है।
बालसुब्रमण्यन और क्लेरमैन की पहल पर इस टेक्नॉलॉजी ने सोलेक्सा के रूप में व्यापारिक स्वरूप हासिल कर लिया है। इस निहायत सफल स्टार्टअप को बाद में बायोटेक कंपनी इल्यूमिना ने अधिग्रहित कर लिया।
घटती लागत
इस सारे अनुक्रमण की लागत की बात करते हैं। जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने पहला लगभग पूरा जीनोम अनुक्रमित किया था, तब उसकी अनुमानित लागत 3 अरब डॉलर थी। चूंकि हमारे सारे गुणसूत्रों में कुल मिलाकर 3 अरब क्षार जोड़ियां हैं, तो यह गणना आसान है कि अनुक्रमण की लागत 1 डॉलर प्रति क्षार जोड़ी थी। वर्ष 2020 तक NGS टेक्नॉलॉजी की बदौलत आपके पूरे जीनोम के अनुक्रमण की लागत घटकर चंद हज़ार डॉलर रह गई। जब यह टेक्नॉलॉजी भारत में प्रचलित होगी तब इसकी लागत चंद हज़ार रुपए होगी!
कोरोनावायरस के जीनोम में 3 अरब नहीं बल्कि मात्र 30,000 आरएनए क्षार हैं। तब कोई अचरज की बात नहीं कि हमारे पास नए कोरोनावायरस और उसके वैरिएन्ट्स के जीनोम को लेकर जानकारी का अंबार है। यूके में स्वास्थ्य अधिकारियों ने हर सोलह पॉज़िटिव व्यक्तियों में से 1 के वायरस जीनोम का अनुक्रमण किया है। लोकप्रिय जीनोम डैटा साझेदारी साइट GSAID पर 172 देशों से 20 लाख से ज़्यादा सार्स-कोव-2 जीनोम अनुक्रम उपलब्ध हैं। दुनिया भर में कोरोनावायरस के नए-नए संस्करणों के प्रसार और उत्पत्ति की निगरानी NGS के दम पर ही संभव हुई है।
शंकर बालसुब्रमण्यन आज भी एक बढ़िया प्रयोगशाला का संचालन करते हैं, जो ऐसे उपचारात्मक अणु की डिज़ाइन पर केंद्रित है जो कई जीन्स की बेलगाम अभिव्यक्ति को नियंत्रित करके कैंसर जैसी स्थितियों में उनके द्वारा किए जाने वाले नुकसान को रोक सकेंगे। (स्रोत फीचर्स)
नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
Photo Credit : https://th.thgim.com/sci-tech/science/c6n9jx/article35254815.ece/ALTERNATES/FREE_660/11TH-SCIWINNERSjpg