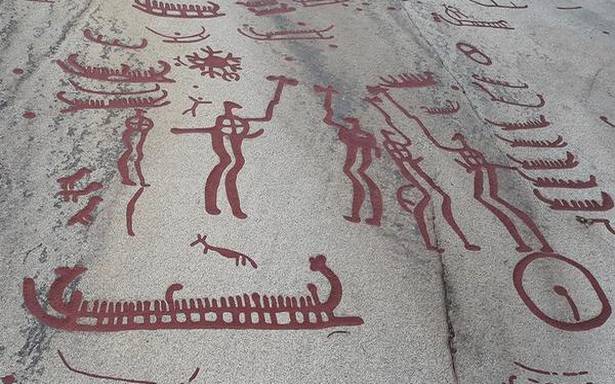मार्च 2020 में मिशिगन विश्वविद्यालय की कैंसर विज्ञानी रेशमा जग्सी ने कोविड-19 महामारी के महिला वैज्ञानिकों के काम पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के बारे में पूर्वानुमान लगाते हुए एक राय लिखी थी। डैटा न होने के कारण संपादकों ने इस राय को प्रकाशित करने से मना कर दिया था। लेकिन इसके बाद से कई टिप्पणीकार यही बात दोहराते आए हैं। अब अध्ययन से प्राप्त प्रमाणों से स्पष्ट हो गया है कि कोविड-19 महामारी में पहले से व्याप्त असमानताएं और बढ़ गर्इं हैं, इस दौर ने महिला वैज्ञानिकों के लिए नई चुनौतियां खड़ी की हैं। खासकर जिन महिला वैज्ञानिकों के बच्चे हैं उन्होंने अपना अनुसंधान कार्य करते रहने के लिए अतिरिक्त संघर्ष किया है।
कुछ विषयों में किए गए अध्ययन के डैटा से पता चलता है कि कोरोना महामारी के शुरुआती महीनों में भेजे गए प्रीप्रिंट्स, पांडुलिपियों, और प्रकाशित शोधपत्रों में महिला लेखकों की संख्या में कमी आई है। 20,000 शोधकर्ताओं पर वैश्विक स्तर पर किए गए सर्वेक्षण में पाया गया है कि इस दौरान पिता-वैज्ञानिकों की तुलना में माता-वैज्ञानिकों के अनुसंधान कार्यों के घंटों में 33 प्रतिशत अधिक की कमी आई है। मई 2020 से जुलाई 2020 तक हुए सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि माता-वैज्ञानिकों ने पिता-वैज्ञानिकों की तुलना में अधिक घरेलू दायित्व निभाए और बच्चों की देखभाल करने में अधिक समय बिताया।
लेकिन इस दौरान थोड़ी सकारात्मक बातें भी दिखीं। एक फंडिंग एजेंसी ने महामारी के दौरान बढ़ी लैंगिक असमानता को पहचाना और उसमें सुधार के प्रयास किए। दरअसल, फरवरी 2020 में केनेडियन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान ने कोविड-19 सम्बंधी शोध कार्यों के लिए अनुदान की पेशकश की थी, जिसमें एजेंसी ने शोधकर्ताओं को प्रस्ताव भेजने के लिए महज़ 8 दिन की मोहलत दी थी। यह कनाडा में तालाबंदी के पहले की बात है। लेकिन उन्होंने देखा कि प्राप्त प्रस्तावों में से केवल 29 प्रतिशत प्रस्ताव ही महिला शोधकर्ताओं द्वारा भेजे गए थे, यह संख्या पूर्व में भेजे जाने वाले प्रस्तावों की संख्या से लगभग सात प्रतिशत कम थी।
संख्या में इतना अंतर देखने के बाद संस्थान के इंस्टीट्यूट ऑफ जेंडर एंड हेल्थ की निदेशक कारा तेनेनबॉम को लगा कि हमने कहीं कुछ गलती कर दी है। इसीलिए जब संस्थान ने दो महीने बाद कोविड-19 शोध कार्यों के लिए दोबारा प्रस्ताव मंगाए तो उन्होंने प्रस्ताव भेजने की समय सीमा को 8 दिन से बढ़ाकर 19 दिन कर दी और दस्तावेज़ी कार्रवाइयां भी कम कर दीं। प्रोसीडिंग्स ऑफ दी नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज़ में के अनुसार दूसरे दौर में महिलाओं द्वारा भेजे गए प्रस्तावों की संख्या बढ़कर 39 प्रतिशत हो गई थी।
संस्थान द्वारा मांगे गए प्रस्तावों के संदर्भ में लावल युनिवर्सिटी की स्वास्थ्य शोधकर्ता होली विटमैन अपना अनुभव बताती हैं, “जब पहली बार मैंने प्रस्ताव भेजने की समय सीमा महज़ 8 दिन देखी तो मैंने सोचा कि दो बच्चों और अपनी स्वास्थ्य स्थिति के साथ इतने कम समय में अनुदान के लिए देर रात तक बैठकर प्रस्ताव लिखना और भेजना संभव नहीं है। लेकिन जब अनुदान के लिए दोबारा प्रस्ताव मांगे गए तो प्रस्ताव लिखने के लिए पर्याप्त समय था, जिसमें अंतत: मुझे अनुदान मिला भी।”
महामारी के दौर में अधिकांश शोधकर्ताओं के शोध कार्य के घंटों में कमी आई। ताज़ा अध्ययन बताते हैं कि पालक-शोधकर्ताओं, खासकर माता-शोधकर्ताओं के काम के घंटों में बहुत कमी आई है। पिता की तुलना में माताओं ने बच्चे की देखभाल और गृहकार्य करने में अधिक समय बिताया। इस संदर्भ में सान्ता क्लारा युनिवर्सिटी की रॉबिन नेल्सन बताती हैं कि पिछले साल की तुलना में कोरोनाकाल में उनके काम के घंटे घटकर आधे हो गए हैं क्योंकि उनके दो बच्चे अब घर पर होते हैं। कुछ शोधकर्ता अन्य की तुलना में अधिक बाधाओं में काम कर रहे हैं। इसलिए हमें अब अनुदान की प्रक्रिया, समय सीमा, नीतियों आदि पर सवाल उठाने चाहिए।
बोस्टन विश्वविद्यालय के इकॉलॉजिस्ट रॉबिन्सन फुलवाइलर का कहना है कि विश्वविद्यालयों और फंडिंग एजेंसियों को वैज्ञानिकों को यह बताने का भी विकल्प देना चाहिए कि कोविड-19 ने उनके काम में किस तरह की बाधा डाली या प्रभावित किया। इसके अलावा नियोक्ताओं को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी शोधकर्ताओं को ठीक-ठाक झूलाघर जैसी सुविधाएं मिलें। फुलवाइलर और अन्य माता-वैज्ञानिकों ने प्लॉस बायोलॉजी में इस तरह की व कई अन्य सिफारिशें की हैं। कोरोनाकाल में और स्पष्ट होती असमानता को अब दूर करने के प्रयास करने का वक्त है। (स्रोत फीचर्स)
नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
Photo Credit : https://www.sciencemag.org/sites/default/files/styles/article_main_image_-1280w__no_aspect/public/ca_0212NID_Mother_Child_online.jpg?itok=KtvdvK2V